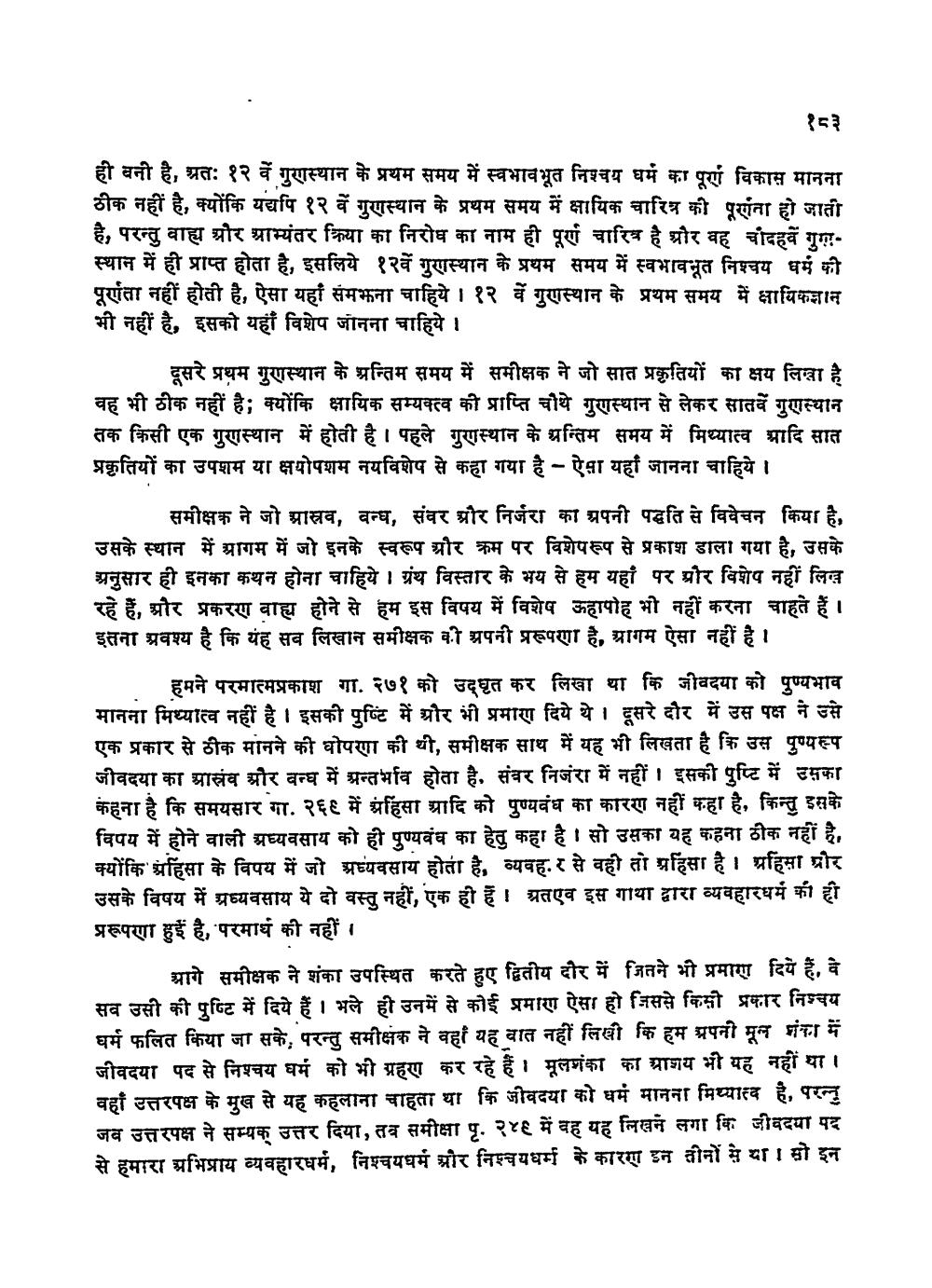________________
१८३
ही बनी है, अत: १२ वें गुणस्थान के प्रथम समय में स्वभावभूत निश्चय धर्म का पूर्ण विकास मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि १२ वें गुणस्थान के प्रथम समय में क्षायिक चारित्र की पूर्णता हो जाती है, परन्तु वाह्य और आभ्यंतर क्रिया का निरोध का नाम ही पूर्ण चारित्र है और वह चौदहवें गुणस्थान में ही प्राप्त होता है, इसलिये १२वें गुणस्थान के प्रथम समय में स्वभावभूत निश्चय धर्म की पूर्णता नहीं होती है, ऐसा यहां समझना चाहिये । १२ वें गुणस्थान के प्रथम समय में क्षायिकज्ञान भी नहीं है, इसको यहाँ विशेप जानना चाहिये ।
दूसरे प्रथम गुणस्थान के अन्तिम समय में समीक्षक ने जो सात प्रकृतियों का क्षय लिन्ना है वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी एक गुणस्थान में होती है । पहले गुणस्थान के अन्तिम समय में मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों का उपशम या क्षयोपशम नयविशेष से कहा गया है - ऐसा यहां जानना चाहिये।
समीक्षक ने जो आस्रव, बन्ध, संवर और निर्जरा का अपनी पद्धति से विवेचन किया है, उसके स्थान में आगम में जो इनके स्वरूप और क्रम पर विशेषरूप से प्रकाश डाला गया है, उसके अनुसार ही इनका कथन होना चाहिये । ग्रंथ विस्तार के भय से हम यहां पर और विशेष नहीं लिख रहे हैं, और प्रकरण वाह्य होने से हम इस विषय में विशेष ऊहापोह भी नहीं करना चाहते हैं । इतना अवश्य है कि यह सब लिखान समीक्षक की अपनी प्ररूपणा है, पागम ऐसा नहीं है।
हमने परमात्मप्रकाश गा. २७१ को उद्धृत कर लिखा था कि जीवदया को पुण्यभाव मानना मिथ्यात्व नहीं है । इसकी पुष्टि में और भी प्रमाण दिये थे। दूसरे दौर में उस पक्ष ने उसे एक प्रकार से ठीक मानने की घोपणा की थी, समीक्षक साथ में यह भी लिखता है कि उस पुण्यरूप जीवदया का आस्रव और बन्ध में अन्तर्भाव होता है. संवर निजरा में नहीं। इसकी पुष्टि में उसका कहना है कि समयसार मा. २६६ में अहिंसा आदि को पुण्यवंध का कारण नहीं कहा है, किन्तु इसके विपय में होने वाली अध्यवसाय को ही पुण्यवंध का हेतु कहा है। सो उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अहिंसा के विपय में जो अध्यवसाय होता है, व्यवहार से वही तो अहिंसा है। अहिंसा और उसके विषय में अध्यवसाय ये दो वस्तु नहीं, एक ही हैं। अतएव इस गाथा द्वारा व्यवहारधर्म की ही प्ररूपणा हुई है, परमार्थ की नहीं ।
आगे समीक्षक ने शंका उपस्थित करते हुए द्वितीय दौर में जितने भी प्रमाण दिये हैं, वे सब उसी की पुष्टि में दिये हैं। भले ही उनमें से कोई प्रमाण ऐसा हो जिससे किसी प्रकार निश्चय धर्म फलित किया जा सके, परन्तु समीक्षक ने वहां यह बात नहीं लिखी कि हम अपनी मूल शंका में जीवदया पद से निश्चय धर्म को भी ग्रहण कर रहे हैं। मूलशंका का प्राशय भी यह नहीं था। वहाँ उत्तरपक्ष के मुख से यह कहलाना चाहता था कि जीवदया को धर्म मानना मिथ्यात्व है, परन्तु जब उत्तरपक्ष ने सम्यक् उत्तर दिया, तब समीक्षा पृ. २४६ में वह यह लिखने लगा कि जीवदया पद से हमारा अभिप्राय व्यवहारधर्म, निश्चयधर्म और निश्चयधर्म के कारण इन तीनों में या । सो इन