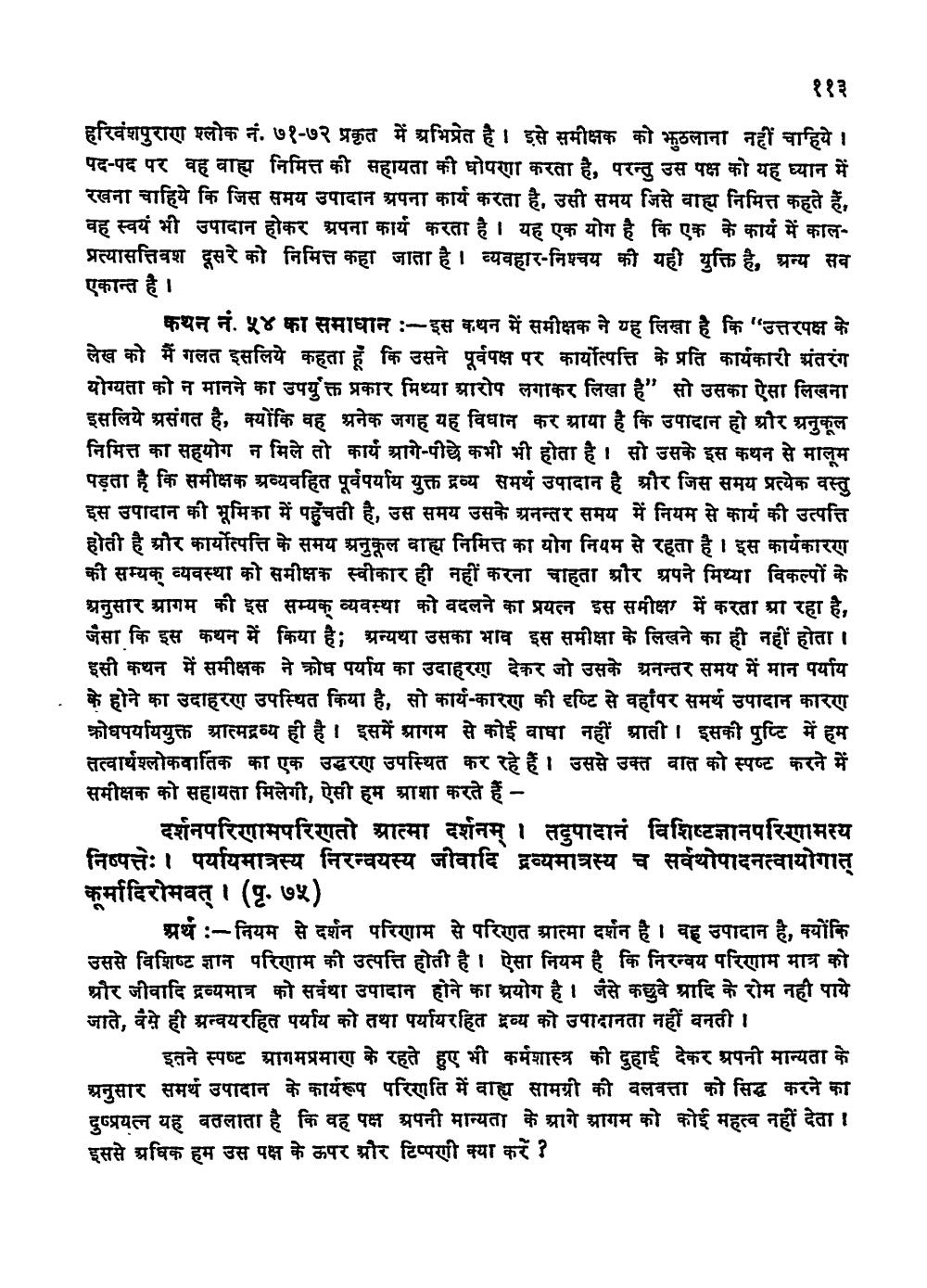________________
११३ हरिवंशपुराण श्लोक नं. ७१-७२ प्रकृत में अभिप्रेत है। इसे समीक्षक को झुठलाना नहीं चाहिये। पद-पद पर वह वाह्य निमित्त की सहायता की घोपणा करता है, परन्तु उस पक्ष को यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिस समय उपादान अपना कार्य करता है, उसी समय जिसे वाह्य निमित्त कहते हैं, वह स्वयं भी उपादान होकर अपना कार्य करता है। यह एक योग है कि एक के कार्य में कालप्रत्यासत्तिवश दूसरे को निमित्त कहा जाता है। व्यवहार-निश्चय की यही युक्ति है, अन्य सव एकान्त है।
कथन नं. ५४ का समाधान :-इस कथन में समीक्षक ने यह लिखा है कि "उत्तरपक्ष के लेख को मैं गलत इसलिये कहता हूँ कि उसने पूर्वपक्ष पर कार्योत्पत्ति के प्रति कार्यकारी अंतरंग योग्यता को न मानने का उपर्युक्त प्रकार मिथ्या आरोप लगाकर लिखा है" सो उसका ऐसा लिखना इसलिये असंगत है, क्योंकि वह अनेक जगह यह विधान कर आया है कि उपादान हो और अनुकूल निमित्त का सहयोग न मिले तो कार्य आगे-पीछे कभी भी होता है। सो उसके इस कथन से मालूम पड़ता है कि समीक्षक अव्यवहित पूर्वपर्याय युक्त द्रव्य समर्थ उपादान है और जिस समय प्रत्येक वस्तु इस उपादान की भूमिका में पहुंचती है, उस समय उसके अनन्तर समय में नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है और कार्योत्पत्ति के समय अनुकूल वाह्य निमित्त का योग नियम से रहता है । इस कार्यकारण की सम्यक् व्यवस्था को समीक्षक स्वीकार ही नहीं करना चाहता और अपने मिथ्या विकल्पों के अनुसार आगम की इस सम्यक् व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न इस समीक्षा में करता आ रहा है, जैसा कि इस कथन में किया है; अन्यथा उसका भाव इस समीक्षा के लिखने का ही नहीं होता। इसी कथन में समीक्षक ने क्रोध पर्याय का उदाहरण देकर जो उसके अनन्तर समय में मान पर्याय के होने का उदाहरण उपस्थित किया है, सो कार्य-कारण की दृष्टि से वहांपर समर्थ उपादान कारण क्रोधपर्याययुक्त आत्मद्रव्य ही है। इसमें आगम से कोई वाधा नहीं आती। इसकी पुष्टि में हम तत्वार्थश्लोकवार्तिक का एक उद्धरण उपस्थित कर रहे हैं। उससे उक्त बात को स्पष्ट करने में समीक्षक को सहायता मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं -
दर्शनपरिणामपरिणतो आत्मा दर्शनम् । तदुपादानं विशिष्टज्ञानपरिणामस्य निष्पत्तः। पर्यायमात्रस्य निरन्वयस्य जीवादि द्रव्यमात्रस्य च सर्वथोपादनत्वायोगात् कूर्मादिरोमवत् । (पृ. ७५)
अर्थ:-नियम से दर्शन परिणाम से परिणत आत्मा दर्शन है। वह उपादान है, क्योंकि उससे विशिष्ट ज्ञान परिणाम की उत्पत्ति होती है। ऐसा नियम है कि निरन्वय परिणाम मात्र को
और जीवादि द्रव्यमात्र को सर्वथा उपादान होने का प्रयोग है। जैसे कछुवे प्रादि के रोम नही पाये जाते, वैसे ही अन्वयरहित पर्याय को तथा पर्यायरहित द्रव्य को उपादानता नहीं बनती।
इतने स्पष्ट आगमप्रमाण के रहते हुए भी कर्मशास्त्र की दुहाई देकर अपनी मान्यता के अनुसार समर्थ उपादान के कार्यरूप परिणति में वाह्य सामग्री की बलवत्ता को सिद्ध करने का दुष्प्रयत्न यह बतलाता है कि वह पक्ष अपनी मान्यता के आगे आगम को कोई महत्व नहीं देता। इससे अधिक हम उस पक्ष के ऊपर और टिप्पणी क्या करें?