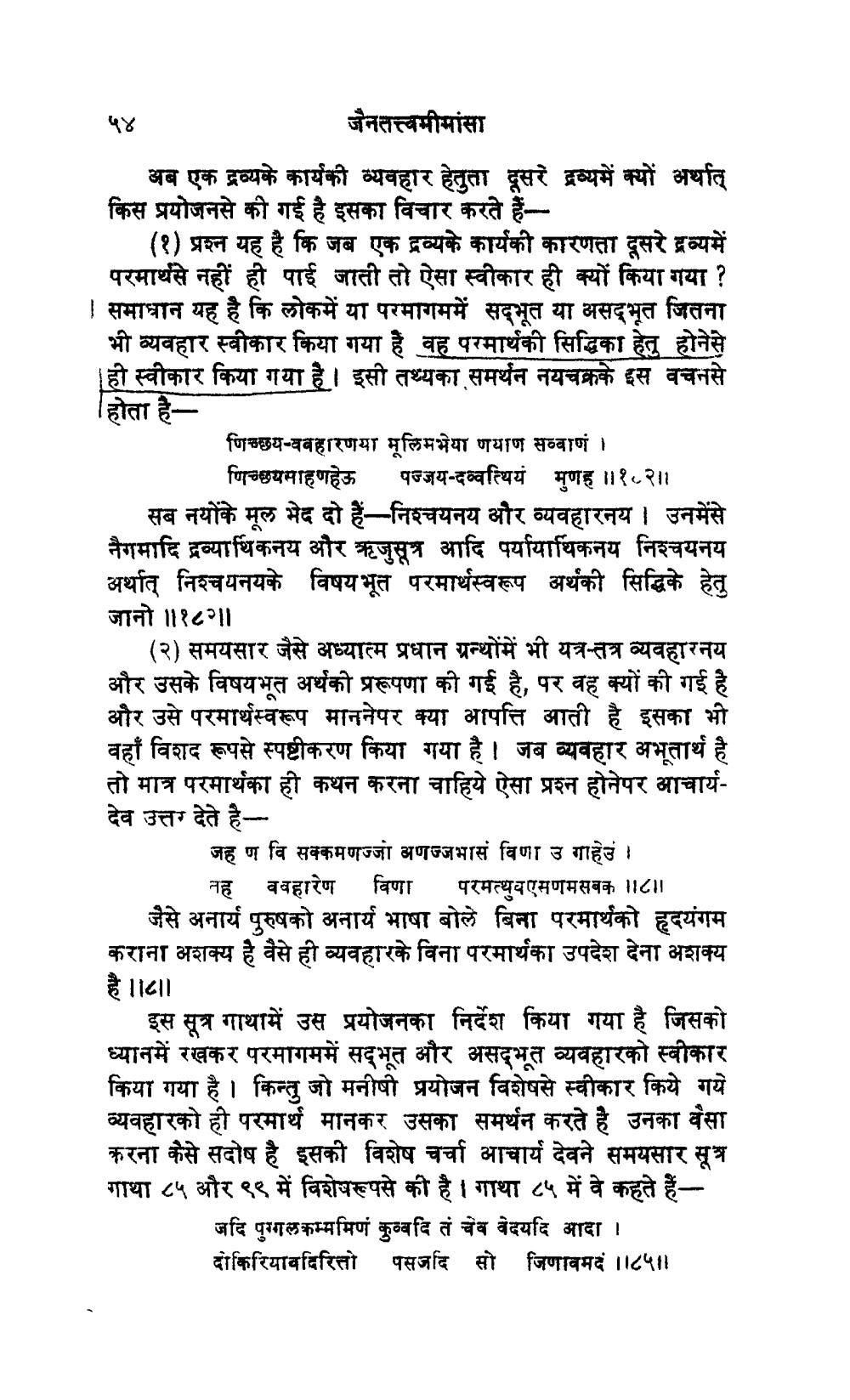________________
५४
जैनतत्त्वमीमांसा अब एक द्रव्यके कार्यकी व्यवहार हेतुता दूसरे द्रव्यमें क्यों अर्थात् किस प्रयोजनसे की गई है इसका विचार करते हैं
(१) प्रश्न यह है कि जब एक द्रव्यके कार्यको कारणता दूसरे द्रव्यमें परमार्थसे नहीं हो पाई जाती तो ऐसा स्वीकार ही क्यों किया गया ? } समाधान यह है कि लोकमें या परमागममें सद्भूत या असद्भूत जितना
भी व्यवहार स्वीकार किया गया है वह परमार्थकी सिद्धिका हेतु होनेसे ही स्वीकार किया गया है। इसी तथ्यका समर्थन नयचक्रके इस वचनसे होता है
णिछछय-ववहारणया मूलिमभेया णयाण सव्वाणं ।
णिच्छयमाहणहेऊ पज्जय-दव्वत्थियं मुणह ॥१८२॥ सब नयोंके मूल भेद दो हैं-निश्चयनय और व्यवहारनय । उनमेंसे नैगमादि द्रव्याथिकनय और ऋजुसूत्र आदि पर्यायार्थिकनय निश्चयनय अर्थात् निश्चयनयके विषयभूत परमार्थस्वरूप अर्थकी सिद्धिके हेतु जानो ॥१८॥
(२) समयसार जैसे अध्यात्म प्रधान ग्रन्थोंमें भी यत्र-तत्र व्यवहारनय और उसके विषयभत अर्थको प्ररूपणा की गई है, पर वह क्यों की गई है और उसे परमार्थस्वरूप माननेपर क्या आपत्ति आती है इसका भी वहाँ विशद रूपसे स्पष्टीकरण किया गया है। जब व्यवहार अभूतार्थ है तो मात्र परमार्थका ही कथन करना चाहिये ऐसा प्रश्न होनेपर आचार्यदेव उत्तर देते है
जह ण वि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहे ।
नह ववहारेण विणा परमत्थुवएमणमसबक ॥८॥ जैसे अनार्य पुरुषको अनार्य भाषा बोले बिना परमार्थको हृदयंगम कराना अशक्य है वैसे ही व्यवहारके विना परमार्थका उपदेश देना अशक्य है।1८॥
इस सूत्र गाथामें उस प्रयोजनका निर्देश किया गया है जिसको ध्यानमें रखकर परमागममें सद्भुत और असद्भत व्यवहारको स्वीकार किया गया है। किन्तु जो मनीषी प्रयोजन विशेषसे स्वीकार किये गये व्यवहारको ही परमार्थ मानकर उसका समर्थन करते है उनका वैसा करना कैसे सदोष है इसकी विशेष चर्चा आचार्य देवने समयसार सूत्र गाथा ८५ और ९९ में विशेषरूपसे की है । गाथा ८५ में वे कहते हैं
जदि पुग्गलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा । दोकिरियावदिरित्तो पसदि सो जिणावमदं ।।८५॥