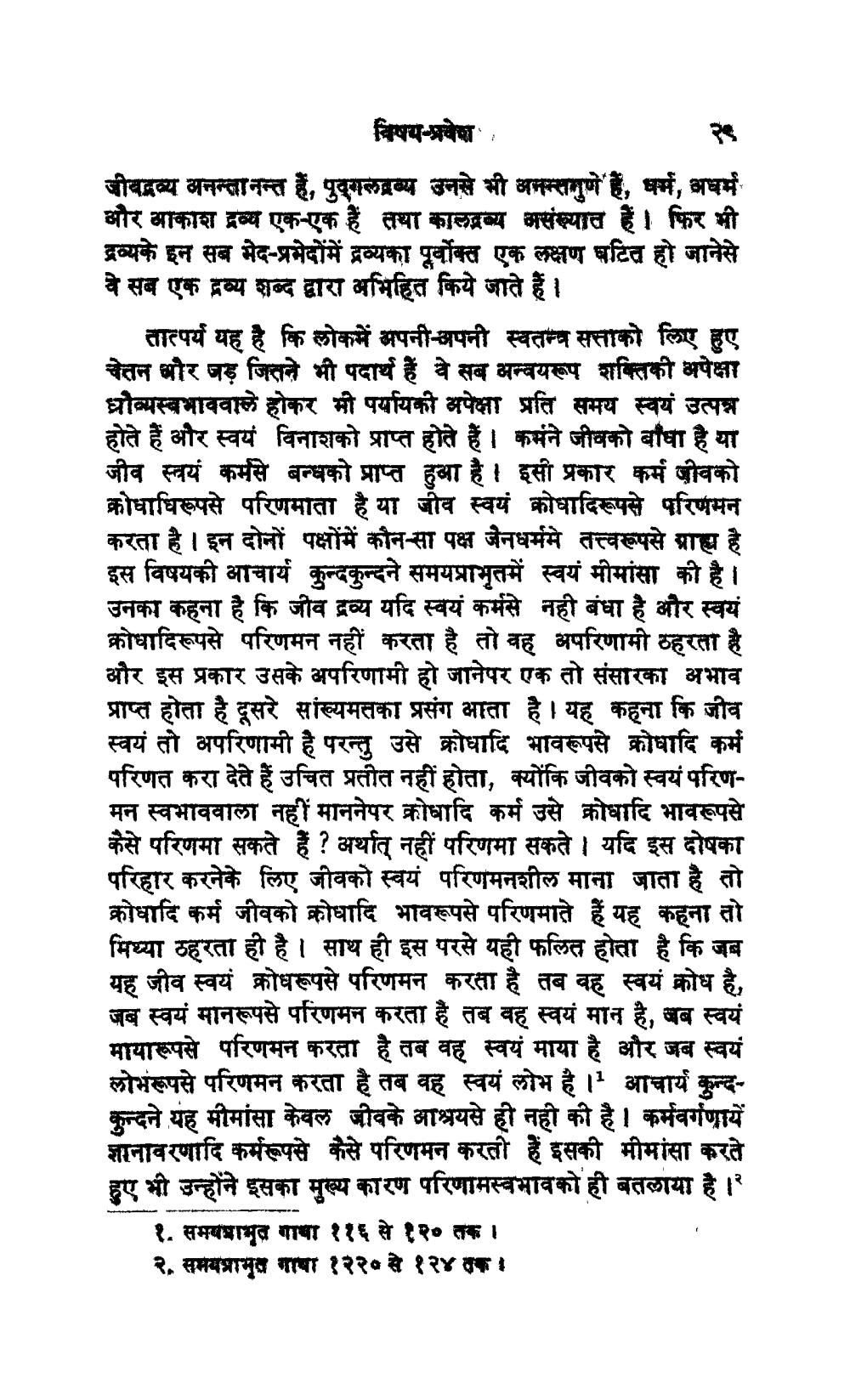________________
विषय-प्रवेषा, जीवद्रव्य अनन्तानन्त हैं, पुद्गलद्रव्य उनसे भी अमन्तगुणें हैं, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य एक-एक हैं तथा कालद्रव्य असंख्यात हैं। फिर भी द्रव्यके इन सब भेद-प्रभेदोंमें द्रव्यका पूर्वोक्त एक लक्षण घटित हो जानेसे वे सब एक द्रव्य शब्द द्वारा अभिहित किये जाते हैं।
तात्पर्य यह है कि लोकमें अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ताको लिए हुए चेतन और जड़ जितने भी पदार्थ हैं वे सब अन्वयरूप शक्तिकी अपेक्षा ध्रौव्यस्वभाववाले होकर मी पर्यायकी अपेक्षा प्रति समय स्वयं उत्पन्न होते हैं और स्वयं विनाशको प्राप्त होते हैं। कर्मने जीवको बाँधा है या जीव स्वयं कर्मसे बन्धको प्राप्त हुवा है। इसी प्रकार कर्म जीवको क्रोधाधिरूपसे परिणमाता है या जीव स्वयं क्रोधादिरूपसे परिणमन करता है । इन दोनों पक्षोंमें कौन-सा पक्ष जैनधर्ममे तत्त्वरूपसे ग्राह्य है इस विषयकी आचार्य कुन्दकुन्दने समयप्राभृतमें स्वयं मीमांसा की है। उनका कहना है कि जीव द्रव्य यदि स्वयं कर्मसे नही बंधा है और स्वयं क्रोधादिरूपसे परिणमन नहीं करता है तो वह अपरिणामी ठहरता है और इस प्रकार उसके अपरिणामी हो जानेपर एक तो संसारका अभाव प्राप्त होता है दूसरे सांख्यमतका प्रसंग आता है। यह कहना कि जीव स्वयं तो अपरिणामी है परन्तु उसे क्रोधादि भावरूपसे क्रोधादि कर्म परिणत करा देते हैं उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जीवको स्वयं परिणमन स्वभाववाला नहीं माननेपर क्रोधादि कर्म उसे क्रोधादि भावरूपसे कैसे परिणमा सकते हैं ? अर्थात् नहीं परिणमा सकते । यदि इस दोषका परिहार करनेके लिए जीवको स्वयं परिणमनशील माना जाता है तो क्रोधादि कर्म जीवको क्रोधादि भावरूपसे परिणमाते हैं यह कहना तो मिथ्या ठहरता ही है। साथ ही इस परसे यही फलित होता है कि जब यह जीव स्वयं क्रोधरूपसे परिणमन करता है तब वह स्वयं क्रोध है, जब स्वयं मानरूपसे परिणमन करता है तब वह स्वयं मान है, बब स्वयं मायारूपसे परिणमन करता है तब वह स्वयं माया है और जब स्वयं लोभरूपसे परिणमन करता है तब वह स्वयं लोभ है । आचार्य कुन्दकुन्दने यह मीमांसा केवल जीवके आश्रयसे ही नहीं की है। कर्मवर्गणायें ज्ञानावरणादि कर्मरूपसे कैसे परिणमन करती हैं इसकी मीमांसा करते हुए भी उन्होंने इसका मुख्य कारण परिणामस्वभावको ही बतलाया है।
१. समवशाभूत गाषा ११६ से १२० तक । २. समवप्रामृत गापा १२२० से १२४ तक।