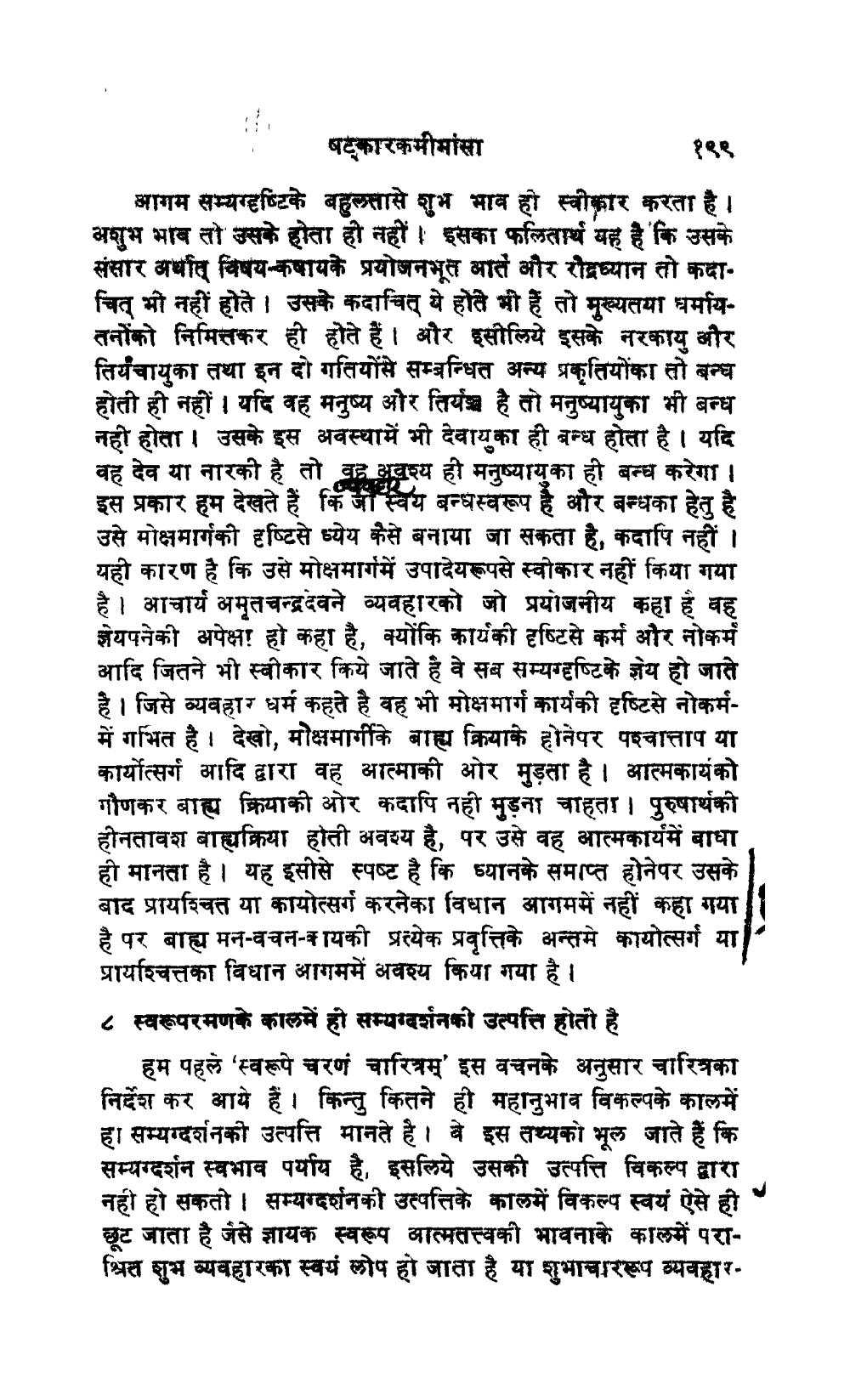________________
षट्कारकमीमांसा
१९९
आगम सम्यग्दृष्टिके बहुलतासे शुभ भाव ही स्वीकार करता है । अशुभ भाव तो उसके होता ही नहीं। इसका फलितार्थ यह है कि उसके संसार अर्थात् विषय कषायके प्रयोजनभूत आते और रोद्रध्यान तो कदाचित् भी नहीं होते। उसके कदाचित् ये होते भी हैं तो मुख्यतया धर्मायतनोंको निमित्तकर ही होते हैं । और इसीलिये इसके नरकायु और तिर्यंचायुका तथा इन दो गतियोंसे सम्बन्धित अन्य प्रकृतियोंका तो बन्ध होती ही नहीं । यदि वह मनुष्य और तिर्यश्च है तो मनुष्यायुका भी बन्ध नहीं होता । उसके इस अवस्था में भी देवायुका ही बन्ध होता है । यदि
वह देव या नारकी है ताश्य ही मनुष्यायुका ही बन्ध करेगा ।
वह
इस प्रकार हम देखते हैं किं बन्धस्वरूप है और बन्धका हेतु है उसे मोक्षमार्गको दृष्टिसे ध्येय कैसे बनाया जा सकता है, कदापि नहीं । यही कारण है कि उसे मोक्षमार्गमें उपादेयरूपसे स्वीकार नहीं किया गया है । आचार्य अमृतचन्द्रदेवने व्यवहारको जो प्रयोजनीय कहा है वह ज्ञेयपनेकी अपेक्षा हो कहा है, क्योंकि कार्यकी दृष्टिसे कर्म और नोकर्म आदि जितने भी स्वीकार किये जाते है वे सब सम्यग्दृष्टि के ज्ञेय हो जाते है । जिसे व्यवहार धर्म कहते है वह भी मोक्षमार्ग कार्यकी दृष्टिसे नोकर्ममें गति है । देखो, मोक्षमार्गीके बाह्य क्रियाके होनेपर पश्चात्ताप या कार्योत्सर्ग आदि द्वारा वह आत्माकी ओर मुड़ता है । आत्मकार्यको गौणकर बाह्य क्रियाकी ओर कदापि नही मुड़ना चाहता । पुरुषार्थकी हीनतावश बाह्यक्रिया होती अवश्य है, पर उसे वह आत्मकार्य में बाधा ही मानता है । यह इसीसे स्पष्ट है कि ध्यानके समाप्त होनेपर उसके बाद प्रायश्चित या कायोत्सर्ग करनेका विधान आगममें नहीं कहा गया है पर बाह्य मन-वचन-कायकी प्रत्येक प्रवृत्तिके अन्तमे कायोत्सर्ग या प्रायश्चित्तका विधान आगममें अवश्य किया गया है ।
८ स्वरूपरमणके कालमें हो सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होती है
हम पहले 'स्वरूपे चरणं चारित्रम्' इस वचनके अनुसार चारित्रका निर्देश कर आये हैं । किन्तु कितने ही महानुभाव विकल्पके कालमें हा सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति मानते है । वे इस तथ्यको भूल जाते हैं कि सम्यग्दर्शन स्वभाव पर्याय है, इसलिये उसकी उत्पत्ति विकल्प द्वारा नही हो सकती । सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिके कालमें विकल्प स्वयं ऐसे ही छूट जाता है जैसे ज्ञायक स्वरूप आत्मतत्त्वकी भावनाके कालमें पराश्रित शुभ व्यवहारका स्वयं लोप हो जाता है या शुभाचाररूप व्यवहार
-