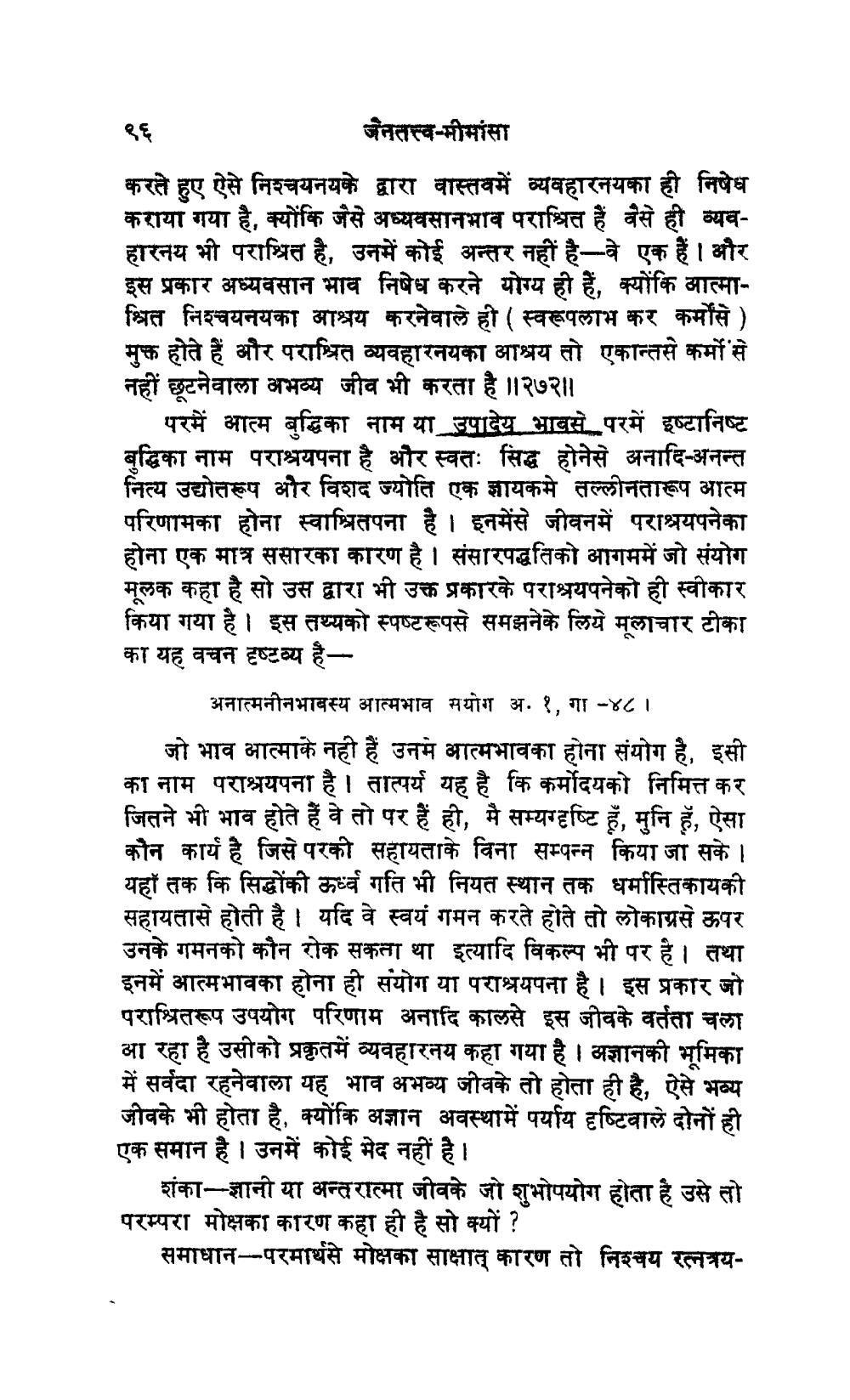________________
जनतत्त्व-मीमांसा करते हुए ऐसे निश्चयनयके द्वारा वास्तवमें व्यवहारनयका ही निषेध कराया गया है, क्योंकि जैसे अध्यवसानभाव पराश्रित हैं वैसे ही व्यवहारनय भी पराश्रित है, उनमें कोई अन्तर नहीं है-वे एक हैं। और इस प्रकार अध्यवसान भाव निषेध करने योग्य ही हैं, क्योंकि आत्माश्रित निश्चयनयका आश्रय करनेवाले ही ( स्वरूपलाभ कर कर्मोसे) मुक्त होते हैं और पराश्रित व्यवहारनयका आश्रय तो एकान्तसे कर्मों से नहीं छूटनेवाला अभव्य जीव भी करता है ॥२७२॥
परमें आत्म बुद्धिका नाम या उपादेय भावसे परमें इष्टानिष्ट बुद्धिका नाम पराश्रयपना है और स्वतः सिद्ध होनेसे अनादि-अनन्त नित्य उद्योतरूप और विशद ज्योति एक ज्ञायकमे तल्लीनतारूप आत्म परिणामका होना स्वाश्रितपना है। इनमेंसे जीवनमें पराश्रयपनेका होना एक मात्र ससारका कारण है । संसारपद्धतिको आगममें जो संयोग मूलक कहा है सो उस द्वारा भी उक्त प्रकारके पराश्रयपनेको ही स्वीकार किया गया है। इस तथ्यको स्पष्टरूपसे समझनेके लिये मूलाचार टीका का यह वचन दृष्टव्य है
अनात्मनीनभावस्य आत्मभाव मयोग अ. १, गा -४८ । जो भाव आत्माके नही हैं उनमे आत्मभावका होना संयोग है, इसी का नाम पराश्रयपना है। तात्पर्य यह है कि कर्मोदयको निमित्त कर जितने भी भाव होते हैं वे तो पर हैं ही, मै सम्यग्दृष्टि हूँ, मुनि हुँ, ऐसा कौन कार्य है जिसे परकी सहायताके विना सम्पन्न किया जा सके। यहाँ तक कि सिद्धोंकी ऊर्ध्व गति भी नियत स्थान तक धर्मास्तिकायकी सहायतासे होती है। यदि वे स्वयं गमन करते होते तो लोकाग्रसे ऊपर उनके गमनको कौन रोक सकता था इत्यादि विकल्प भी पर है। तथा इनमें आत्मभावका होना ही संयोग या पराश्रयपना है। इस प्रकार जो पराश्रितरूप उपयोग परिणाम अनादि कालसे इस जीवके वर्तता चला आ रहा है उसीको प्रकृतमें व्यवहारनय कहा गया है । अज्ञानकी भूमिका में सर्वदा रहनेवाला यह भाव अभव्य जीवके तो होता ही है, ऐसे भव्य जीवके भी होता है, क्योंकि अज्ञान अवस्थामें पर्याय दृष्टिवाले दोनों ही एक समान है। उनमें कोई भेद नहीं है।
शंका-ज्ञानी या अन्तरात्मा जीवके जो शुभोपयोग होता है उसे तो परम्परा मोक्षका कारण कहा ही है सो क्यों ?
समाधान-परमार्थसे मोक्षका साक्षात् कारण तो निश्चय रत्नत्रय