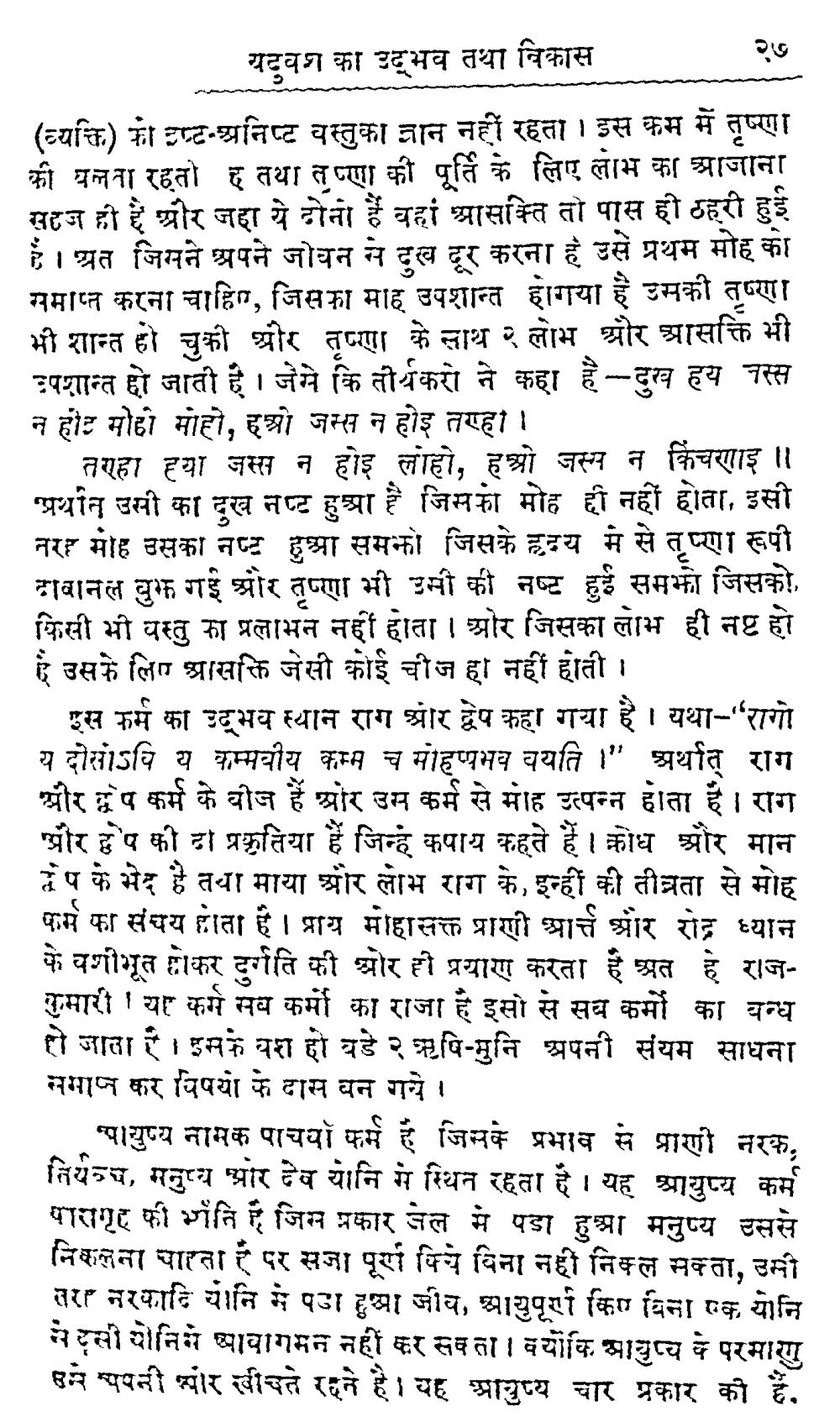________________
यदवश का उद्भव तथा विकास
(व्यक्ति) को इष्ट-अनिष्ट वस्तुका नान नहीं रहता । इस क्रम में तृष्णा की चलता रहतो ह तथा त प्णा की पूर्ति के लिए लाभ का आजाना सहज ही है और जहा ये दोनो हैं वहां आसक्ति तो पास ही ठहरी हुई है । अत जिमने अपने जोवन ने दुख दूर करना है उसे प्रथम मोह को समाप्त करना चाहिए, जिसका माह उपशान्त होगया है उसकी तष्णा भी शान्त हो चुकी श्रीर तणा के साथ २ लोभ और आसक्ति भी उपशान्त हो जाती है । जेमे कि तीर्थकरो ने कहा है -दुख हय नस्स न होट मोहो मोहो, हो जस्स न होइ तरहा। __तरहा हया जसस न होइ लाहो, हो जस्म न किंचणाइ ।। "प्रर्थात उसी का दुख नष्ट हुआ है जिसको मोह ही नहीं होता, इसी नरह मोह उसका नष्ट हुआ समझो जिसके हृदय में से तृप्णा रूपी दावानल बुझ गई और तष्णा भी उनी की नष्ट हुई समझो जिसको, किसी भी वस्तु का प्रलाभन नहीं होता । और जिसका लाभ ही नष्ट हो है उसके लिए प्रासक्ति जेसी कोई चीज हा नहीं होती।
इस कर्म का उद्भव स्थान राग और द्वेष कहा गया है । यथा-"रागो य दोसांऽपि य कम्मवीय कम्म च मोहप्पभव वयति ।" अर्थात् राग
और द्वेष कर्म के बीज है और उस कर्म से मोह उत्पन्न होता है। राग "पौर हप की दो प्रकृतिया हैं जिन्हें कपाय कहते हैं। क्रोध और मान दंप के भेद है तथा माया और लोभ राग के, इन्हीं की तीव्रता से मोह फार्म का संचय होता है । प्राय मोहासक्त प्राणी प्रार्त और रोद्र ध्यान के वशीभूत होकर दुर्गति की ओर ही प्रयाण करता है अत हे राजसुमारी । या कर्म सब कर्मो का राजा है इसो से सब कर्मों का बन्ध हो जाता है। इसके वश हो बडे २ ऋषि-मुनि अपनी संयम साधना समाप्त कर विषयों के दास बन गये।
पायुप्य नामक पाचयों फर्म है जिसके प्रभाव से प्राणी नरक, निर्यच, मनुष्य 'पोर देव योनि में स्थित रहता है । यह श्रायुप्य कर्म पारागृह की गति है जिन प्रकार जेल में पड़ा हुआ मनुष्य उससे निकलना चारतारे पर सजा पूर्ण किये बिना नहीं निकल सक्ता, उनी सरा नरकादि योनि में पड़ा हुआ जीव, श्रायुपूर्ण किए बिना एक योनि मंदसी योनि यावागमन नहीं कर सकता। क्योंकि आयुप्य वे परमाणु हरे पपनी यार खीचते रहने है। यह प्रायुप्य चार प्रकार की हैं.