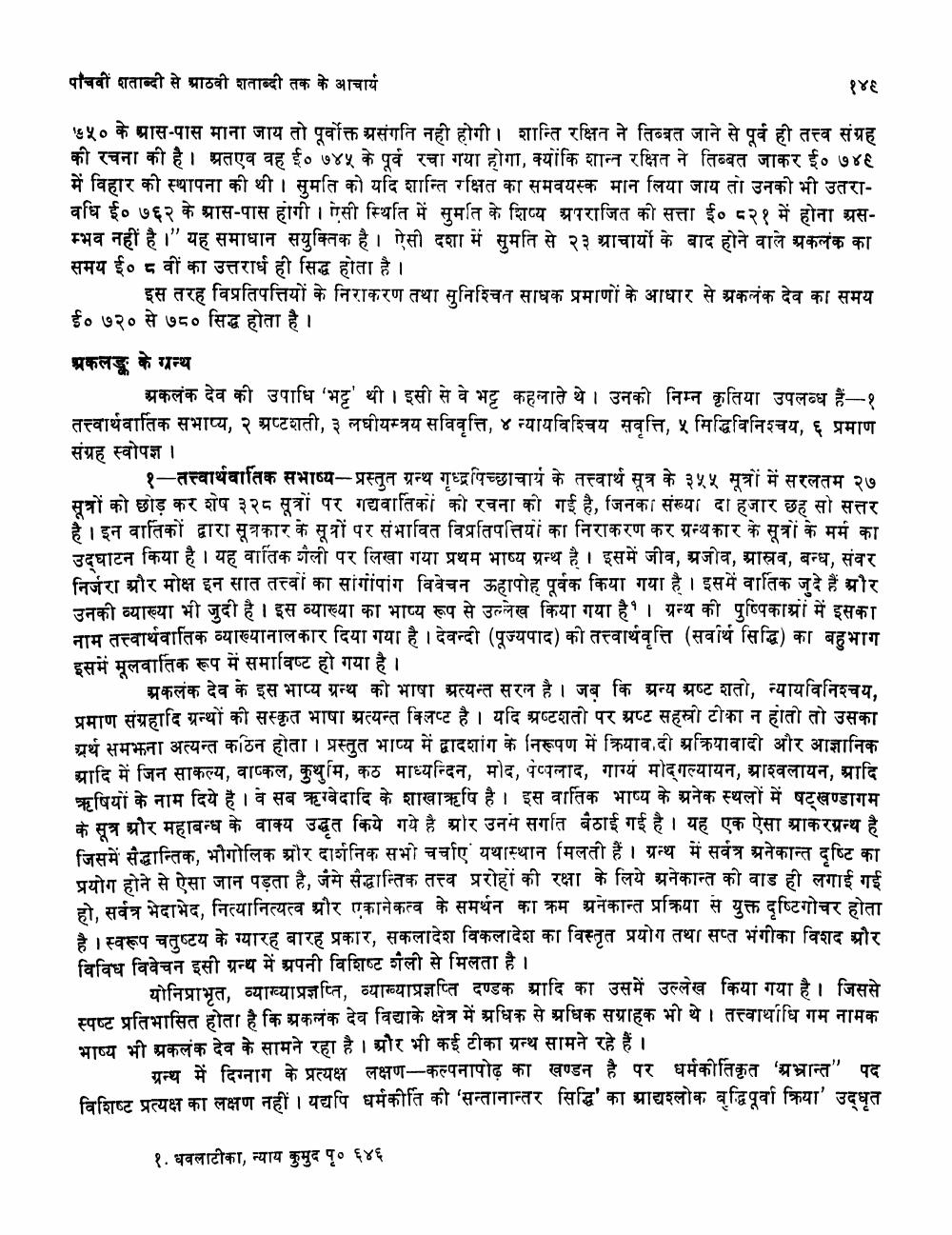________________
पांचवीं शताब्दी से पाठवी शताब्दी तक के आचार्य
१४६
७५० के पास-पास माना जाय तो पूर्वोक्त असंगति नही होगी। शान्ति रक्षित ने तिब्बत जाने से पूर्व ही तत्त्व संग्रह की रचना की है। अतएव वह ई० ७४५ के पूर्व रचा गया होगा, क्योंकि शान्त रक्षित ने तिब्बत जाकर ई० ७४६ में विहार की स्थापना की थी। सुमति को यदि शान्ति रक्षित का समवयस्क मान लिया जाय तो उनको भी उतरावधि ई० ७६२ के पास-पास होगी। ऐसी स्थिति में सुमति के शिष्य अपराजित को सत्ता ई०८२१ में होना असम्भव नहीं है।" यह समाधान सयुक्तिक है। ऐसी दशा में सूमति से २३ प्राचार्यों के बाद होने वाले अकलंक का समय ई०८ वीं का उत्तरार्ध ही सिद्ध होता है।
इस तरह विप्रतिपत्तियों के निराकरण श्चित साधक प्रमाणों के आधार से अकलंक देव का समय ई० ७२० से ७८० सिद्ध होता है । प्रकलङ्क के ग्रन्थ
अकलंक देव की उपाधि 'भट्ट' थी। इसी से वे भट्ट कहलाते थे। उनको निम्न कृतिया उपलब्ध हैं-१ तत्त्वार्थवातिक सभाप्य, २ अप्टशती, ३ लघीयस्त्रय सविवृत्ति, ४ न्यायविश्चिय सवृत्ति, ५ सिद्धिविनिश्चय, ६ प्रमाण संग्रह स्वोपज्ञ।
१-तत्त्वार्थवातिक सभाष्य-प्रस्तुत ग्रन्थ गृध्द्रपिच्छाचार्य के तत्त्वार्थ सूत्र के ३५५ सूत्रों में सरलतम २७ सूत्रों को छोड़ कर शेष ३२८ सूत्रों पर गद्यवार्तिकों को रचना की गई है, जिनका संख्या दा हजार छह सो सत्तर है। इन वार्तिकों द्वारा सूत्रकार के सूत्रों पर संभावित विप्रतिपत्तियों का निराकरण कर ग्रन्थकार के सूत्रों के मर्म का उद्घाटन किया है । यह वार्तिक शैली पर लिखा गया प्रथम भाष्य ग्रन्थ है । इसमें जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों का सांगोपांग विवेचन ऊहापोह पूर्वक किया गया है। इसमें वार्तिक जदे हैं और उनकी व्याख्या भी जुदी है । इस व्याख्या का भाष्य रूप से उल्लेख किया गया है । ग्रन्थ की पुष्पिकाओं में इसका नाम तत्त्वार्थवातिक व्याख्यानालकार दिया गया है । देवन्दी (पूज्यपाद) की तत्त्वार्थवृत्ति (सर्वार्थ सिद्धि) का बहुभाग इसमें मलवातिक रूप में समाविष्ट हो गया है।
अकलंक देव के इस भाप्य ग्रन्थ को भाषा अत्यन्त सरल है। जब कि अन्य प्रष्ट शतो, न्यायविनिश्चय, प्रमाण संग्रहादि ग्रन्थों की सस्कृत भाषा अत्यन्त क्लिष्ट है। यदि अष्टशती पर अष्ट सहस्रो टोका न होती तो उसका अर्थ समझना अत्यन्त कठिन होता । प्रस्तुत भाग्य में द्वादशांग के निरूपण में क्रियावादी प्रक्रियावादी और आज्ञानिक प्रादि में जिन साकल्य, वाकल, कुथुमि, कठ माध्यन्दिन, मोद, पप्पलाद, गाग्यं मोद्गल्यायन, प्राश्वलायन, आदि ऋषियों के नाम दिये है। वे सब ऋग्वेदादि के शाखाऋषि है। इस वार्तिक भाष्य के अनेक स्थलों में षट्खण्डागम के सूत्र और महाबन्ध के वाक्य उद्धृत किये गये है ओर उनमे सति बैठाई गई है। यह एक ऐसा आकरग्रन्थ है जिसमें सैद्धान्तिक, भौगोलिक और दार्शनिक सभी चर्चाए यथास्थान मिलती हैं। ग्रन्थ में सर्वत्र अनेकान्त दष्टि का प्रयोग होने से ऐसा जान पड़ता है, जैसे सैद्धान्तिक तत्त्व प्ररोहों की रक्षा के लिये अनेकान्त को वाड ही लगाई गई हो, सर्वत्र भेदाभेद, नित्यानित्यत्व और एकानेकत्व के समर्थन का क्रम अनेकान्त प्रक्रिया से युक्त दृष्टिगोचर होता है । स्वरूप चतुष्टय के ग्यारह बारह प्रकार, सकलादेश विकलादेश का विस्तृत प्रयोग तथा सप्त भंगीका विशद और विविध विवेचन इसी ग्रन्थ में अपनी विशिष्ट शैली से मिलता है।
योनिप्राभूत, व्याख्याप्रज्ञप्ति, व्याख्याप्रज्ञप्ति दण्डक आदि का उसमें उल्लेख किया गया है। जिससे स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि अकलंक देव विद्याके क्षेत्र में अधिक से अधिक सग्राहक भी थे। तत्त्वार्थाधि गम नामक भाष्य भी अकलंक देव के सामने रहा है। और भी कई टीका ग्रन्थ सामने रहे हैं।
ग्रन्थ में दिग्नाग के प्रत्यक्ष लक्षण-कल्पनापोढ़ का खण्डन है पर धर्मकीतिकृत 'अभ्रान्त" पद विशिष्ट प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं । यद्यपि धर्मकीर्ति की 'सन्तानान्तर सिद्धि' का आद्यश्लोक बुद्धिपूर्वा क्रिया' उद्धत
१. धवलाटीका, न्याय कुमुद पृ० ६४६