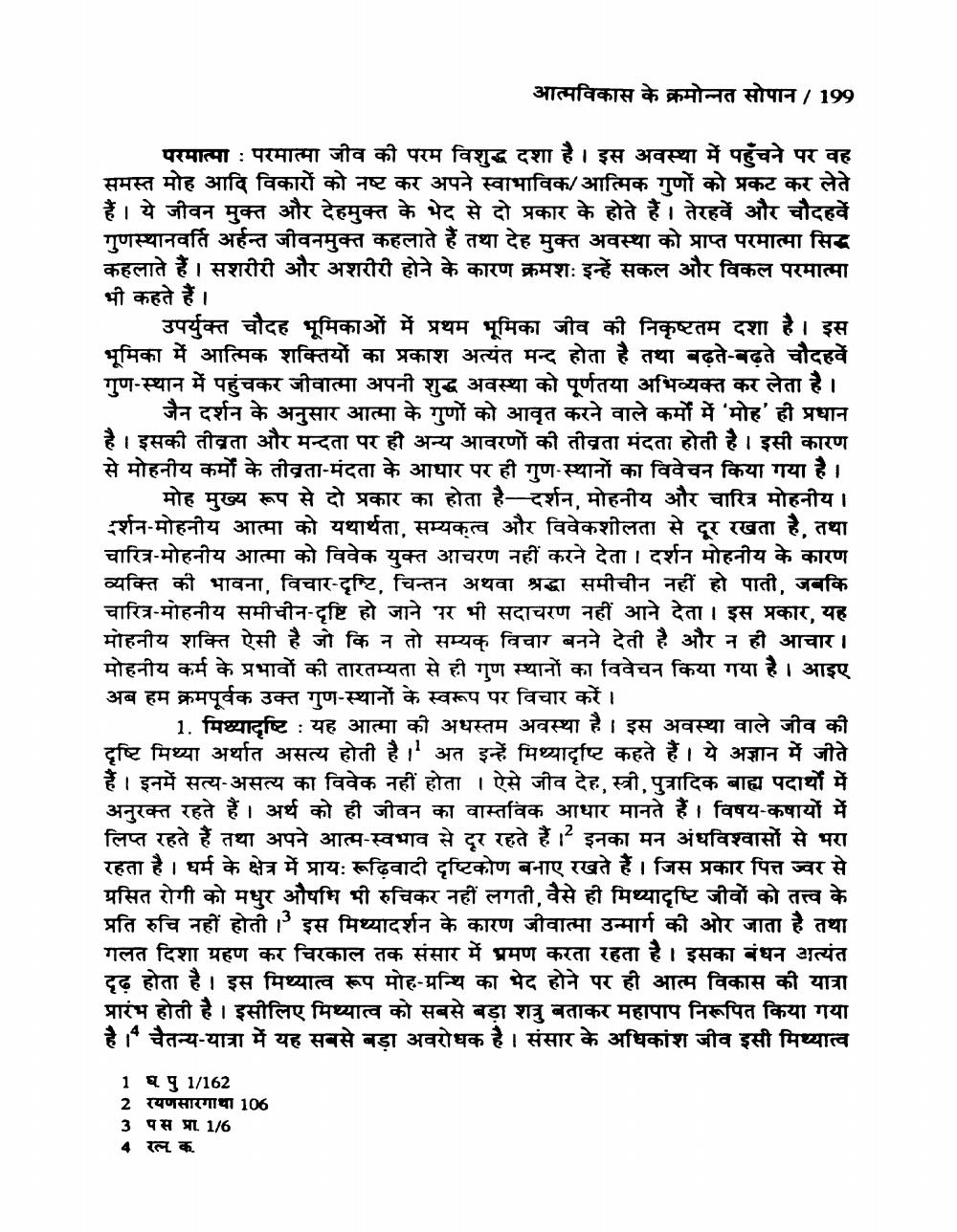________________
आत्मविकास के क्रमोन्नत सोपान / 199
परमात्मा : परमात्मा जीव की परम विशुद्ध दशा है। इस अवस्था में पहुँचने पर वह समस्त मोह आदि विकारों को नष्ट कर अपने स्वाभाविक / आत्मिक गुणों को प्रकट कर लेते हैं। ये जीवन मुक्त और देहमुक्त के भेद से दो प्रकार के होते हैं। तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ति अर्हन्त जीवनमुक्त कहलाते हैं तथा देह मुक्त अवस्था को प्राप्त परमात्मा सिद्ध कहलाते हैं । सशरीरी और अशरीरी होने के कारण क्रमशः इन्हें सकल और विकल परमात्मा भी कहते हैं
।
उपर्युक्त चौदह भूमिकाओं में प्रथम भूमिका जीव की निकृष्टतम दशा है। इस भूमिका में आत्मिक शक्तियों का प्रकाश अत्यंत मन्द होता है तथा बढ़ते-बढ़ते चौदहवें गुण-स्थान में पहुंचकर जीवात्मा अपनी शुद्ध अवस्था को पूर्णतया अभिव्यक्त कर लेता है । जैन दर्शन के अनुसार आत्मा के गुणों को आवृत करने वाले कर्मों में 'मोह' ही प्रधान है। इसकी तीव्रता और मन्दता पर ही अन्य आवरणों की तीव्रता मंदता होती है । इसी कारण से मोहनीय कर्मों के तीव्रता-मंदता के आधार पर ही गुण-स्थानों का विवेचन किया गया है। मोह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है— दर्शन, मोहनीय और चारित्र मोहनीय | दर्शन - मोहनीय आत्मा को यथार्थता, सम्यकृत्व और विवेकशीलता से दूर रखता है, तथा चारित्र - मोहनीय आत्मा को विवेक युक्त आचरण नहीं करने देता । दर्शन मोहनीय के कारण व्यक्ति की भावना, विचार-दृष्टि, चिन्तन अथवा श्रद्धा समीचीन नहीं हो पाती, जबकि चारित्र - मोहनीय समीचीन दृष्टि हो जाने पर भी सदाचरण नहीं आने देता। इस प्रकार, यह मोहनीय शक्ति ऐसी है जो कि न तो सम्यक् विचार बनने देती है और न ही आचार । मोहनीय कर्म के प्रभावों की तारतम्यता से ही गुण स्थानों का विवेचन किया गया है। आइए अब हम क्रमपूर्वक उक्त गुण-स्थानों के स्वरूप पर विचार करें।
1. मिथ्यादृष्टि: यह आत्मा की अधस्तम अवस्था है। इस अवस्था वाले जीव की दृष्टि मिथ्या अर्थात असत्य होती है।' अत इन्हें मिथ्यादृष्टि कहते हैं। ये अज्ञान में जीते हैं। इनमें सत्य-असत्य का विवेक नहीं होता । ऐसे जीव देह, स्त्री, पुत्रादिक बाह्य पदार्थों में अनुरक्त रहते हैं । अर्थ को ही जीवन का वास्तविक आधार मानते हैं। विषय- कषायों में लिप्त रहते हैं तथा अपने आत्म-स्वभाव से दूर रहते हैं । 2 इनका मन अंधविश्वासों से भरा रहता है। धर्म के क्षेत्र में प्रायः रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। जिस प्रकार पित्त ज्वर से प्रसित रोगी को मधुर औषधि भी रुचिकर नहीं लगती, वैसे ही मिथ्यादृष्टि जीवों को तत्त्व के प्रति रुचि नहीं होती । इस मिथ्यादर्शन के कारण जीवात्मा उन्मार्ग की ओर जाता है तथा गलत दिशा ग्रहण कर चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता रहता है। इसका बंधन अत्यंत दृढ़ होता है। इस मिथ्यात्व रूप मोह-प्रन्थि का भेद होने पर ही आत्म विकास की यात्रा प्रारंभ होती है । इसीलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा शत्रु बताकर महापाप निरूपित किया गया है । 4 चैतन्य यात्रा में यह सबसे बड़ा अवरोधक है। संसार के अधिकांश जीव इसी मिथ्यात्व
1पु1/162
2 रयणसारगाथा 106
3 प स प्रा. 1/6
4 रत्न क.