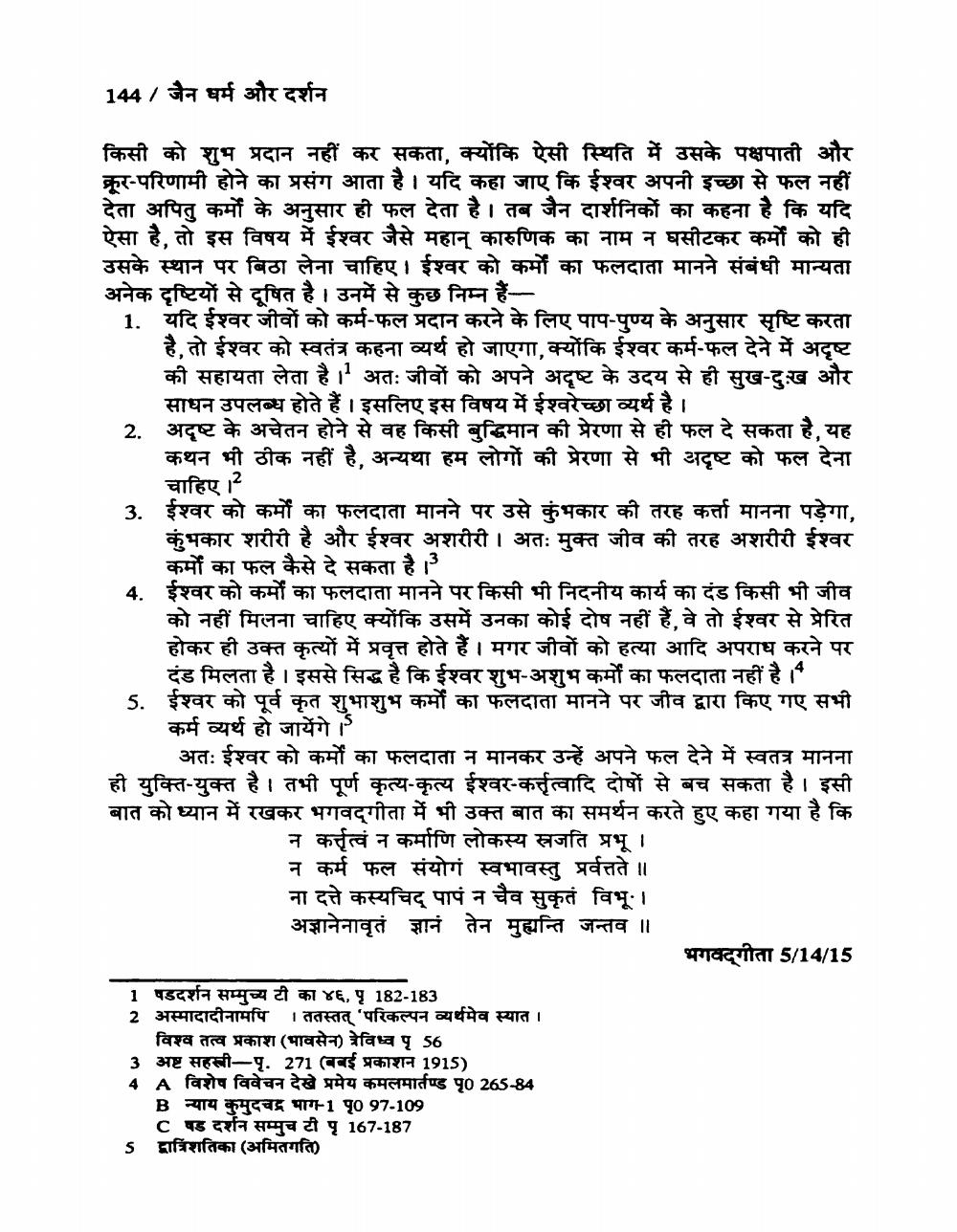________________
144 / जैन धर्म और दर्शन
किसी को शुभ प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके पक्षपाती और क्रूर-परिणामी होने का प्रसंग आता है। यदि कहा जाए कि ईश्वर अपनी इच्छा से फल नहीं देता अपितु कर्मों के अनुसार ही फल देता है। तब जैन दार्शनिकों का कहना है कि यदि ऐसा है, तो इस विषय में ईश्वर जैसे महान् कारुणिक का नाम न घसीटकर कों को ही उसके स्थान पर बिठा लेना चाहिए। ईश्वर को कर्मों का फलदाता मानने संबंधी मान्यता अनेक दृष्टियों से दूषित है। उनमें से कुछ निम्न हैं1. यदि ईश्वर जीवों को कर्म-फल प्रदान करने के लिए पाप-पुण्य के अनुसार सृष्टि करता
है, तो ईश्वर को स्वतंत्र कहना व्यर्थ हो जाएगा,क्योंकि ईश्वर कर्म-फल देने में अदृष्ट की सहायता लेता है। अत: जीवों को अपने अदृष्ट के उदय से ही सुख-दुःख और
साधन उपलब्ध होते हैं । इसलिए इस विषय में ईश्वरेच्छा व्यर्थ है। 2. अदृष्ट के अचेतन होने से वह किसी बुद्धिमान की प्रेरणा से ही फल दे सकता है, यह
कथन भी ठीक नहीं है, अन्यथा हम लोगों की प्रेरणा से भी अदृष्ट को फल देना
चाहिए। 3. ईश्वर को कर्मों का फलदाता मानने पर उसे कुंभकार की तरह कर्ता मानना पड़ेगा,
कुंभकार शरीरी है और ईश्वर अशरीरी। अतः मुक्त जीव की तरह अशरीरी ईश्वर
कर्मों का फल कैसे दे सकता है। 4. ईश्वर को कर्मों का फलदाता मानने पर किसी भी निदनीय कार्य का दंड किसी भी जीव
को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसमें उनका कोई दोष नहीं हैं वे तो ईश्वर से प्रेरित होकर ही उक्त कृत्यों में प्रवृत्त होते हैं। मगर जीवों को हत्या आदि अपराध करने पर
दंड मिलता है । इससे सिद्ध है कि ईश्वर शुभ-अशुभ कर्मों का फलदाता नहीं है। 5. ईश्वर को पूर्व कृत शुभाशुभ कर्मों का फलदाता मानने पर जीव द्वारा किए गए सभी
कर्म व्यर्थ हो जायेंगे।
अतः ईश्वर को कर्मों का फलदाता न मानकर उन्हें अपने फल देने में स्वतत्र मानना ही युक्ति-युक्त है। तभी पूर्ण कृत्य-कृत्य ईश्वर-कर्तृत्वादि दोषों से बच सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवद्गीता में भी उक्त बात का समर्थन करते हुए कहा गया है कि
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य स्रजति प्रभू । न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रर्वत्तते । ना दत्ते कस्यचिद् पापं न चैव सुकृतं विभूः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव ॥
भगवद्गीता 5/14/15
1 षडदर्शन सम्मुच्य टी का ४६, पृ 182-183 2 अस्मादादीनामपि । ततस्तत् 'परिकल्पन व्यर्थमेव स्यात ।
विश्व तत्व प्रकाश (भावसेन) विध्व पृ 56 3 अष्ट सहखी-पृ. 271 (बबई प्रकाशन 1915) 4 A विशेष विवेचन देखे प्रमेय कमलमार्तण्ड पृ0 265-84
B न्याय कुमुदचद्र भाग-1 पृ097-109
C पड दर्शन सम्मुच टी पृ 167-187 5 द्वात्रिंशतिका (अमितगति)