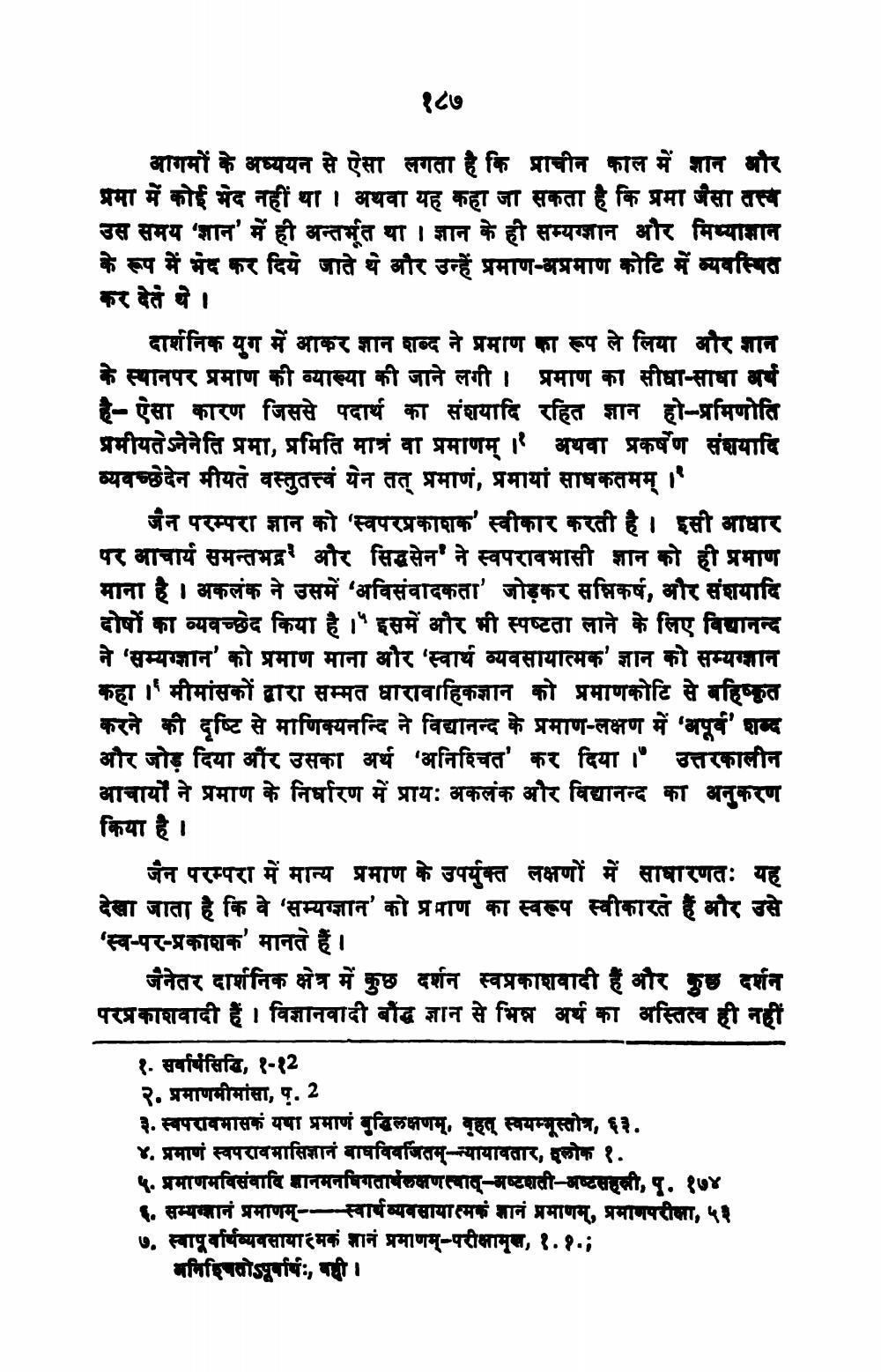________________
१८७
आगमों के अध्ययन से ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में शान और प्रमा में कोई भेद नहीं था । अथवा यह कहा जा सकता है कि प्रमा जैसा तत्व उस समय 'ज्ञान' में ही अन्तर्भूत था । ज्ञान के ही सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान के रूप में भेद कर दिये जाते थे और उन्हें प्रमाण अप्रमाण कोटि में व्यवस्थित कर देते थे ।
दार्शनिक युग में आकर ज्ञान शब्द ने प्रमाण का रूप ले लिया और ज्ञान के स्थानपर प्रमाण की व्याख्या की जाने लगी । प्रमाण का सीधा-साधा अर्थ है - ऐसा कारण जिससे पदार्थ का संशयादि रहित ज्ञान हो - प्रमिणोति प्रमीयतेऽनेनेति प्रमा, प्रमिति मात्रं वा प्रमाणम् । अथवा प्रकर्षेण संशयादि व्यवच्छेदेन मीयतं वस्तुतत्त्वं येन तत् प्रमाणं, प्रमायां साधकतमम् ।
1
जैन परम्परा ज्ञान को 'स्वपरप्रकाशक' स्वीकार करती है । इसी आधार पर आचार्य समन्तभद्र और सिद्धसेन ने स्वपरावभासी ज्ञान को ही प्रमाण माना है । अकलंक ने उसमें 'अविसंवादकता' जोड़कर सन्निकर्ष, और संशयादि दोषों का व्यवच्छेद किया है ।" इसमें और भी स्पष्टता लाने के लिए विद्यानन्द ने 'सम्यग्ज्ञान' को प्रमाण माना और 'स्वार्थ व्यवसायात्मक' ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहा ।' मीमांसकों द्वारा सम्मत धारावाहिकज्ञान को प्रमाणकोटि से बहिष्कृत करने की दृष्टि से माणिक्यनन्दि ने विद्यानन्द के प्रमाण - लक्षण में 'अपूर्व' शब्द और जोड़ दिया और उसका अर्थ 'अनिश्चित' कर दिया । उत्तरकालीन आचार्यों ने प्रमाण के निर्धारण में प्राय: अकलंक और विद्यानन्द का अनुकरण किया है ।
जैन परम्परा में मान्य प्रमाण के उपर्युक्त लक्षणों में साधारणतः यह देखा जाता है कि वे 'सम्यग्ज्ञान' को प्रमाण का स्वरूप स्वीकारते हैं और उसे 'स्व-पर-प्रकाशक' मानते हैं ।
जैनेतर दार्शनिक क्षेत्र में कुछ दर्शन स्वप्रकाशवादी हैं और कुछ दर्शन परप्रकाशवादी हैं | विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञान से भिन्न अर्थ का अस्तित्व ही नहीं
१. सर्वार्थसिद्धि, १-१2
२. प्रमाणमीमांसा, पु. 2
३. स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं बुद्धिलक्षणम्, बृहत् स्वयम्भूस्तोत्र, ६३.
४. प्रमाणं स्वपरावमासिज्ञानं बाघविवर्जितम् न्यायावतार, इलोक १.
५. प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमनधिगतार्थ लक्षणत्वात्-मष्टशती - अष्टसहली, पू. १७४
६. सम्यन्ज्ञानं प्रमाणम् - स्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्, प्रमाणपरीक्षा, ५३
७. स्वापू वर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्- परीक्षामूस, १.१ ;
मनिश्चितोऽपूर्वार्थः, नही ।