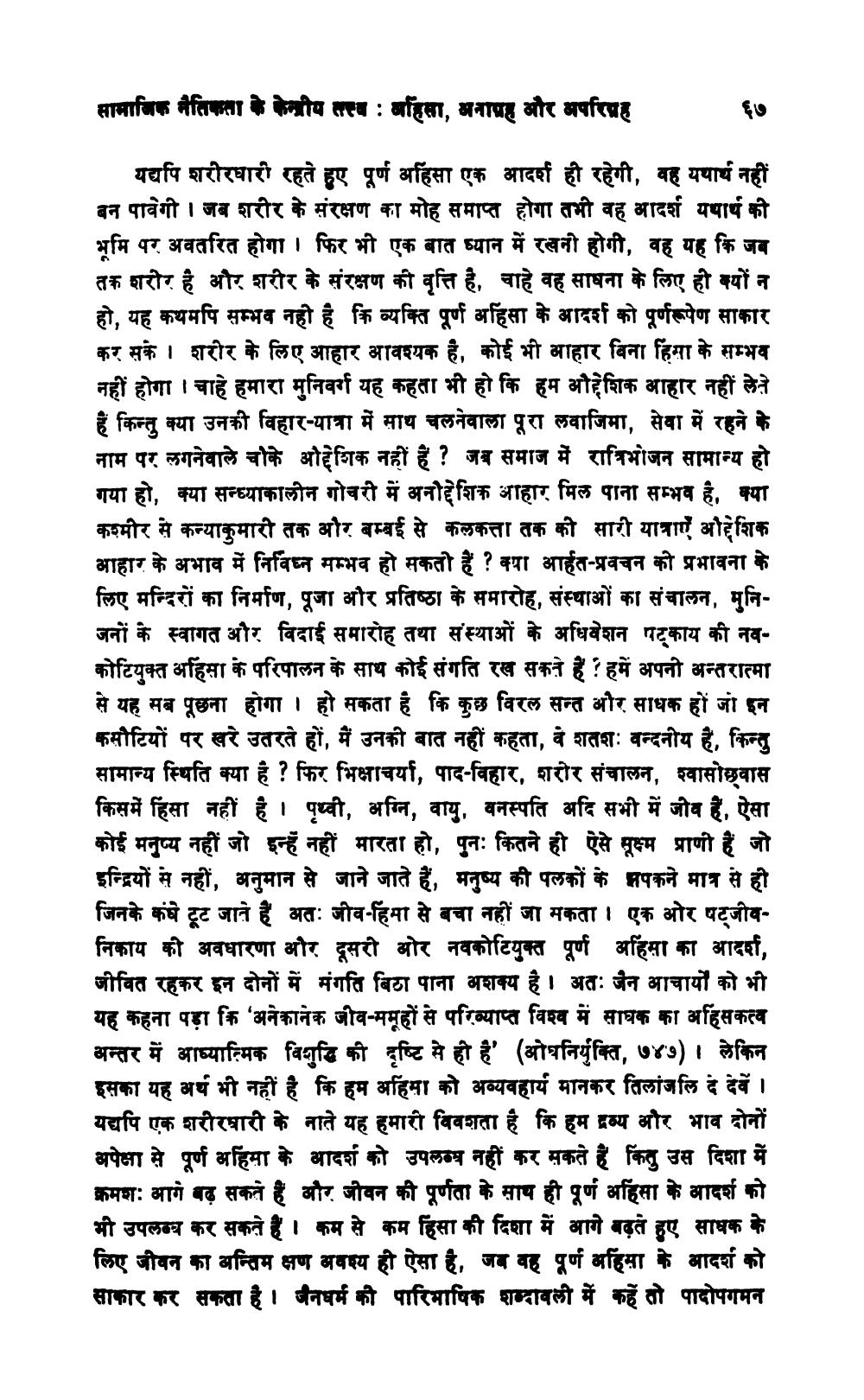________________
सामाजिक नैतिकता के केनीय तत्व : बहिसा, अनामह और अपरिवह
यद्यपि शरीरधारी रहते हुए पूर्ण अहिंसा एक आदर्श ही रहेगी, वह यथार्थ नहीं बन पावेगी । जब शरीर के संरक्षण का मोह समाप्त होगा तभी वह आदर्श यथार्थ की भूमि पर अवतरित होगा। फिर भी एक बात ध्यान में रखनी होगी, वह यह कि जब तक शरीर है और शरीर के संरक्षण की वृत्ति है, चाहे वह साधना के लिए ही क्यों न हो, यह कथमपि सम्भव नही है कि व्यक्ति पूर्ण अहिंसा के आदर्श को पूर्णरूपेण साकार कर सके । शरीर के लिए आहार आवश्यक है, कोई भी आहार बिना हिंमा के सम्भव नहीं होगा । चाहे हमारा मुनिवर्ग यह कहता भी हो कि हम औदेशिक आहार नहीं लेते हैं किन्तु क्या उनकी विहार-यात्रा में साथ चलनेवाला पूरा लवाजिमा, सेवा में रहने के नाम पर लगनेवाले चौके औद्देशिक नहीं हैं ? जब समाज में रात्रिभोजन सामान्य हो गया हो, क्या सन्ध्याकालीन गोचरी में अनौद्देशिक आहार मिल पाना सम्भव है, क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बम्बई से कलकत्ता तक की सारी यात्राएँ औदेशिक आहार के अभाव में निर्विघ्न सम्भव हो सकती हैं ? क्या आहेत-प्रवचन को प्रभावना के लिए मन्दिरों का निर्माण, पूजा और प्रतिष्ठा के समारोह, संस्थाओं का संचालन, मुनिजनों के स्वागत और विदाई समारोह तथा संस्थाओं के अधिवेशन पटकाय की नवकोटियुक्त अहिंसा के परिपालन के साथ कोई संगति रख सकते हैं ? हमें अपनी अन्तरात्मा से यह सब पूछना होगा । हो सकता है कि कुछ विरल सन्त और साधक हों जो इन कसौटियों पर खरे उतरते हों, मैं उनकी बात नहीं कहता, वे शतशः वन्दनीय है, किन्तु सामान्य स्थिति क्या है ? फिर भिक्षाचर्या, पाद-विहार, शरीर संचालन, श्वासोछ्वास किसमें हिंसा नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति अदि सभी में जीव है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो इन्हें नहीं मारता हो, पुनः कितने ही ऐसे सूक्ष्म प्राणी है जो इन्द्रियों में नहीं, अनुमान से जाने जाते हैं, मनुष्य की पलकों के सपकने मात्र से ही जिनके कंधे टूट जाते हैं अतः जीव-हिमा से बचा नहीं जा मकता। एक ओर षट्जीवनिकाय की अवधारणा और दूसरी ओर नवकोटियुक्त पूर्ण अहिंसा का आदर्श, जीवित रहकर इन दोनों में मंगति बिठा पाना अशक्य है। अतः जैन आचार्यों को भी यह कहना पड़ा कि 'अनेकानेक जीव-ममूहों से परिव्याप्त विश्व में साधक का अहिंसकत्व अन्तर में आध्यात्मिक विशुद्धि की दृष्टि से ही है' (ओपनियुक्ति, ७४७)। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम अहिंमा को अव्यवहार्य मानकर तिलांजलि दे देवें । यद्यपि एक शरीरधारी के नाते यह हमारी विवशता है कि हम द्रव्य और भाव दोनों अपेक्षा से पूर्ण अहिंसा के आदर्श को उपलब्ध नहीं कर सकते है किंतु उस दिशा में क्रमशः आगे बढ़ सकते है और जीवन की पूर्णता के साथ ही पूर्ण अहिंसा के आदर्श को भी उपलब्ध कर सकते हैं। कम से कम हिंसा की दिशा में आगे बढ़ते हुए साधक के लिए जीवन का अन्तिम क्षण अवश्य ही ऐसा है, जब वह पूर्ण अहिंसा के आदर्श को साकार कर सकता है। जैनधर्म की पारिभाषिक शब्दावली में कहें तो पादोपगमन