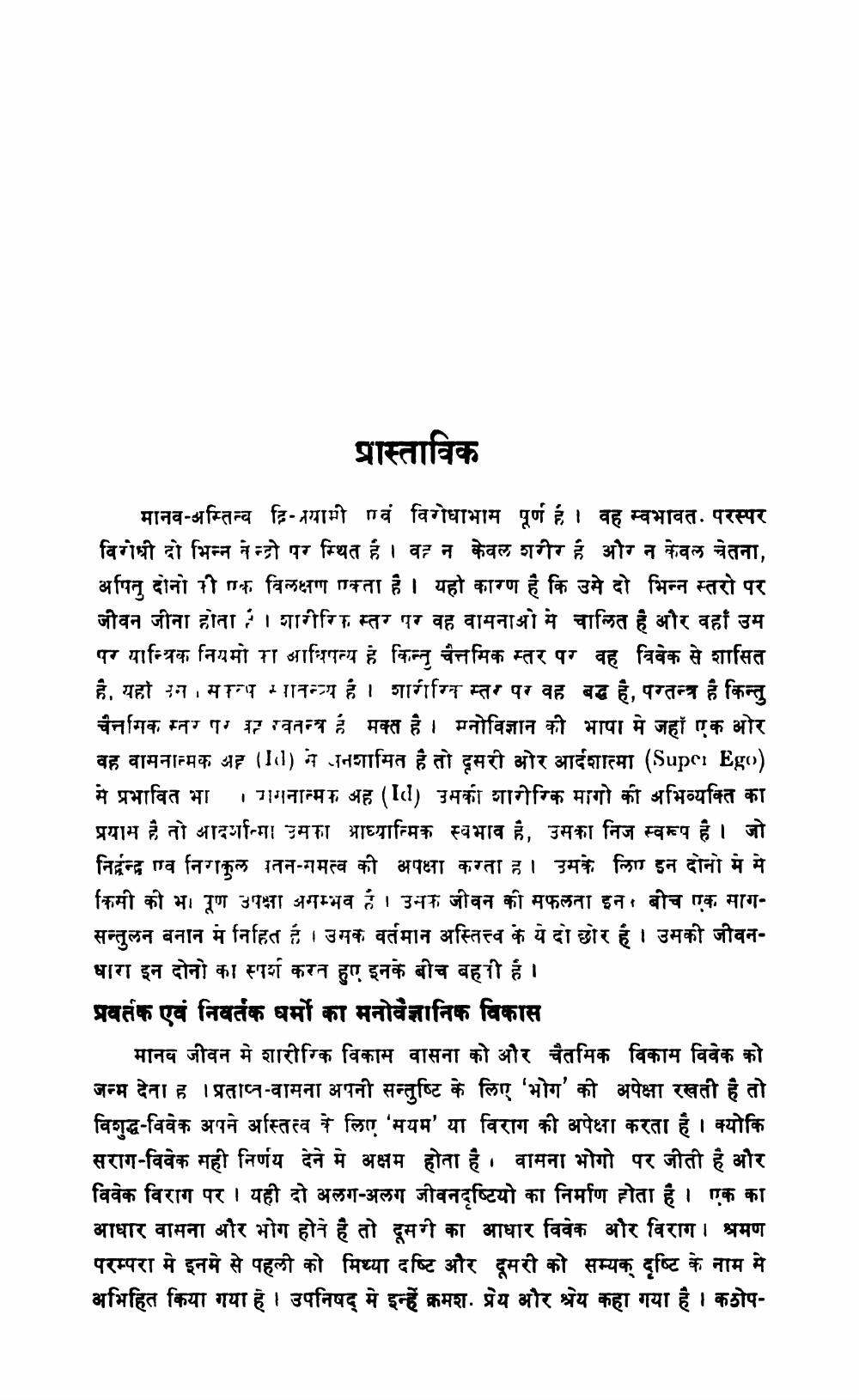________________
प्रास्ताविक
मानव अस्तित्व हि-यामी एवं विरोधाभास पूर्ण है । वह स्वभावत. परस्पर विरोधी दो भिन्न केन्द्रो पर स्थित है । वह न केवल शरीर है और न केवल चेतना, अपितु दोनो की एक विलक्षण एकता है । यहो कारण है कि उसे दो भिन्न स्तरो पर जीवन जीना होता है। शारीरिक स्तर पर वह वामनाओं में चालित है और वहाँ उम पर यान्त्रिक नियमों का आधिपत्य है किन्तु चैत्तमिक स्तर पर वह विवेक से शासित है, यहाँ उसासानन्य है । शारीरिक स्तर पर वह बद्ध है, परतन्त्र है किन्तु चैनमिक स्तर पर स्वतन्त्र है मक्त है। मनोविज्ञान की भाषा मे जहाँ एक ओर वह वासनात्मक अह (Id) ने जनशामित है तो दूसरी ओर आर्दशात्मा ( Super Ego ) में प्रभावित भा | गगनात्मक अह ( Id) उसकी शारीरिक मागो की अभिव्यक्ति का प्रयास है तो आदर्शामा उसका आध्यात्मिक स्वभाव है, निर्द्वन्द्व एव निराकुल तन-गमत्व की अपेक्षा करता है। उसके लिए इन दोनों में मे किसी को भण उपक्षा असम्भव है । उनक जीवन की सफलता इन बीच एक मागसन्तुलन बनान में निहित है। उसके वर्तमान अस्तित्त्व के ये दो छोर है । उसकी जीवनधारा इन दोनो का स्पर्श करत हुए इनके बीच बहती हैं ।
उसका निज स्वरूप है । जो
प्रवर्तक एवं निवर्तक धर्मो का मनोवैज्ञानिक विकास
मानव जीवन मे शारीरिक विकास वासना को और चैतमिक विकास विवेक को जन्म देना ह । प्राप्त वामना अपनी सन्तुष्टि के लिए 'भोग' की अपेक्षा रखती है तो विशुद्ध-विवेक अपने अस्तित्व के लिए 'मयम' या विराग की अपेक्षा करता है । क्योकि सराग - विवेक सही निर्णय देने में अक्षम होता है । वामना भोगो पर जीती है और विवेक विराग पर । यही दो अलग-अलग जीवनदृष्टियो का निर्माण होता है । एक का आधार वासना और भोग होने है तो दूसरी का आधार विवेक और विराग । श्रमण परम्परा मे इनमे से पहली को मिथ्या दष्टि और दूसरी को सम्यक् दृष्टि के नाम मे अभिहित किया गया है । उपनिषद् में इन्हें क्रमश. प्रेय और श्रेय कहा गया है । कठोप