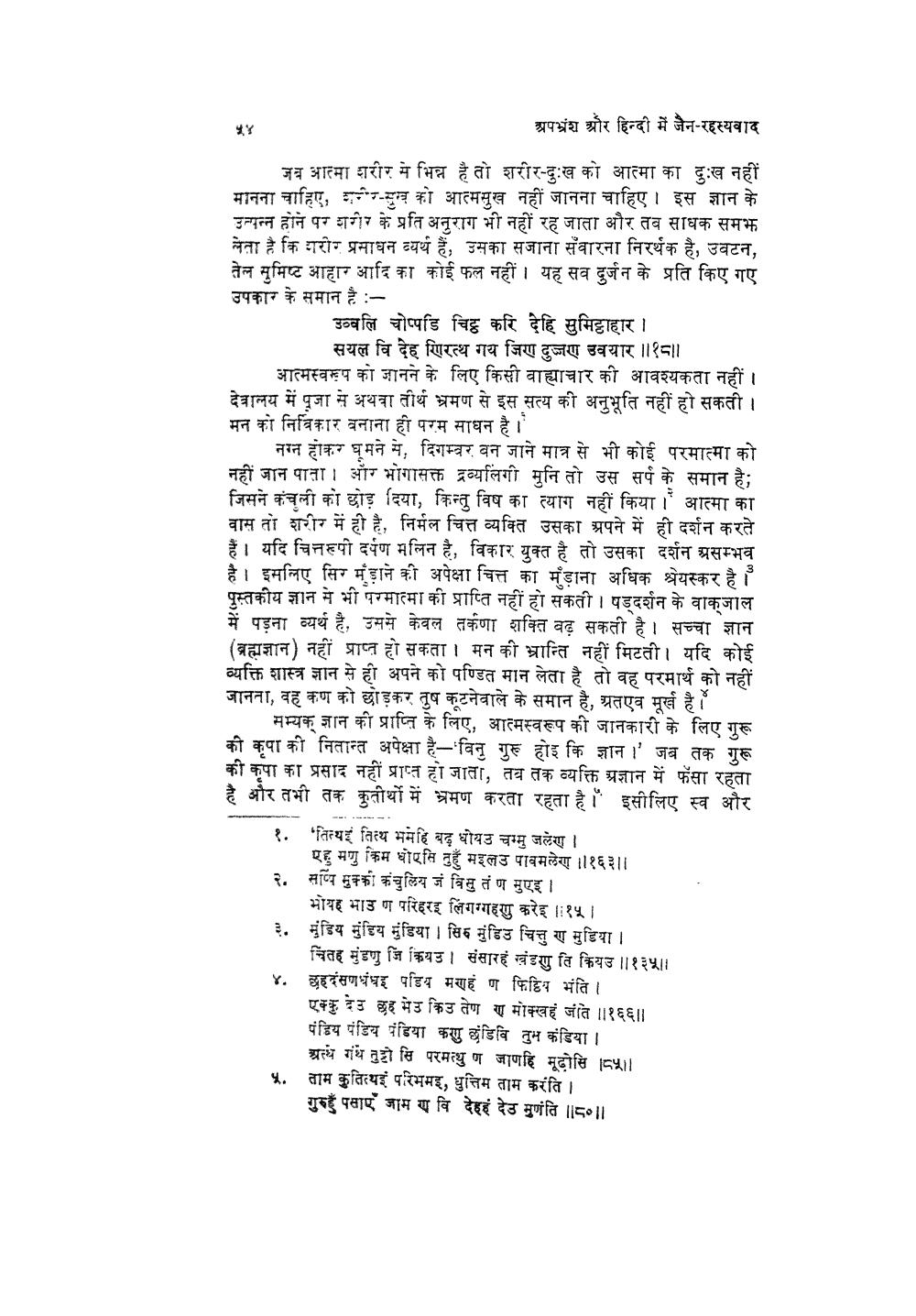________________
अपभ्रंश और हिन्दी में जैन - रहस्यवाद
जब आत्मा शरीर मे भिन्न है तो शरीर दुःख को आत्मा का दुःख नहीं मानना चाहिए, शरीरसुख को आत्मसुख नहीं जानना चाहिए। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर शरीर के प्रति अनुराग भी नहीं रह जाता और तब साधक समझ लेता है कि शरीर प्रसाधन व्यर्थ हैं, उसका सजाना सँवारना निरर्थक है, उबटन, तेल सुमिष्ट आहार आदि का कोई फल नहीं । यह सब दुर्जन के प्रति किए गए उपकार के समान है :
५४
उव्वल चोप्पड चिट्ठ करि देहि सुमिट्ठाहार ।
सयल वि देह रित्थ गय जिण दुज्जण उवयार || १८ ||
आत्मस्वरूप को जानने के लिए किसी बाह्याचार की आवश्यकता नहीं । देवालय में पूजा से अथवा तीर्थ भ्रमण से इस सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती । मन को निर्विकार बनाना ही परम साधन है ।
नग्न होकर घूमने से, दिगम्बर बन जाने मात्र से भी कोई परमात्मा को नहीं जान पाता। और भोगासक्त द्रव्यलिंगी मुनि तो उस सर्प के समान है; जिसने कंचुली को छोड़ दिया, किन्तु विष का त्याग नहीं किया । आत्मा का वास तो शरीर में ही है, निर्मल चित्त व्यक्ति उसका अपने में ही दर्शन करते हैं । यदि चित्तरूपी दर्पण मलिन है, विकार युक्त है तो उसका दर्शन असम्भव है। इसलिए सिर मुंडाने की अपेक्षा चित्त का मुँड़ाना अधिक श्रेयस्कर है । पुस्तकीय ज्ञान से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती । षड्दर्शन के वाक्जाल में पड़ना व्यर्थ है, उससे केवल तर्कणा शक्ति बढ़ सकती है। सच्चा ज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) नहीं प्राप्त हो सकता। मन की भ्रान्ति नहीं मिटती । यदि कोई व्यक्ति शास्त्र ज्ञान से ही अपने को पण्डित मान लेता है तो वह परमार्थ को नहीं जानता, वह कण को छोड़कर तुष कूटनेवाले के समान है, अतएव मूर्ख है ।
की
सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मस्वरूप की जानकारी के लिए गुरू कृपा की नितान्त अपेक्षा है- विनु गुरू होइ कि ज्ञान ।' जब तक गुरू की कृपा का प्रसाद नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक व्यक्ति अज्ञान में फँसा रहता है और तभी तक कुतीर्थो में भ्रमण करता रहता है। इसीलिए स्व और
१.
' तित्थई तित्थ भमेहि बढ़ धोयउ चम्मु जलेण । हुमणु किम घोसितुहुँ मइलउ पावमलेण || १६३।।
२. सपि मुक्की कंचुलिय जं विसु तं ण मुएइ ।
भोयह भाउ ण परिहरइ लिंगग्गहणु करेइ || १५ | ३. मुंडिय मुंडिय मुंडिया । सिप मुंडिउ चित्तु ण मुडिया | चितह मुंडण जि क्रियउ । संसारहं खंड ति क्रियउ || १३५ ।। ४. छहदंसणइ पडिय महं ण फिडिय भंति ।
५.
एक् देउ छह मे किउ तेण ण मोक्खहं जीते || १६६|| पंडिय पंडिय पंडिया करणु छंडिवि तुम कंडिया | श्रथ गंध तुट्टो सि परमत्थु ण जाणहि मूढोसि |५|| ताम कुतित्थई परिभमइ, धुत्तिम ताम करंति । गुरु पसाएँ जामय वि देहहं देउ मुणंति ||८०||