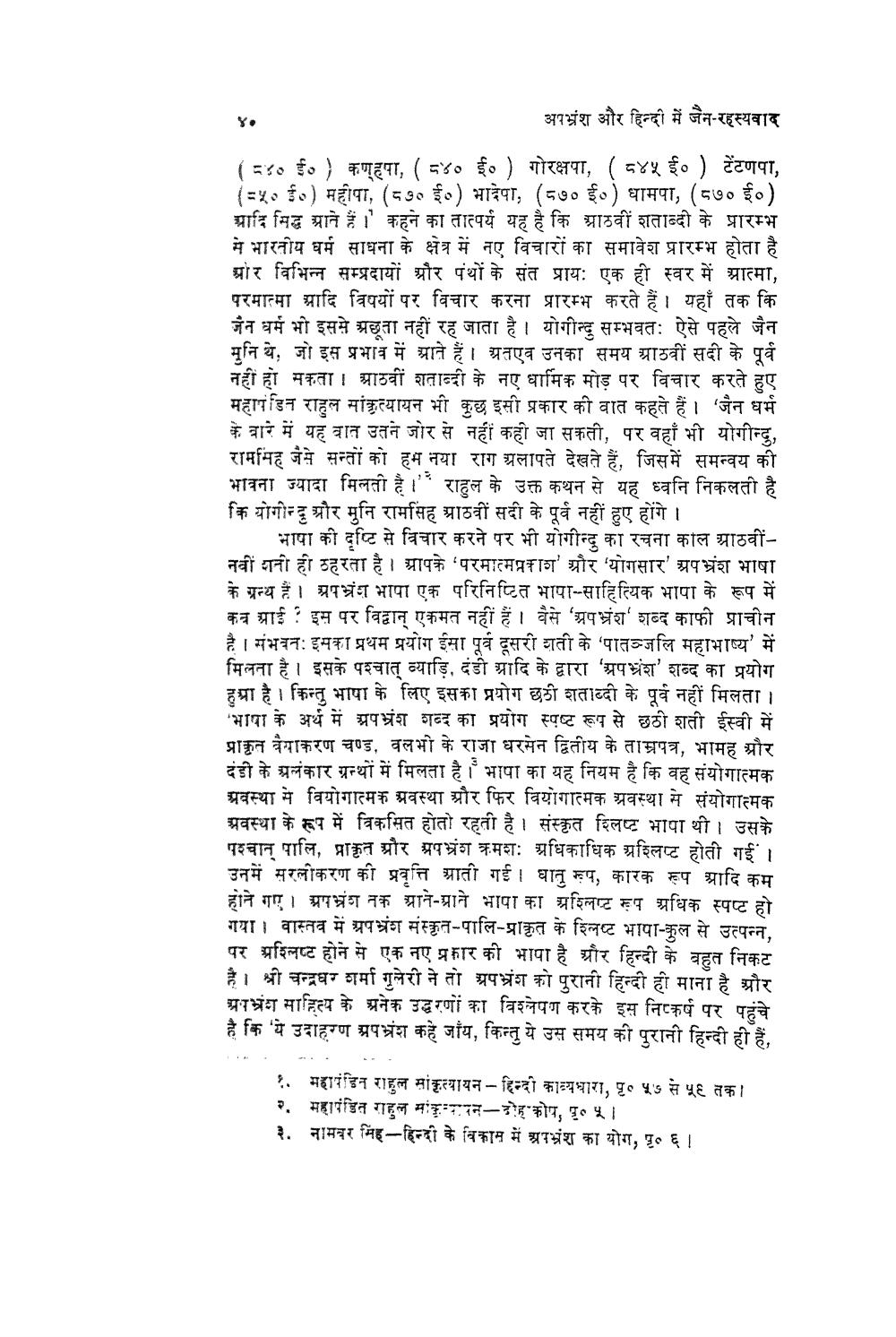________________
४.
अपभ्रंश और हिन्दी में जैन-रहस्यवाद
(८४० ई.) कण्हपा, (८४० ई०) गोरक्षपा, (८४५ ई० ) टेंटणपा, (५० ई०) महीपा, (८७० ई०) भादेपा, (८७० ई०) धामपा, (८७० ई०)
आदि मिद्ध आते हैं।' कहने का तात्पर्य यह है कि पाठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय धर्म साधना के क्षेत्र में नए विचारों का समावेश प्रारम्भ होता है और विभिन्न सम्प्रदायों और पंथों के संत प्राय: एक ही स्वर में आत्मा, परमात्मा आदि विषयों पर विचार करना प्रारम्भ करते हैं। यहाँ तक कि जैन धर्म भी इससे अछूता नहीं रह जाता है। योगीन्दु सम्भवत: ऐसे पहले जैन मुनि थे, जो इस प्रभाव में आते हैं। अतएव उनका समय पाठवीं सदी के पूर्व नहीं हो सकता। आठवीं शताब्दी के नए धार्मिक मोड़ पर विचार करते हुए महापंडिन राहुल सांकृत्यायन भी कुछ इसी प्रकार की वात कहते हैं। 'जैन धर्म के बारे में यह बात उतने जोर से नहीं कही जा सकती, पर वहाँ भी योगीन्दु, रामसिंह जैसे सन्तों को हम नया राग अलापते देखते हैं, जिसमें समन्वय की भावना ज्यादा मिलती है। राहुल के उक्त कथन से यह ध्वनि निकलती है कि योगीन्दु और मुनि रामसिंह पाठवीं सदी के पूर्व नहीं हुए होंगे।
भाषा की दृष्टि से विचार करने पर भी योगीन्दु का रचना काल आठवींनवीं शती ही ठहरता है। आपके ‘परमात्मप्रकाश' और 'योगसार' अपभ्रंश भाषा के ग्रन्थ हैं। अपभ्रंश भाषा एक परिनिप्टित भाषा-साहित्यिक भाषा के रूप में कब आई ? इस पर विद्वान् एकमत नहीं हैं। वैसे 'अपभ्रंश' शब्द काफी प्राचीन है। संभवतः इसका प्रथम प्रयोग ईसा पूर्व दूसरी शती के 'पातञ्जलि महाभाष्य' में मिलता है। इसके पश्चात व्याडि, दंडी आदि के द्वारा 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग हुया है। किन्तु भाषा के लिए इसका प्रयोग छठी शताब्दी के पूर्व नहीं मिलता। 'भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से छठी शती ईस्वी में प्राकृत वैयाकरण चण्ड, वलभी के राजा धरसेन द्वितीय के ताम्रपत्र, भामह और दंडी के अलंकार ग्रन्थों में मिलता है। भाषा का यह नियम है कि वह संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था और फिर वियोगात्मक अवस्था से संयोगात्मक अवस्था के रूप में विकसित होतो रहती है। संस्कृत श्लिष्ट भाषा थी। उसके पश्चात पालि, प्राकृत और अपभ्रंश क्रमशः अधिकाधिक अश्लिप्ट होती गई। उनमें सरलीकरण की प्रवृत्ति पाती गई। धातु रूप, कारक रूप आदि कम होने गए। अपभ्रंश तक आते-पाते भाषा का अश्लिष्ट रूप अधिक स्पष्ट हो गया। वास्तव में अपभ्रंश संस्कृत-पालि-प्राकृत के श्लिष्ट भाषा-कुल से उत्पन्न, पर अश्लिष्ट है
होने से एक नए प्रकार की भापा है और हिन्दी के बहत निकट है। श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने तो अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी ही माना है और अपभ्रंग साहित्य के अनेक उद्धरणों का विश्लेपण करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि 'ये उदाहरण अपभ्रंश कहे जाय, किन्तु ये उस समय की पुरानी हिन्दी ही हैं,
१. महापंडिन राहुल सांकृत्यायन - हिन्दी काव्यधारा, पृ० ५७ से ५६ तक। २. महापंडित गहुल मकवान-दोहकोप, पृ०५। ३. नामवर सिंह-हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ०६।