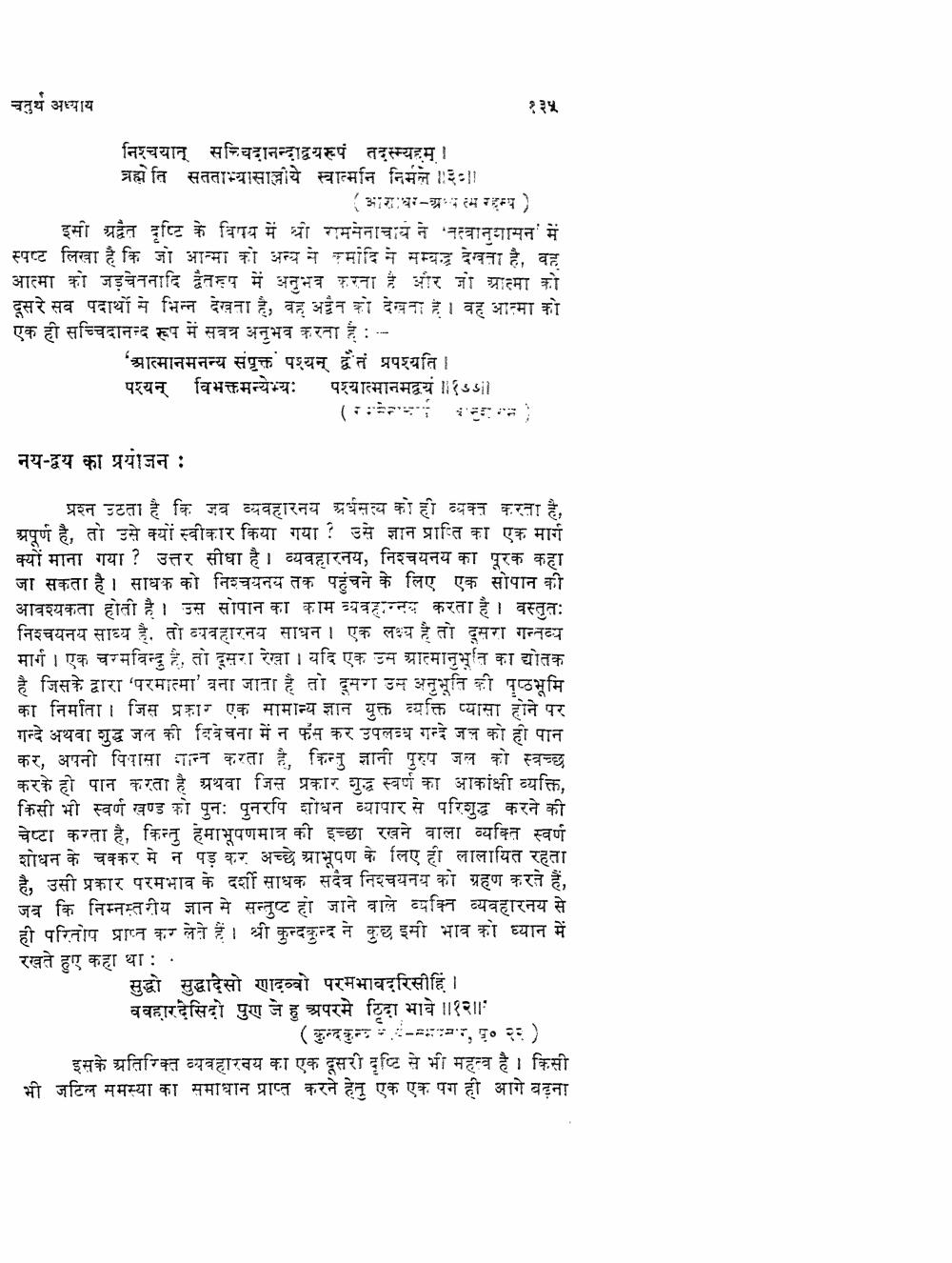________________
चतुर्थ अध्याय
निश्चयान् सच्चिदानन्दाद्वयरूपं तदस्म्यहम् । ब्रह्मेति सतताभ्यासालीये स्वात्मनि निर्मन्न । ३०॥
(अराधर-अात्म रहन्य) इसी अद्वैत दृष्टि के विषय में श्री रामनाचार्य ने नवानगासन में स्पष्ट लिखा है कि जो आत्मा को अन्य ने कांदि ने सम्बद्ध देखता है, वह आत्मा को जड़चेतनादि द्वैतरूप में अनुभव करता है और जो प्रात्मा को दुसरे सब पदार्थों से भिन्न देखता है, वह अद्वैन को देखना है। वह आत्मा को एक ही सच्चिदानन्द रूप में सवत्र अनुभव करता है : ---
'आत्मानमनन्य संपृक्त पश्यन् द्वैतं प्रपश्यति । पश्यन् विभक्तमन्येभ्यः पश्यात्मानमद्वयं ॥१७॥
नय-द्वय का प्रयोजन :
प्रश्न उठता है कि जब व्यवहारनय अर्धसत्य को ही व्यक्त करता है, अपूर्ण है, तो उसे क्यों स्वीकार किया गया? उसे ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग क्यों माना गया? उत्तर सीधा है। व्यवहारनय, निश्चयनय का पुरक कहा जा सकता है। साधक को निश्चयनय तक पहुंचने के लिए एक सोपान की आवश्यकता होती है। उस सोपान का काम व्यवहान्न करता है। वस्तुतः निश्चयनय साध्य है. तो व्यवहारनय साधन । एक लक्ष्य है तो दूसरा गन्तव्य मार्ग । एक चरमविन्दु है, तो दुसरा रेखा । यदि एक उस आत्मानुभूति का द्योतक
है जिसके द्वारा ‘परमात्मा' बना जाता है तो दूसग उन अनुभूति की पृष्ठभूमि __ का निर्माता। जिस प्रकार एक मामान्य ज्ञान युक्त व्यक्ति प्यासा होने पर
गन्दे अथवा शुद्ध जल की विवेचना में न फंस कर उपलब्ध गन्दे जल को ही पान कर, अपनी पिपासा गान्न करता है, किन्तु ज्ञानी पुरुप जल को स्वच्छ करके हो पान करता है अथवा जिस प्रकार गुद्ध स्वर्ण का आकांक्षी व्यक्ति, किसी भी स्वर्ण खण्ड को पुनः पुनरपि शोधन व्यापार से परिशुद्ध करने की चेप्टा करता है, किन्तु हेमाभूपणमात्र की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वर्ण शोधन के चक्कर मे न पड़ कर अच्छे आभूषण के लिए ही लालायित रहता
है, उसी प्रकार परमभाव के दर्शी साधक सदैव निश्चयनय को ग्रहण करते हैं, __ जब कि निम्नस्तरीय ज्ञान से सन्तुष्ट हो जाने वाले व्यक्ति व्यवहारनय से
ही परितोप प्राप्त कर लेते हैं। श्री कुन्दकुन्द ने कुछ इमी भाव को ध्यान में रखते हुए कहा था : .
सुद्धो सुद्धादेसो णादव्वो परमभावदरिसीहि । ववहारदेसिदो पुण जे हु अपरमे टिदा भावे ॥१२॥
इसके अतिरिक्त व्यवहारचय का एक दूसरी दृष्टि से भी महत्व है। किसी भी जटिल समस्या का समाधान प्राप्त करने हेतु एक एक पग ही आगे बढ़ना