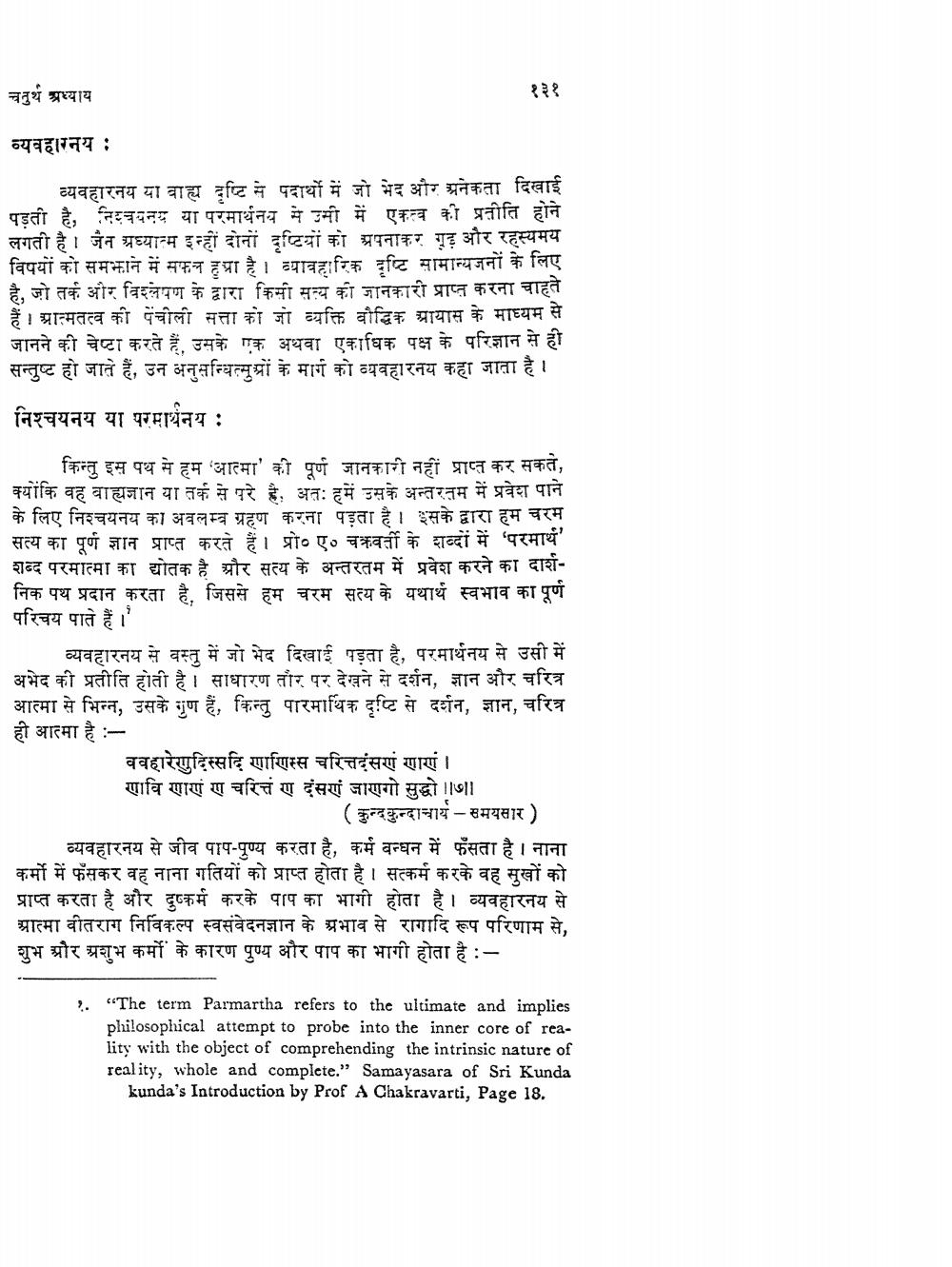________________
चतुर्थ अध्याय
व्यवहारनय :
व्यवहारनय या बाह्य दृष्टि से पदार्थों में जो भेद और अनेकता दिखाई पड़ती है, नियनय या परमार्थनय मे उसी में एकत्व की प्रतीति होने लगती है। जैन अध्यात्म इन्हीं दोनों दृष्टियों को अपनाकर गुड़ और रहस्यमय विषयों को समझाने में सफल हुआ है। व्यावहारिक दृष्टि सामान्यजनों के लिए है, जो तर्क और विश्लेषण के द्वारा किसी सत्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मतत्व की वीसी सत्ता को जो व्यक्ति बौद्धिक प्रयास के माध्यम से जानने की चेष्टा करते हैं, उसके एक अथवा एकाधिक पक्ष के परिज्ञान से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, उन अनुसन्धमुओं के मार्ग की व्यवहारनय कहा जाता है। निश्चयनय या परमार्थनय
१३१
:
किन्तु इस पथ मे हम 'आत्मा' की पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वह वाह्यज्ञान या तर्क से परे है, अतः हमें उसके अन्तरतम में प्रवेश पाने के लिए निश्चयनय का अवलम्ब ग्रहण करना पड़ता है। इसके द्वारा हम चरम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रो० ए० चक्रवर्ती के शब्दों में 'परमार्थ' शब्द परमात्मा का द्योतक है और सत्य के अन्तरतम में प्रवेश करने का दार्श निक पथ प्रदान करता है, जिससे हम चरम सत्य के यथार्थ स्वभाव का पूर्ण परिचय पाते हैं।'
व्यवहारनय से वस्तु में जो भेद दिखाई पड़ता है, परमार्थनय से उसी में अभेद की प्रतीति होती है । साधारण तौर पर देखने से दर्शन, ज्ञान और चरित्र आत्मा से भिन्न, उसके गुण हैं, किन्तु पारमार्थिक दृष्टि से दर्शन, ज्ञान, चरित्र ही आत्मा है
:
बवहारेणुदिस्सदि गाणिस्स परित्तदंसणं गाणं । णावि गाणं ण चरितं ण दंसणं जागो सुद्धो ॥१७॥ ( कुन्दकुन्दाचार्य – समयसार )
व्यवहारनय से जीव पाप-पुण्य करता है, कर्म बन्धन में फँसता है । नाना कर्मों में फँसकर वह नाना गतियों को प्राप्त होता है। सत्कर्म करके वह सुखों को प्राप्त करता है और दुष्कर्म करके पाप का भागी होता है । व्यवहारनय से आत्मा वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदनज्ञान के प्रभाव से रागादि रूप परिणाम से, शुभ और अशुभ कर्मों के कारण पुण्य और पाप का भागी होता है :
-
१. “The term Parmartha refers to the ultimate and implies philosophical attempt to probe into the inner core of reality with the object of comprehending the intrinsic nature of reality, whole and complete." Samayasara of Sri Kunda kunda's Introduction by Prof A Chakravarti, Page 18.