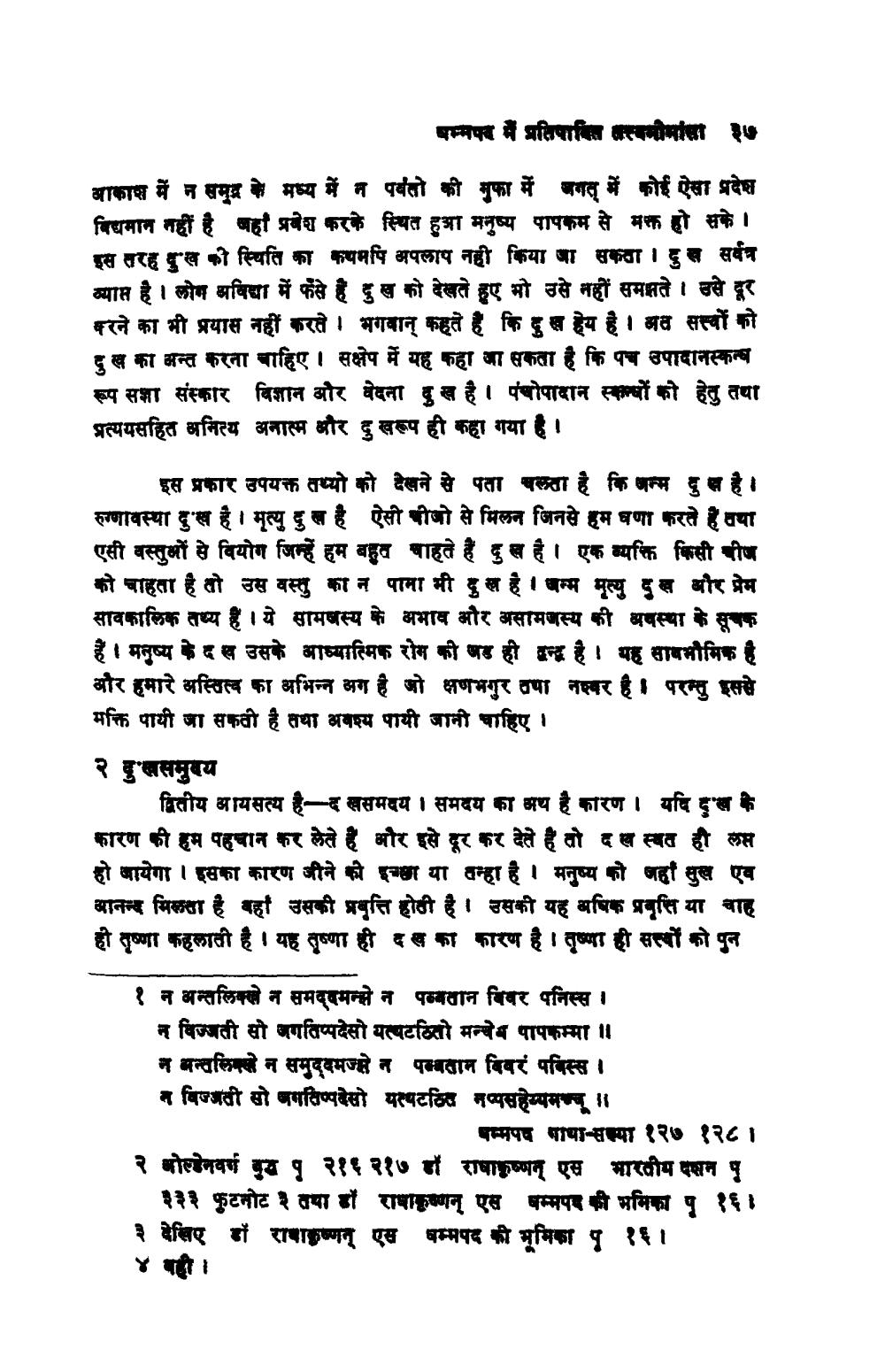________________
पम्मपद में प्रतिपादित अपनीमांसा ३७ आकाश में न समुद्र के मध्य में न पर्वतो की मुफा में बनत में कोई ऐसा प्रदेश विद्यमान नहीं है वहाँ प्रवेश करके स्थित हुआ मनुष्य पापकम से मक हो सके । इस तरह दुख की स्थिति का कथमपि अपलाप नही किया जा सकता । दुख सर्वत्र व्याप्त है । लोग अविद्या में फंसे है दुख को देखते हुए भी उसे नहीं समझते । उसे दूर करने का भी प्रयास नहीं करते । भगवान् कहते है कि दुख हेय है । अत सस्वों को दुख का अन्त करना चाहिए । सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पच उपादानस्कन्ध रूप सज्ञा संस्कार विज्ञान और वेदना दुख है। पंचोपादान सल्बों को हेतु तथा प्रत्ययसहित अनित्य अनात्म और दुखरूप ही कहा गया है।
इस प्रकार उपयक्त तथ्यो को देखने से पता चलता है कि जन्म दुख है। रुग्णावस्था दुःख है । मृत्यु दुख है ऐसी चीजो से मिलन जिनसे हम घणा करते है तथा एसी वस्तुओं से वियोग जिन्हें हम बहुत चाहते हैं दुख है । एक व्यक्ति किसी चीण को चाहता है तो उस वस्तु का न पामा भी दुख है । बन्म मृत्यु दुख और प्रेम सावकालिक तथ्य है। ये सामषस्य के अभाव और असामजस्य की अवस्था के सूचक है। मनुष्य के दस उसके आध्यात्मिक रोम की बड ही इन्द्र है। यह सावभौमिक है
और हमारे अस्तित्व का अभिन्न अग है जो क्षणभगुर तपा नश्वर है। परन्तु इससे मक्ति पायी जा सकती है तथा अवश्य पायी जानी चाहिए ।
द्वितीय आयसत्य है-दखसमवय । समदय का अर्थ है कारण । यदि दुख कारण की हम पहचान कर लेते है और इसे दूर कर देते हैं तो दख स्वत ही लस हो पायेगा । इसका कारण जीने को इच्छा या तन्हा है । मनुष्य को जहां सुख एव मानन्द मिलता है वहां उसकी प्रवृत्ति होती है। उसकी यह अधिक प्रवृत्ति या चाह हो तृष्णा कहलाती है । यह तृष्णा ही द ख का कारण है । तृष्णा ही सस्तों को पुन
१ न अन्तलिकले न समदनमन्झे न पब्बतान विवर पनिस्स । न विज्जती सो जगतिप्पदेसो यत्पटठितो मन्चेष पापकम्मा ।। न मन्तालिमले न समुदवमलेन पन्नताम विवरं पविस्स । नविज्जती सो जगतिपदेसो यत्पटटिस मप्पसहेम्पमच्चू ।।
पम्मपद पापा-सच्या १२७ १२८ । २ गोल्डेनवर्ग बुट १ २१६ २१७ में राधाकृष्णन् एस भारतीय पान १
३३३ फुटनोट ३ तथा डॉ राधाकृष्णन् एस पम्मपरकी भमिका पृ १६ ॥ ३ देखिए में राधाकृष्णन् एस धम्मपद की भूमिका १ १६ ।