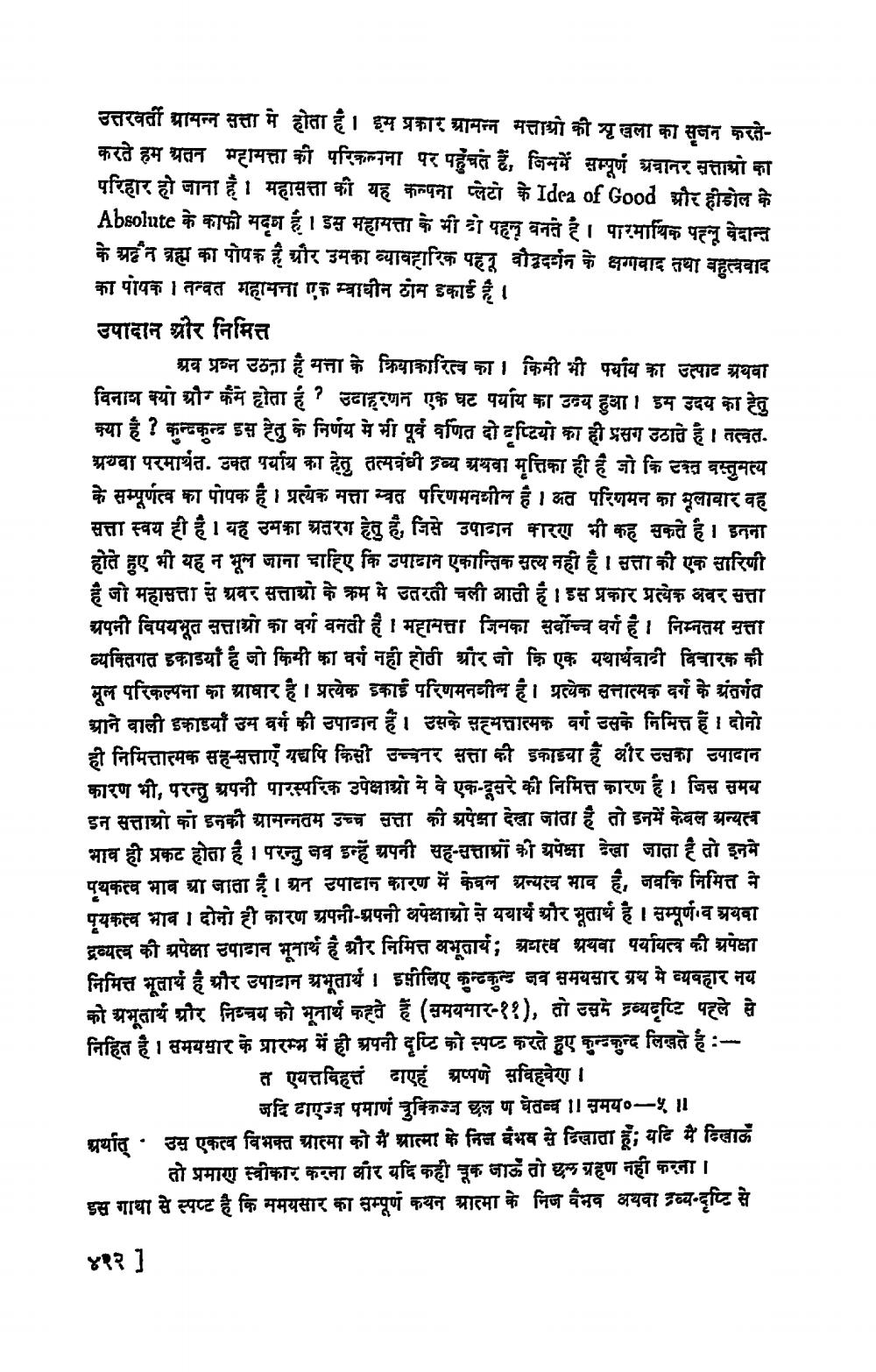________________
उत्तरवर्ती आसन्न सत्ता में होता है। इस प्रकार प्रामन्न मत्तानो की मृखला का सनन करतेकरते हम अतन महामत्ता की परिकल्पना पर पहुंचते हैं, जिनमें सम्पूर्ण अवानर सत्तात्री का परिहार हो जाता है। महासत्ता की यह कल्पना प्लेटो के Idea of Good और हीडोल के Absolute के काफी मदन है । इस महासत्ता के भी दो पहल बनते हैं। पारमार्थिक पहलू वेदान्त के अट्ठन ब्रह्म का पोषक है और उसका व्यावहारिक पहलू बौदर्शन के भगवाद तथा बहुत्ववाद का पोषक । नन्वत महामना एकम्बाचीन ठोस इकाई है। उपादान और निमित्त
अब प्रश्न उठता है मत्ता के क्रियाकारित्व का। किमी भी पर्याय का उत्पाद अथवा विनाश क्या और कैसे होता है ? उदाहरणन एक घट पर्याय का उदय हुआ। इस उदय का हेतु क्या है ? कुन्दकुन्द इस हेतु के निर्णय में भी पूर्व वणित दो दृष्टियो का ही प्रसग उठाते है । तत्वत. अग्वा परमार्थत. उक्त पर्याय का हेतु तत्सबंधी द्रव्य अथवा मृत्तिका ही है जो कि रक्त वस्तुमत्य के सम्पूर्णत्व का पोपक है । प्रत्यक मत्ता स्वत परिणमनशील है । अत परिणमन का मूलावार वह सत्ता स्वय ही है । यह उमका अतरग हेतु है, जिसे उपादान कारण भी कह सकते है। इतना होते हुए भी यह न भूल जाना चाहिए कि उपादान एकान्तिक सत्य नहीं है । सत्ता की एक सारिणी है जो महासत्ता से अवर सत्ताओं के क्रम में उतरती चली आती है । इस प्रकार प्रत्येक अवर सत्ता अपनी विषयभूत सत्ताओं का वर्ग वनती है । महासत्ता जिनका सर्वोच्च वर्ग है। निम्नतम सत्ता व्यक्तिगत इकाइयां है जो किसी का वर्ग नहीं होती और नो कि एक यथार्थवादी विचारक की मूल परिकल्पना का आधार है । प्रत्येक इकाई परिणमनगील है। प्रत्येक सत्तात्मक वर्ग के अंतर्गत आने वाली इकाइयाँ उस वर्ग की उपादान हैं। उसके समत्तात्मक वर्ग उसके निमित्त हैं । दोनो ही निमित्तात्मक सह-सत्ताएं यद्यपि किसी उच्चनर सत्ता की इकाइया है और उसका उपादान कारण भी, परन्तु अपनी पारस्परिक उपेक्षाओं में वे एक-दूसरे की निमित्त कारण है। जिस समय इन सत्ताओं को इनकी आमन्नतम उच्च सत्ता की अपेक्षा देखा जाता है तो इनमें केवल अन्यत्व भाव ही प्रकट होता है । परन्तु जब इन्हें अपनी सह-सत्तानों की अपेक्षा देखा जाता है तो इनमे पृथकत्व भाव आ जाता है । अन उपादान कारण में केवल अन्यत्व भाव है, जबकि निमित्त ने पृयकत्व भाव । दोनो ही कारण अपनी-अपनी अपेक्षाओं में ययार्थ और भूतार्थ है । सम्पूर्णव अथवा द्रव्यत्व की अपेक्षा उपादान भूतार्थ है और निमित्त अभूतार्य; अगत्व अथवा पर्यायत्त की अपेक्षा निमित्त भूतार्थ है और उपादान अभूतार्थ । इसीलिए कुन्दकुन्द जब समयसार अय मे व्यवहार नय को अभूतार्थ और निश्चय को भूतार्थ कहते हैं (समयमार-११), तो उसमे द्रव्यदृष्टि पहले से निहित है । समयमार के प्रारम्भ में ही अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कुन्दकुन्द लिखते है :
त एयत्तविहत्तं दाएहं अप्पणे सविहवेण ।
जदि दाएन्ज पमाणं त्रुक्किल छल ण घेतब्य ।। समय०-५॥ अर्थात् • उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं प्रात्मा के निन वैभव से दिखाता हूँ; यदि मैं दिखाऊँ
तो प्रमाण स्वीकार करना और यदि कही चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना । इस गाथा से स्पष्ट है कि ममयसार का सम्पूर्ण कथन आत्मा के निज वैभव अथवा द्रव्य दृष्टि से
४१२]