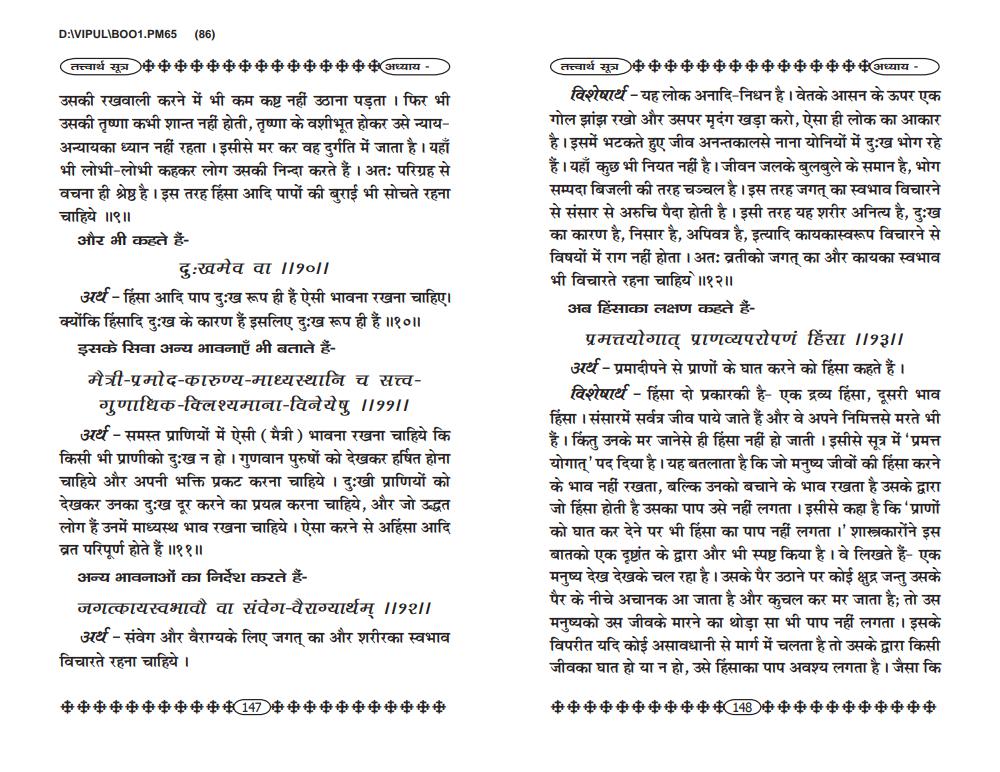________________
DRIVIPULIBOO1.PM65
(86)
(तत्वार्थ सूत्र
अध्याय .D
उसकी रखवाली करने में भी कम कष्ट नहीं उठाना पड़ता । फिर भी उसकी तृष्णा कभी शान्त नहीं होती, तृष्णा के वशीभूत होकर उसे न्यायअन्यायका ध्यान नहीं रहता । इसीसे मर कर वह दुर्गति में जाता है। यहाँ भी लोभी-लोभी कहकर लोग उसकी निन्दा करते हैं । अतः परिग्रह से वचना ही श्रेष्ठ है । इस तरह हिंसा आदि पापों की बुराई भी सोचते रहना चाहिये ॥९॥ और भी कहते हैं
दु:खमेव वा ||१०|| अर्थ- हिंसा आदि पाप दुःख रूप ही हैं ऐसी भावना रखना चाहिए। क्योंकि हिंसादि दुःख के कारण हैं इसलिए दुःख रूप ही हैं ॥१०॥ इसके सिवा अन्य भावनाएँ भी बताते हैंमैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थानि च सत्त्व
गुणाधिक-क्लिश्यमाना-विनेयेषु ।।११।। अर्थ - समस्त प्राणियों में ऐसी (मैत्री) भावना रखना चाहिये कि किसी भी प्राणीको दुःख न हो । गुणवान पुरुषों को देखकर हर्षित होना चाहिये और अपनी भक्ति प्रकट करना चाहिये । दुःखी प्राणियों को देखकर उनका दुःख दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये, और जो उद्धत लोग हैं उनमें माध्यस्थ भाव रखना चाहिये । ऐसा करने से अहिंसा आदि व्रत परिपूर्ण होते हैं ॥११॥
अन्य भावनाओं का निर्देश करते हैंजगत्कायस्वभावौ वा संवेग-वैराग्यार्थम् ||१||
अर्थ-संवेग और वैराग्यके लिए जगत् का और शरीरका स्वभाव विचारते रहना चाहिये।
(तत्त्वार्थ सूत्र *************** अध्याय -
विशेषार्थ-यह लोक अनादि-निधन है । वेतके आसन के ऊपर एक गोल झांझ रखो और उसपर मृदंग खड़ा करो, ऐसा ही लोक का आकार है। इसमें भटकते हुए जीव अनन्तकालसे नाना योनियों में दुःख भोग रहे हैं। यहाँ कुछ भी नियत नहीं है। जीवन जलके बुलबुले के समान है, भोग सम्पदा बिजली की तरह चञ्चल है। इस तरह जगत् का स्वभाव विचारने से संसार से अरुचि पैदा होती है। इसी तरह यह शरीर अनित्य है, दुःख का कारण है, निसार है, अपिवत्र है, इत्यादि कायकास्वरूप विचारने से विषयों में राग नहीं होता । अतः व्रतीको जगत् का और कायका स्वभाव भी विचारते रहना चाहिय ॥१२॥ अब हिंसाका लक्षण कहते हैं
प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ||१३|| अर्थ-प्रमादीपने से प्राणों के घात करने को हिंसा कहते हैं। विशेषार्थ - हिंसा दो प्रकारकी है- एक द्रव्य हिंसा, दूसरी भाव हिंसा । संसारमें सर्वत्र जीव पाये जाते हैं और वे अपने निमित्तसे मरते भी हैं। किंतु उनके मर जानेसे ही हिंसा नहीं हो जाती । इसीसे सूत्र में 'प्रमत्त योगात्' पद दिया है। यह बतलाता है कि जो मनुष्य जीवों की हिंसा करने के भाव नहीं रखता, बल्कि उनको बचाने के भाव रखता है उसके द्वारा जो हिंसा होती है उसका पाप उसे नहीं लगता । इसीसे कहा है कि 'प्राणों को घात कर देने पर भी हिंसा का पाप नहीं लगता।' शास्त्रकारोंने इस बातको एक दृष्टांत के द्वारा और भी स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं- एक मनष्य देख देखके चल रहा है। उसके पैर उठाने पर कोई क्षद्र जन्तु उसके पैर के नीचे अचानक आ जाता है और कुचल कर मर जाता है तो उस मनुष्यको उस जीवके मारने का थोड़ा सा भी पाप नहीं लगता । इसके विपरीत यदि कोई असावधानी से मार्ग में चलता है तो उसके द्वारा किसी जीवका घात हो या न हो, उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है। जैसा कि
*
*****
**41470
*
22****
坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐实148座本本坐坐坐坐坐坐坐坐