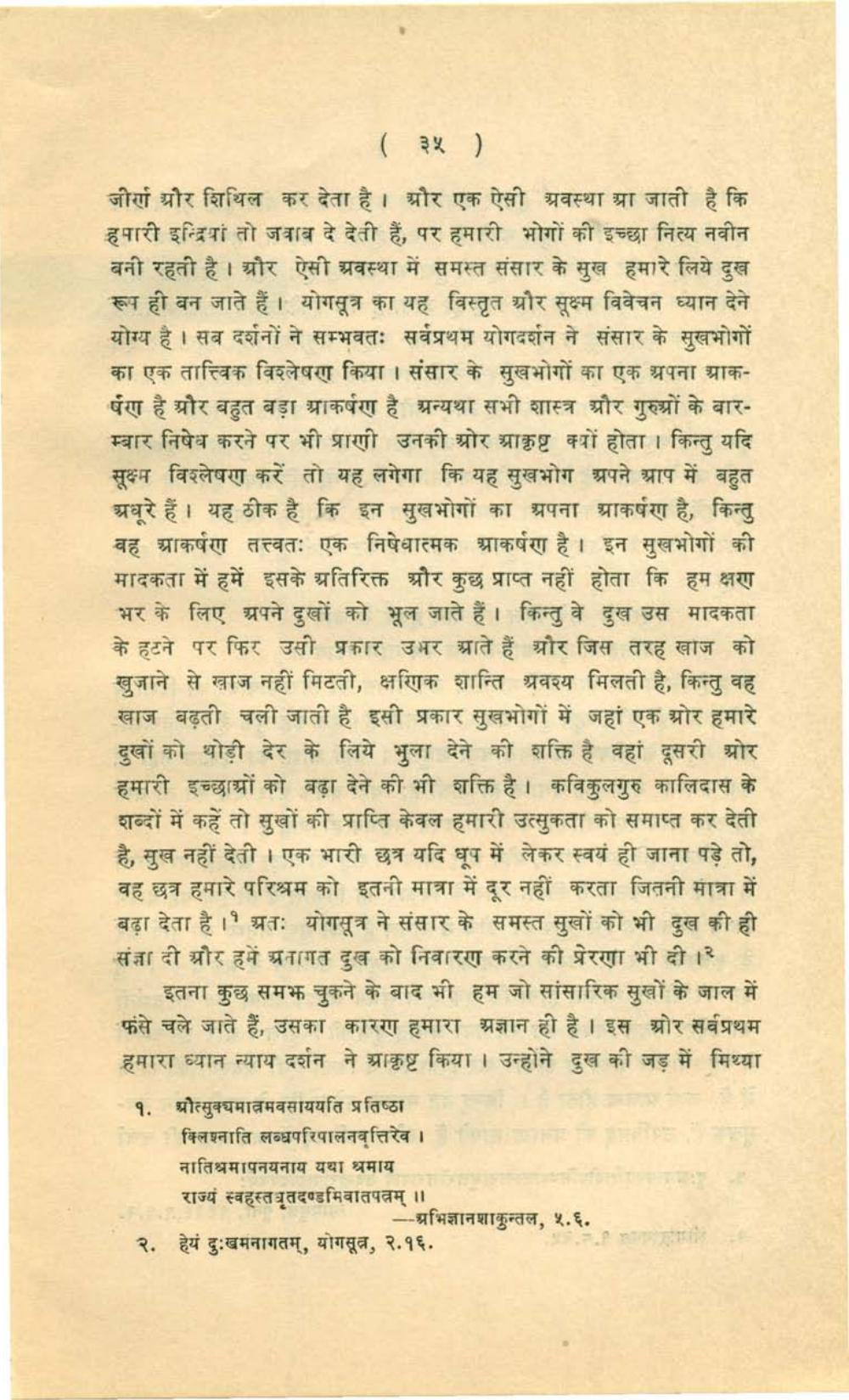________________
( ३५ )
जीर्ण और शिथिल कर देता है । और एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारी इन्द्रियां तो जवाब दे देती हैं, पर हमारी भोगों की इच्छा नित्य नवीन बनी रहती है । और ऐसी अवस्था में समस्त संसार के सुख हमारे लिये दुख रूप ही बन जाते हैं। योगसूत्र का यह विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन ध्यान देने योग्य है । सब दर्शनों ने सम्भवतः सर्वप्रथम योगदर्शन ने संसार के सुखभोगों का एक तात्त्विक विश्लेषण किया। संसार के सुखभोगों का एक अपना आक
आकर्षण है, किन्तु
इन सुखभोगों की
है और बहुत बड़ा आकर्षण है अन्यथा सभी शास्त्र और गुरुत्रों के बारम्बार निषेध करने पर भी प्राणी उनकी ओर आकृष्ट क्यों होता । किन्तु यदि सूक्ष्म विश्लेषण करें तो यह लगेगा कि यह सुखभोग अपने आप में बहुत अधूरे हैं। यह ठीक है कि इन सुखभोगों का अपना वह आकर्षण तत्त्वतः एक निषेधात्मक आकर्षण है । मादकता में हमें इसके अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता कि हम क्षण भर के लिए अपने दुखों को भूल जाते हैं । किन्तु वे दुख उस मादकता के हटने पर फिर उसी प्रकार उभर आते हैं और जिस तरह खाज को खुजाने से खाज नहीं मिटती, क्षणिक शान्ति श्रवश्य मिलती है, किन्तु वह खाज बढ़ती चली जाती है इसी प्रकार सुखभोगों में जहां एक ओर हमारे दुखों को थोड़ी देर के लिये भुला देने की शक्ति है वहां दूसरी ओर हमारी इच्छाओं को बढ़ा देने की भी शक्ति है । कविकुलगुरु कालिदास के शब्दों में कहें तो सुखों की प्राप्ति केवल हमारी उत्सुकता को समाप्त कर देती है, सुख नहीं देती । एक भारी छत्र यदि धूप में लेकर स्वयं ही जाना पड़े तो, वह छत्र हमारे परिश्रम को इतनी मात्रा में दूर नहीं करता जितनी मात्रा में बढ़ा देता है ।' अत: योगसूत्र ने संसार के समस्त सुखों को भी दुख की ही संज्ञा दी और हमें अनागत दुख को निवारण करने की प्रेरणा भी दी ।
इतना कुछ समझ चुकने के बाद भी हम जो सांसारिक सुखों के जाल में फंसे चले जाते हैं, उसका कारण हमारा अज्ञान ही है । इस ओर सर्वप्रथम हमारा ध्यान न्याय दर्शन ने आकृष्ट किया। उन्होंने दुख की जड़ में मिथ्या
१. श्रौत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा
क्लिश्नाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव । नातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम् ॥
- अभिज्ञानशाकुन्तल, ५.६.
२. हेयं दुःखमनागतम्, योगसूत्र, २.१६.