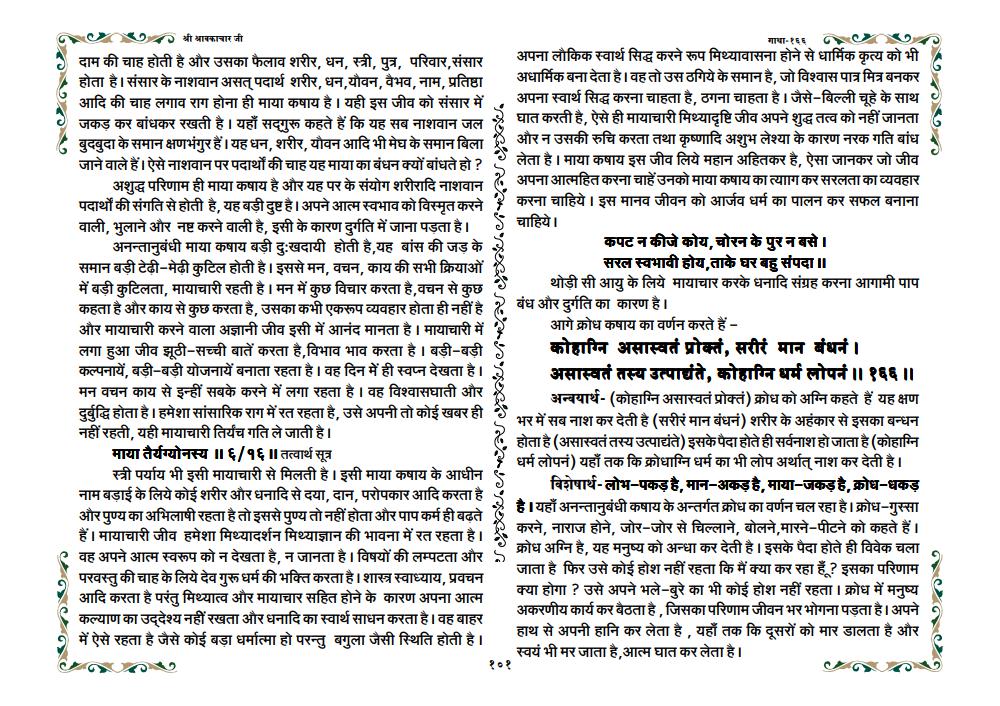________________
श्री श्रावकाचार जी दाम की चाह होती है और उसका फैलाव शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार संसार अपना लौकिक स्वार्थ सिद्ध करने रूप मिथ्यावासना होने से धार्मिक कृत्य को भी होता है। संसार के नाशवान असत् पदार्थ शरीर, धन,यौवन, वैभव, नाम, प्रतिष्ठा
अधार्मिक बना देता है। वह तो उस ठगिये के समान है, जो विश्वास पात्र मित्र बनकर आदि की चाह लगाव राग होना ही माया कषाय है। यही इस जीव को संसार में
अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, ठगना चाहता है। जैसे-बिल्ली चहे के साथ जकड़ कर बांधकर रखती है। यहाँ सदगुरू कहते हैं कि यह सब नाशवान जल घात करती है, ऐसे ही मायाचारी मिथ्यादृष्टि जीव अपने शुद्ध तत्व को नहीं जानता बुदबुदा के समान क्षणभंगुर हैं। यह धन, शरीर, यौवन आदि भी मेघ के समान बिला और न उसकी रुचि करता तथा कृष्णादि अशुभ लेश्या के कारण नरक गति बांध जाने वाले हैं। ऐसे नाशवान पर पदार्थों की चाह यह माया का बंधन क्यों बांधते हो? लेता है। माया कषाय इस जीव लिये महान अहितकर है, ऐसा जानकर जो जीव
___ अशुद्ध परिणाम ही माया कषाय है और यह पर के संयोग शरीरादि नाशवान ८ अपना आत्महित करना चाहें उनको माया कषाय का त्याग कर सरलता का व्यवहार पदार्थों की संगति से होती है, यह बड़ी दुष्ट है। अपने आत्म स्वभावको विस्मृत करने करना चाहिये । इस मानव जीवन को आर्जव धर्म का पालन कर सफल बनाना वाली, भुलाने और नष्ट करने वाली है, इसी के कारण दुर्गति में जाना पड़ता है। चाहिये। अनन्तानुबंधी माया कषाय बड़ी दु:खदायी होती है,यह बांस की जड़ के
कपट न कीजे कोय,चोरन के पुरन बसे। समान बड़ी टेढ़ी-मेढी कुटिल होती है। इससे मन, वचन, काय की सभी क्रियाओं
सरल स्वभावी होय,ताके घर बहु संपदा॥ में बड़ी कुटिलता, मायाचारी रहती है। मन में कछ विचार करता है.वचन से कछ
थोड़ी सी आयु के लिये मायाचार करके धनादि संग्रह करना आगामी पाप कहता है और काय से कुछ करता है, उसका कभी एकरूप व्यवहार होता ही नहीं है बंध और दुर्गति का कारण है। और मायाचारी करने वाला अज्ञानी जीव इसी में आनंद मानता है। मायाचारी में
आगे क्रोध कषाय का वर्णन करते हैं - लगा हुआ जीव झूठी-सच्ची बातें करता है.विभाव भाव करता है। बड़ी-बड़ी कोहाग्नि असास्वतं प्रोक्तं, सरीर मान बंधनं । कल्पनायें, बड़ी-बड़ी योजनायें बनाता रहता है। वह दिन में ही स्वप्न देखता है। असास्वतं तस्य उत्पाचंते, कोहाग्नि धर्म लोपनं ।। १६६।। मन वचन काय से इन्हीं सबके करने में लगा रहता है। वह विश्वासघाती और
अन्वयार्थ- (कोहाग्नि असास्वतं प्रोक्तं) क्रोध को अग्नि कहते हैं यह क्षण दुर्बुद्धि होता है। हमेशा सांसारिक राग में रत रहता है, उसे अपनी तो कोई खबर ही
र भर में सब नाश कर देती है (सरीरं मान बंधन) शरीर के अहंकार से इसका बन्धन नहीं रहती,यही मायाचारी तिर्यंच गति ले जाती है।
होता है (असास्वतंतस्य उत्पाद्यते) इसकेपैदा होते ही सर्वनाश हो जाता है (कोहाग्नि माया तैर्यग्योनस्य ॥६/१६॥ तत्वार्थ सूत्र
" धर्म लोपनं) यहाँ तक कि क्रोधाग्नि धर्म का भी लोप अर्थात् नाश कर देती है। स्त्री पर्याय भी इसी मायाचारी से मिलती है। इसी माया कषाय के आधीन . नाम बड़ाई के लिये कोई शरीर और धनादि से दया, दान, परोपकार आदि करता है
विशेषार्थ-लोभ-पकड़ है,मान-अकड़ है,माया-जकड़ है,क्रोध-धकड़ और पुण्य का अभिलाषी रहता है तो इससे पुण्य तो नहीं होता और पाप कर्म ही बढ़ते :
है।यहाँ अनन्तानुबंधी कषाय के अन्तर्गत क्रोध का वर्णन चल रहा है। क्रोध-गुस्सा हैं। मायाचारी जीव हमेशा मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान की भावना में रत रहता है।
करने, नाराज होने, जोर-जोर से चिल्लाने, बोलने,मारने-पीटने को कहते हैं। वह अपने आत्म स्वरूप को न देखता है, न जानता है। विषयों की लम्पटता और 5
र क्रोध अग्नि है, यह मनुष्य को अन्धा कर देती है। इसके पैदा होते ही विवेक चला परवस्तुकीचाह के लिये देव गुरूधर्म की भक्ति करता है। शास्त्र स्वाध्याय, प्रवचन
जाता है फिर उसे कोई होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ ? इसका परिणाम 1 आदि करता है परंतु मिथ्यात्व और मायाचार सहित होने के कारण अपना आत्म
क्या होगा? उसे अपने भले-बुरे का भी कोई होश नहीं रहता। क्रोध में मनुष्य कल्याण का उद्देश्य नहीं रखता और धनादि का स्वार्थ साधन करता है। वह बाहर
अकरणीय कार्य कर बैठता है, जिसका परिणाम जीवन भर भोगना पड़ता है। अपने में ऐसे रहता है जैसे कोई बड़ा धर्मात्मा हो परन्तु बगुला जैसी स्थिति होती है।
हाथ से अपनी हानि कर लेता है , यहाँ तक कि दूसरों को मार डालता है और स्वयं भी मर जाता है,आत्म घात कर लेता है।
१०१