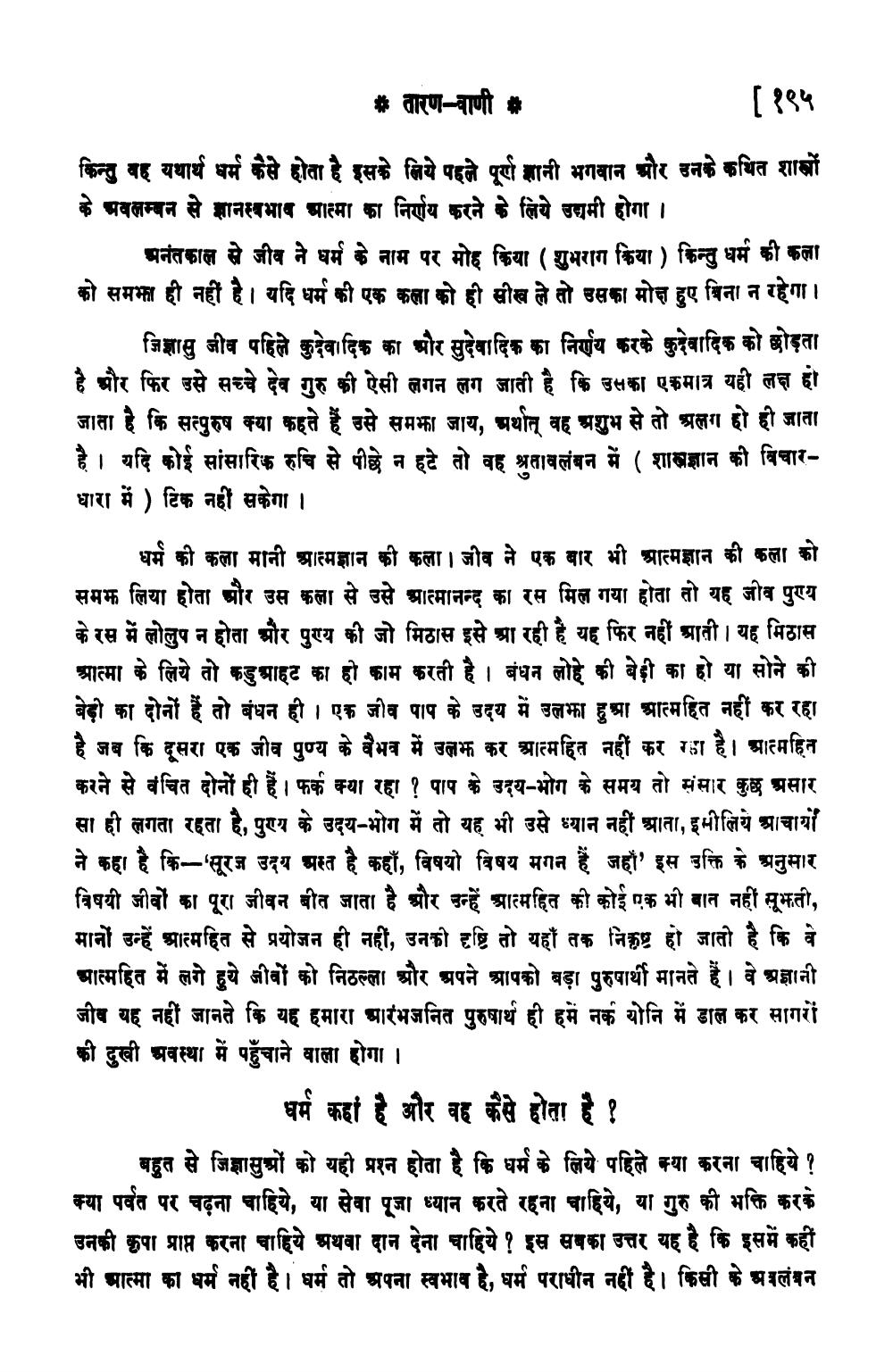________________
* तारण-वाणी.
[१९५
किन्तु वह यथार्थ धर्म कैसे होता है इसके लिये पहले पूर्ण ज्ञानी भगवान और उनके कथित शास्त्रों के अवलम्बन से ज्ञानस्वभाव प्रात्मा का निर्णय करने के लिये उद्यमी होगा।
अनंतकाल से जीव ने धर्म के नाम पर मोह किया ( शुभराग किया ) किन्तु धर्म की कला को समझा ही नहीं है। यदि धर्म की एक कला को ही सीख ले तो उसका मोक्ष हुए बिना न रहेगा।
जिज्ञासु जीव पहिले कुदेवादिक का और सुदेवादिक का निर्णय करके कुदेवादिक को छोड़ता है और फिर उसे सच्चे देव गुरु की ऐसी लगन लग जाती है कि उसका एकमात्र यही लक्ष हो जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते हैं उसे समझा जाय, अर्थात् वह अशुभ से तो अलग हो ही जाता है। यदि कोई सांसारिक रुचि से पीछे न हटे तो वह श्रुतावलंबन में ( शास्त्रज्ञान की विचारधारा में ) टिक नहीं सकेगा।
धर्म की कला मानी आत्मज्ञान की कला। जीव ने एक बार भी आत्मज्ञान की कला को समझ लिया होता और उस कला से उसे आत्मानन्द का रस मिल गया होता तो यह जीव पुण्य के रस में लोलुप न होता और पुण्य की जो मिठास इसे आ रही है यह फिर नहीं आती। यह मिठास
आत्मा के लिये तो कडुबाहट का हो काम करती है । बंधन लोहे की बेड़ी का हो या सोने की बेड़ो का दोनों हैं तो बंधन ही । एक जीव पाप के उदय में उलझा हुआ आत्महित नहीं कर रहा है जब कि दूसरा एक जीव पुण्य के वैभव में उलझ कर आत्महित नहीं कर रहा है। आत्महित करने से वंचित दोनों ही हैं। फर्क क्या रहा ? पाप के उदय-भोग के समय तो संसार कुछ असार सा ही लगता रहता है, पुण्य के उदय-भोग में तो यह भी उसे ध्यान नहीं पाता, इमीलिये प्राचार्यो ने कहा है कि-'सूरज उदय अस्त है कहाँ, विषयो विषय मगन हैं जहाँ' इस उक्ति के अनुसार विषयी जीवों का पूरा जीवन बीत जाता है और उन्हें आत्महित की कोई एक भी बात नहीं सूझती, मानों उन्हें आत्महित से प्रयोजन ही नहीं, उनकी दृष्टि तो यहाँ तक निकृष्ट हो जाती है कि वे
आत्महित में लगे हुये जीवों को निठल्ला और अपने आपको बड़ा पुरुषार्थी मानते हैं। वे अज्ञानी जीव यह नहीं जानते कि यह हमारा प्रारंभजनित पुरुषार्थ ही हमें नर्क योनि में डाल कर सागरों की दुखी अवस्था में पहुंचाने वाला होगा ।
धर्म कहां है और वह कैसे होता है ? बहुत से जिज्ञासुओं को यही प्रश्न होता है कि धर्म के लिये पहिले क्या करना चाहिये ? क्या पर्वत पर चढ़ना चाहिये, या सेवा पूजा ध्यान करते रहना चाहिये, या गुरु की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहिये अथवा दान देना चाहिये ? इस सबका उत्तर यह है कि इसमें कहीं भी मात्मा का धर्म नहीं है। धर्म तो अपना स्वभाव है, धर्म पराधीन नहीं है। किसी के प्रवलंबन