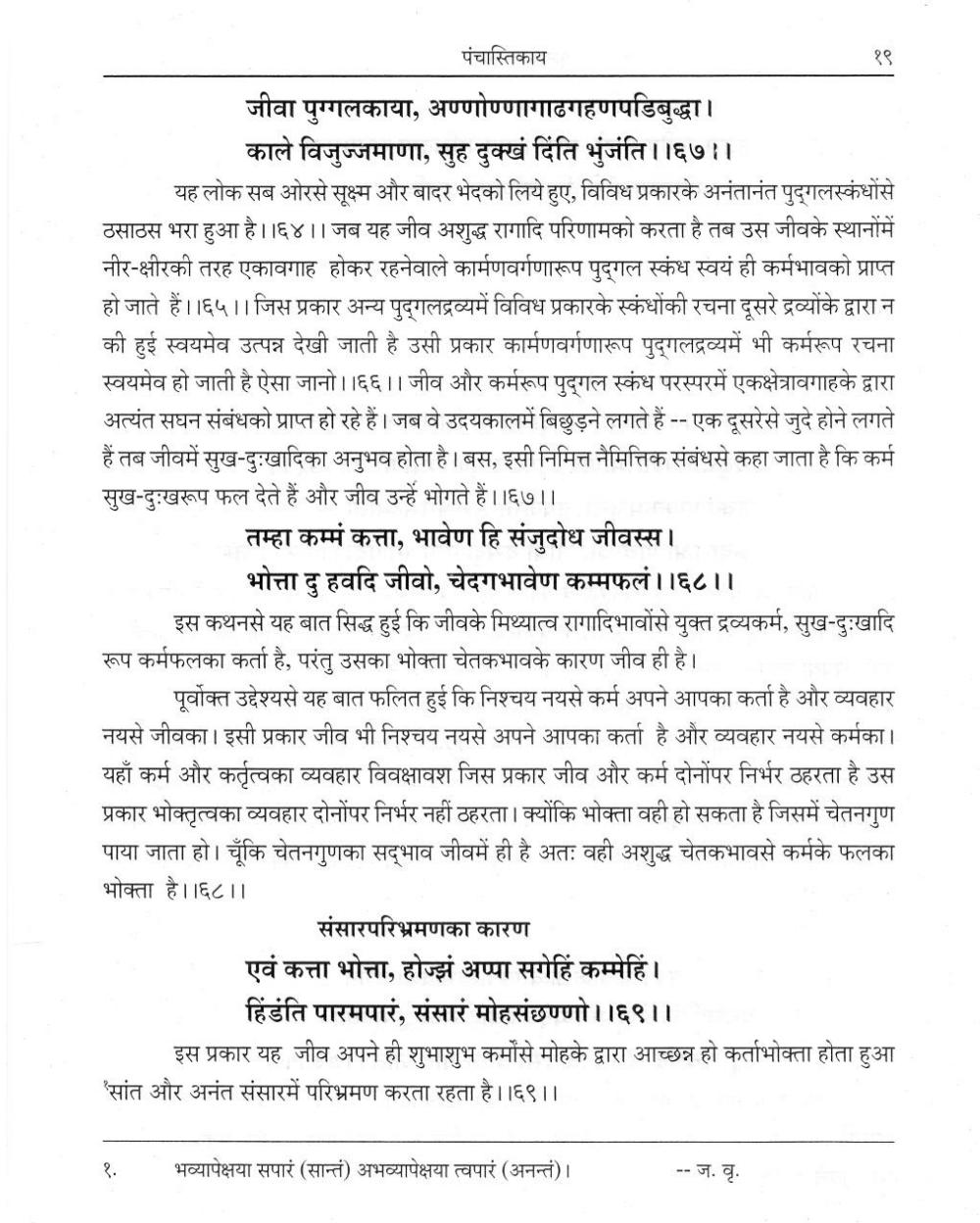________________
पंचास्तिकाय
जीवा पुग्गलकाया, अण्णोण्णागाढगहणपडिबुद्धा।
काले विजुज्जमाणा, सुह दुक्खं दिति भुंजंति।।६७।। यह लोक सब ओरसे सूक्ष्म और बादर भेदको लिये हुए, विविध प्रकारके अनंतानंत पुद्गलस्कंधोंसे ठसाठस भरा हुआ है।।६४ ।। जब यह जीव अशुद्ध रागादि परिणामको करता है तब उस जीवके स्थानोंमें नीर-क्षीरकी तरह एकावगाह होकर रहनेवाले कार्मणवर्गणारूप पुद्गल स्कंध स्वयं ही कर्मभावको प्राप्त हो जाते हैं।।६५ ।। जिस प्रकार अन्य पुद्गलद्रव्यमें विविध प्रकारके स्कंधोंकी रचना दूसरे द्रव्योंके द्वारा न की हुई स्वयमेव उत्पन्न देखी जाती है उसी प्रकार कार्मणवर्गणारूप पुद्गलद्रव्यमें भी कर्मरूप रचना स्वयमेव हो जाती है ऐसा जानो।।६६ ।। जीव और कर्मरूप पुद्गल स्कंध परस्परमें एकक्षेत्रावगाहके द्वारा अत्यंत सघन संबंधको प्राप्त हो रहे हैं। जब वे उदयकालमें बिछुड़ने लगते हैं -- एक दूसरेसे जुदे होने लगते हैं तब जीवमें सुख-दुःखादिका अनुभव होता है। बस, इसी निमित्त नैमित्तिक संबंधसे कहा जाता है कि कर्म सुख-दुःखरूप फल देते हैं और जीव उन्हें भोगते हैं।।६७ ।।
तम्हा कम्मं कत्ता, भावेण हि संजुदोध जीवस्स।
भोत्ता दु हवदि जीवो, चेदगभावेण कम्मफलं ।।६८।। इस कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि जीवके मिथ्यात्व रागादिभावोंसे युक्त द्रव्यकर्म, सुख-दुःखादि रूप कर्मफलका कर्ता है, परंतु उसका भोक्ता चेतकभावके कारण जीव ही है।
पूर्वोक्त उद्देश्यसे यह बात फलित हुई कि निश्चय नयसे कर्म अपने आपका कर्ता है और व्यवहार नयसे जीवका। इसी प्रकार जीव भी निश्चय नयसे अपने आपका कर्ता है और व्यवहार नयसे कर्मका। यहाँ कर्म और कर्तृत्वका व्यवहार विवक्षावश जिस प्रकार जीव और कर्म दोनोंपर निर्भर ठहरता है उस प्रकार भोक्तृत्वका व्यवहार दोनोंपर निर्भर नहीं ठहरता। क्योंकि भोक्ता वही हो सकता है जिसमें चेतनगुण पाया जाता हो। चूँकि चेतनगुणका सद्भाव जीवमें ही है अत: वही अशुद्ध चेतकभावसे कर्मके फलका भोक्ता है।।६८।।
संसारपरिभ्रमणका कारण एवं कत्ता भोत्ता, होज्झं अप्पा सगेहिं कम्मेहिं।
हिंडंति पारमपारं, संसारं मोहसंछण्णो।।६९।। इस प्रकार यह जीव अपने ही शुभाशुभ कर्मोंसे मोहके द्वारा आच्छन्न हो कर्ताभोक्ता होता हुआ 'सांत और अनंत संसारमें परिभ्रमण करता रहता है।।९।।
भव्यापेक्षया सपारं (सान्त) अभव्यापेक्षया त्वपारं (अनन्तं)।
-- ज. वृ.