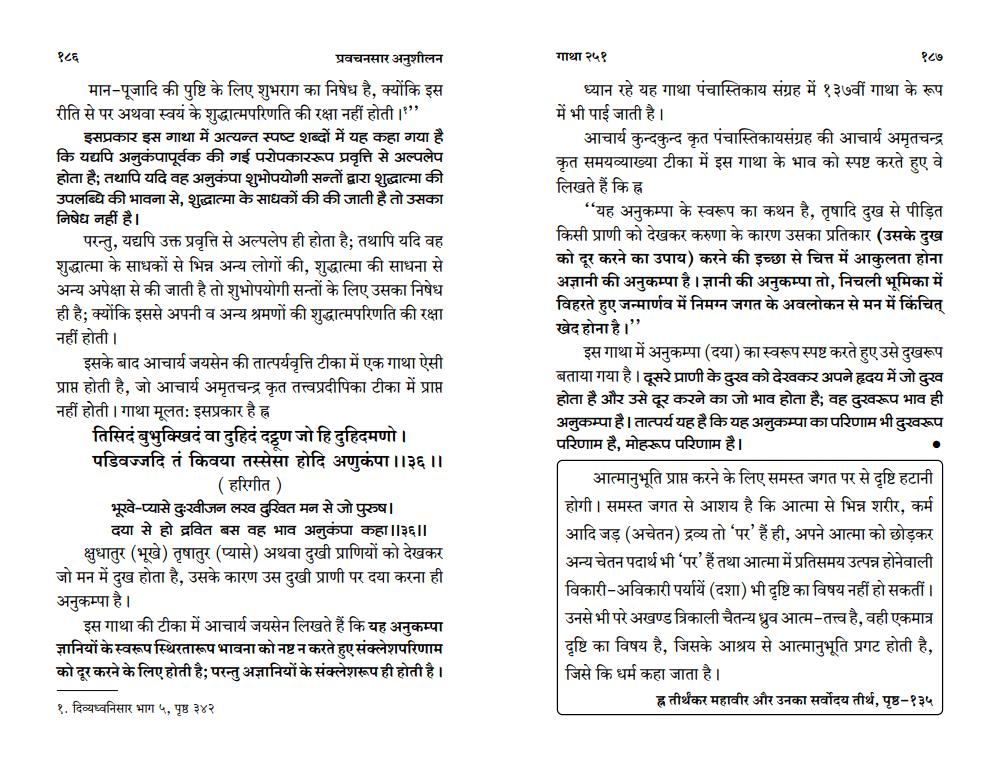________________
प्रवचनसार अनुशीलन मान-पूजादि की पुष्टि के लिए शुभराग का निषेध है, क्योंकि इस रीति से पर अथवा स्वयं के शुद्धात्मपरिणति की रक्षा नहीं होती । ”
इसप्रकार इस गाथा में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि यद्यपि अनुकंपापूर्वक की गई परोपकाररूप प्रवृत्ति से अल्पलेप होता है; तथापि यदि वह अनुकंपा शुभोपयोगी सन्तों द्वारा शुद्धात्मा की उपलब्धि की भावना से, शुद्धात्मा के साधकों की की जाती है तो उसका निषेध नहीं है ।
परन्तु, यद्यपि उक्त प्रवृत्ति से अल्पलेप ही होता है; तथापि यदि वह शुद्धात्मा के साधकों से भिन्न अन्य लोगों की, शुद्धात्मा की साधना से अन्य अपेक्षा से की जाती है तो शुभोपयोगी सन्तों के लिए उसका निषेध ही है; क्योंकि इससे अपनी व अन्य श्रमणों की शुद्धात्मपरिणति की रक्षा नहीं होती।
१८६
इसके बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्यवृत्ति टीका में एक गाथा ऐसी प्राप्त होती है, जो आचार्य अमृतचन्द्र कृत तत्त्वप्रदीपिका टीका में प्राप्त नहीं होती । गाथा मूलतः इसप्रकार है ह्र
तिसिदं बुभुक्खिदं वा दुहिदं दट्ठूण जो हि दुहिदमणो । पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ।। ३६ ।। ( हरिगीत )
भूखे-प्यासे दुःखीजन लख दुखित मन से जो पुरुष । दया से हो द्रवित बस वह भाव अनुकंपा कहा ||३६|| क्षुधातुर (भूखे) तृषातुर (प्यासे) अथवा दुखी प्राणियों को देखकर जो मन में दुख होता है, उसके कारण उस दुखी प्राणी पर दया करना ही अनुकम्पा है।
इस गाथा की टीका में आचार्य जयसेन लिखते हैं कि यह अनुकम्पा ज्ञानियों के स्वरूप स्थिरतारूप भावना को नष्ट न करते हुए संक्लेशपरिणाम को दूर करने के लिए होती है; परन्तु अज्ञानियों के संक्लेशरूप ही होती है । १. दिव्यध्वनिसार भाग ५, पृष्ठ ३४२
गाथा २५१
१८७
ध्यान रहे यह गाथा पंचास्तिकाय संग्रह में १३७वीं गाथा के रूप में भी पाई जाती है।
आचार्य कुन्दकुन्द कृत पंचास्तिकायसंग्रह की आचार्य अमृतचन्द्र कृत समयव्याख्या टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि
"यह अनुकम्पा के स्वरूप का कथन है, तृषादि दुख से पीड़ित किसी प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार ( उसके दुख को दूर करने का उपाय) करने की इच्छा से चित्त में आकुलता होना अज्ञानी की अनुकम्पा है। ज्ञानी की अनुकम्पा तो, निचली भूमिका में विहरते हुए जन्मार्णव में निमग्न जगत के अवलोकन से मन में किंचित् खेद होना है।"
इस गाथा में अनुकम्पा (दया) का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसे दुखरूप बताया गया है। दूसरे प्राणी के दुख को देखकर अपने हृदय में जो दुख होता है और उसे दूर करने का जो भाव होता है; वह दुखरूप भाव ही अनुकम्पा है। तात्पर्य यह है कि यह अनुकम्पा का परिणाम भी दुखरूप परिणाम है, मोहरूप परिणाम है।
आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। समस्त जगत से आशय है कि आत्मा से भिन्न शरीर, कर्म आदि जड़ (अचेतन) द्रव्य तो 'पर' हैं ही, अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी 'पर' हैं तथा आत्मा में प्रतिसमय उत्पन्न होनेवाली विकारी-अविकारी पर्यायें (दशा) भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकतीं। उनसे भी परे अखण्ड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म-तत्त्व है, वही एकमात्र | दृष्टि का विषय है, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रगट होती है, जिसे कि धर्म कहा जाता है।
ह्न तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, पृष्ठ- १३५