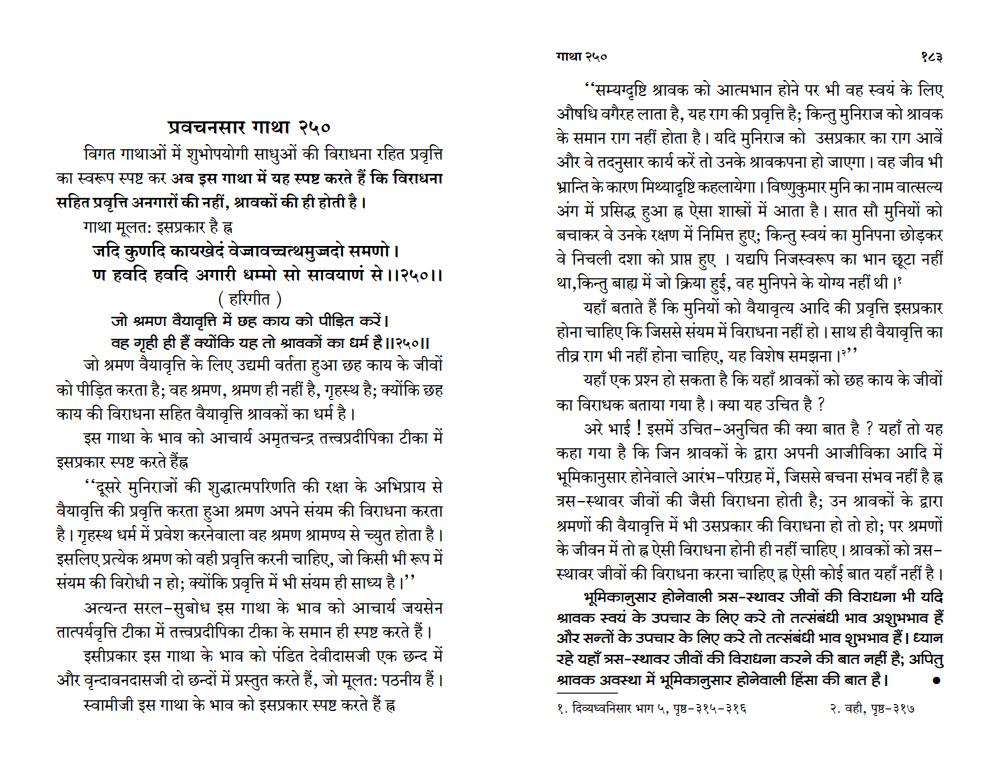________________
प्रवचनसार गाथा २५०
विगत गाथाओं में शुभोपयोगी साधुओं की विराधना रहित प्रवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट कर अब इस गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि विराधना सहित प्रवृत्ति अनगारों की नहीं, श्रावकों की ही होती है ।
गाथा मूलतः इसप्रकार है ह्र
जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो ।
ण हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से ।। २५० ।। ( हरिगीत )
जो श्रमण वैयावृत्ति में छह काय को पीड़ित करें।
वह गृही ही हैं क्योंकि यह तो श्रावकों का धर्म है ।। २५० ॥ जो श्रमण वैयावृत्ति के लिए उद्यमी वर्तता हुआ छह काय के जीवों को पीड़ित करता है; वह श्रमण, श्रमण ही नहीं है, गृहस्थ है; क्योंकि छह काय की विराधना सहित वैयावृत्ति श्रावकों का धर्म है।
इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचन्द्र तत्त्वप्रदीपिका टीका में इसप्रकार स्पष्ट करते हैं
“दूसरे मुनिराजों की शुद्धात्मपरिणति की रक्षा के अभिप्राय से वैयावृत्ति की प्रवृत्ति करता हुआ श्रमण अपने संयम की विराधना करता है। गृहस्थ धर्म में प्रवेश करनेवाला वह श्रमण श्रामण्य से च्युत होता है । इसलिए प्रत्येक श्रमण को वही प्रवृत्ति करनी चाहिए, जो किसी भी रूप में संयम की विरोधी न हो; क्योंकि प्रवृत्ति में भी संयम ही साध्य है।"
अत्यन्त सरल-सुबोध इस गाथा के भाव को आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में तत्त्वप्रदीपिका टीका के समान ही स्पष्ट करते हैं।
इसीप्रकार इस गाथा के भाव को पंडित देवीदासजी एक छन्द में और वृन्दावनदासजी दो छन्दों में प्रस्तुत करते हैं, जो मूलत: पठनीय हैं। स्वामीजी इस गाथा के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र
गाथा २५०
१८३
" सम्यग्दृष्टि श्रावक को आत्मभान होने पर भी वह स्वयं के लिए औषधि वगैरह लाता है, यह राग की प्रवृत्ति है; किन्तु मुनिराज को श्रावक समान राग नहीं होता है। यदि मुनिराज को उसप्रकार का राग आवें और वे तदनुसार कार्य करें तो उनके श्रावकपना हो जाएगा। वह जीव भी भ्रान्ति के कारण मिथ्यादृष्टि कहलायेगा। विष्णुकुमार मुनि का नाम वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुआ ह्र ऐसा शास्त्रों में आता है। सात सौ मुनियों को बचाकर वे उनके रक्षण में निमित्त हुए; किन्तु स्वयं का मुनिपना छोड़कर वे निचली दशा को प्राप्त हुए । यद्यपि निजस्वरूप का भान छूटा नहीं था, किन्तु बाह्य में जो क्रिया हुई, वह मुनिपने के योग्य नहीं थी ।
यहाँ बताते हैं कि मुनियों को वैयावृत्य आदि की प्रवृत्ति इसप्रकार होना चाहिए कि जिससे संयम में विराधना नहीं हो। साथ ही वैयावृत्ति का तीव्र राग भी नहीं होना चाहिए, यह विशेष समझना । २”
यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ श्रावकों को छह काय के जीवों का विराधक बताया गया है। क्या यह उचित है ?
अरे भाई ! इसमें उचित - अनुचित की क्या बात है ? यहाँ तो यह कहा गया है कि जिन श्रावकों के द्वारा अपनी आजीविका आदि में भूमिकानुसार होनेवाले आरंभ - परिग्रह में, जिससे बचना संभव नहीं है ह्र त्रस-स्थावर जीवों की जैसी विराधना होती है; उन श्रावकों के द्वारा श्रमणों की वैयावृत्ति में भी उसप्रकार की विराधना हो तो हो; पर श्रमणों के जीवन में तो ह्र ऐसी विराधना होनी ही नहीं चाहिए। श्रावकों को त्रसस्थावर जीवों की विराधना करना चाहिए ह्र ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है ।
भूमिकानुसार होनेवाली त्रस स्थावर जीवों की विराधना भी यदि श्रावक स्वयं के उपचार के लिए करे तो तत्संबंधी भाव अशुभभाव हैं और सन्तों के उपचार के लिए करे तो तत्संबंधी भाव शुभभाव हैं। ध्यान रहे यहाँ स-स्थावर जीवों की विराधना करने की बात नहीं है; अपितु श्रावक अवस्था में भूमिकानुसार होनेवाली हिंसा की बात है। १. दिव्यध्वनिसार भाग ५, पृष्ठ ३१५-३१६
२. वही, पृष्ठ ३१७