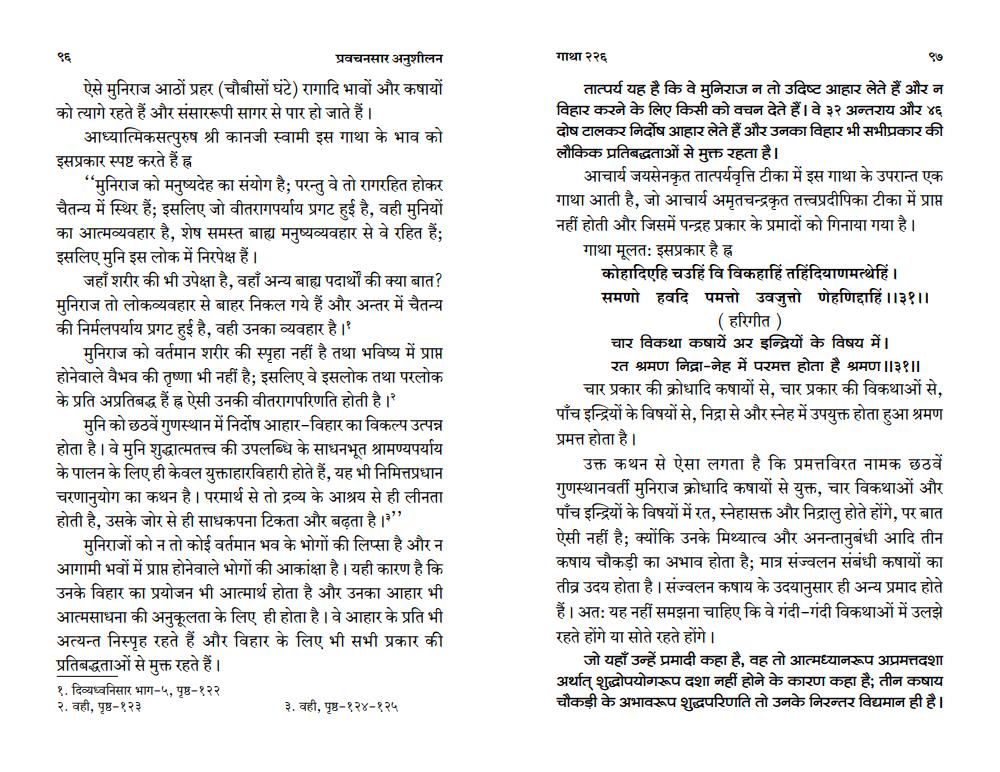________________
गाथा २२६
प्रवचनसार अनुशीलन ऐसे मुनिराज आठों प्रहर (चौबीसों घंटे) रागादि भावों और कषायों को त्यागे रहते हैं और संसाररूपी सागर से पार हो जाते हैं।
आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इस गाथा के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्न
"मुनिराज को मनुष्यदेह का संयोग है; परन्तु वे तो रागरहित होकर चैतन्य में स्थिर हैं; इसलिए जो वीतरागपर्याय प्रगट हुई है, वही मुनियों का आत्मव्यवहार है, शेष समस्त बाह्य मनुष्यव्यवहार से वे रहित हैं; इसलिए मुनि इस लोक में निरपेक्ष हैं।
जहाँ शरीर की भी उपेक्षा है, वहाँ अन्य बाह्य पदार्थों की क्या बात? मुनिराज तो लोकव्यवहार से बाहर निकल गये हैं और अन्तर में चैतन्य की निर्मलपर्याय प्रगट हुई है, वही उनका व्यवहार है।' ___ मुनिराज को वर्तमान शरीर की स्पृहा नहीं है तथा भविष्य में प्राप्त होनेवाले वैभव की तृष्णा भी नहीं है; इसलिए वे इसलोक तथा परलोक के प्रति अप्रतिबद्ध हैं ह्र ऐसी उनकी वीतरागपरिणति होती है। ____ मुनि को छठवें गुणस्थान में निर्दोष आहार-विहार का विकल्प उत्पन्न होता है। वे मुनि शुद्धात्मतत्त्व की उपलब्धि के साधनभूत श्रामण्यपर्याय के पालन के लिए ही केवल युक्ताहारविहारी होते हैं, यह भी निमित्तप्रधान चरणानुयोग का कथन है। परमार्थ से तो द्रव्य के आश्रय से ही लीनता होती है, उसके जोर से ही साधकपना टिकता और बढ़ता है।"
मुनिराजों को न तो कोई वर्तमान भव के भोगों की लिप्सा है और न आगामी भवों में प्राप्त होनेवाले भोगों की आकांक्षा है। यही कारण है कि उनके विहार का प्रयोजन भी आत्मार्थ होता है और उनका आहार भी आत्मसाधना की अनुकूलता के लिए ही होता है। वे आहार के प्रति भी अत्यन्त निस्पृह रहते हैं और विहार के लिए भी सभी प्रकार की प्रतिबद्धताओं से मुक्त रहते हैं। १. दिव्यध्वनिसार भाग-५, पृष्ठ-१२२ २. वही, पृष्ठ-१२३
३. वही, पृष्ठ-१२४-१२५
तात्पर्य यह है कि वे मुनिराज न तो उदिष्ट आहार लेते हैं और न विहार करने के लिए किसी को वचन देते हैं। वे ३२ अन्तराय और ४६ दोष टालकर निर्दोष आहार लेते हैं और उनका विहार भी सभीप्रकार की लौकिक प्रतिबद्धताओं से मुक्त रहता है। ___ आचार्य जयसेनकृत तात्पर्यवृत्ति टीका में इस गाथा के उपरान्त एक गाथा आती है, जो आचार्य अमृतचन्द्रकृत तत्त्वप्रदीपिका टीका में प्राप्त नहीं होती और जिसमें पन्द्रह प्रकार के प्रमादों को गिनाया गया है। गाथा मूलत: इसप्रकार है तू
कोहादिएहि चउहिं वि विकहाहि तहिंदियाणमत्थेहिं । समणो हवदि पमत्तो उवजुत्तो णेहणिद्दाहिं ।।३१।।
(हरिगीत ) चार विकथा कषायें अर इन्द्रियों के विषय में।
रत श्रमण निद्रा-नेह में परमत्त होता है श्रमण ||३१|| चार प्रकार की क्रोधादि कषायों से, चार प्रकार की विकथाओं से, पाँच इन्द्रियों के विषयों से, निद्रा से और स्नेह में उपयुक्त होता हुआ श्रमण प्रमत्त होता है।
उक्त कथन से ऐसा लगता है कि प्रमत्तविरत नामक छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज क्रोधादि कषायों से युक्त, चार विकथाओं और पाँच इन्द्रियों के विषयों में रत, स्नेहासक्त और निद्रालु होते होंगे, पर बात ऐसी नहीं है; क्योंकि उनके मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी आदि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है; मात्र संज्वलन संबंधी कषायों का तीव्र उदय होता है। संज्वलन कषाय के उदयानुसार ही अन्य प्रमाद होते हैं। अत: यह नहीं समझना चाहिए कि वे गंदी-गंदी विकथाओं में उलझे रहते होंगे या सोते रहते होंगे।
जो यहाँ उन्हें प्रमादी कहा है, वह तो आत्मध्यानरूप अप्रमत्तदशा अर्थात् शद्धोपयोगरूप दशा नहीं होने के कारण कहा है; तीन कषाय चौकड़ी के अभावरूप शुद्धपरिणति तो उनके निरन्तर विद्यमान ही है।