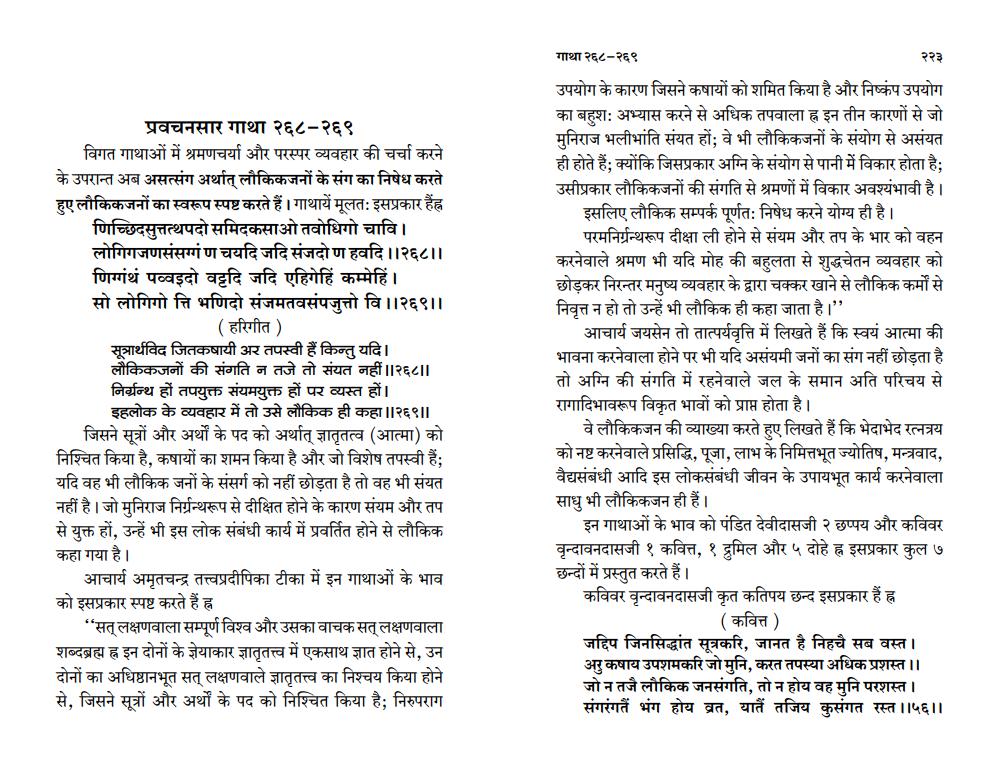________________
प्रवचनसार गाथा २६८- २६९
विगत गाथाओं में श्रमणचर्या और परस्पर व्यवहार की चर्चा करने के उपरान्त अब असत्संग अर्थात् लौकिकजनों के संग का निषेध करते हुए लौकिकजनों का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। गाथायें मूलत: इसप्रकार हैं णिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाओ तवोधिगो चावि । लोगिगजणसंसग्गं ण चयदि जदि संजदो ण हवदि । । २६८ ।। णिग्गंथं पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहिं कम्मेहिं । सो लोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंपजुत्तो वि ।। २६९ ।। ( हरिगीत )
सूत्रार्थविद जितकषायी अर तपस्वी हैं किन्तु यदि । लौकिकजनों की संगति न तजे तो संयत नहीं ॥ २६८ ॥ निर्ग्रन्थ हों तपयुक्त संयमयुक्त हों पर व्यस्त हों । इहलोक के व्यवहार में तो उसे लौकिक ही कहा ॥ २६९ ॥ जिसने सूत्रों और अर्थों के पद को अर्थात् ज्ञातृतत्व (आत्मा) को निश्चित किया है, कषायों का शमन किया है और जो विशेष तपस्वी हैं; यदि वह भी लौकिक जनों के संसर्ग को नहीं छोड़ता है तो वह भी संयत नहीं है। जो मुनिराज निर्ग्रन्थरूप से दीक्षित होने के कारण संयम और तप से युक्त हों, उन्हें भी इस लोक संबंधी कार्य में प्रवर्तित होने से लौकिक कहा गया है।
आचार्य अमृतचन्द्र तत्त्वप्रदीपिका टीका में इन गाथाओं के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं
“सत् लक्षणवाला सम्पूर्ण विश्व और उसका वाचक सत् लक्षणवाला शब्दब्रह्म ह्न इन दोनों के ज्ञेयाकार ज्ञातृतत्त्व में एकसाथ ज्ञात होने से, उन दोनों का अधिष्ठानभूत सत् लक्षणवाले ज्ञातृतत्त्व का निश्चय किया होने से, जिसने सूत्रों और अर्थों के पद को निश्चित किया है; निरुपराग
गाथा २६८- २६९
उपयोग के कारण जिसने कषायों को शमित किया है और निष्कंप उपयोग का बहुशः अभ्यास करने से अधिक तपवाला ह्न इन तीन कारणों से जो मुनिराज भलीभांति संयत हों; वे भी लौकिकजनों के संयोग से असंयत ही होते हैं; क्योंकि जिसप्रकार अग्नि के संयोग से पानी में विकार होता है; उसीप्रकार लौकिकजनों की संगति से श्रमणों में विकार अवश्यंभावी है।
२२३
इसलिए लौकिक सम्पर्क पूर्णतः निषेध करने योग्य ही है। परमनिर्ग्रन्थरूप दीक्षा ली होने से संयम और तप के भार को वहन करनेवाले श्रमण भी यदि मोह की बहुलता से शुद्धचेतन व्यवहार को छोड़कर निरन्तर मनुष्य व्यवहार के द्वारा चक्कर खाने से लौकिक कर्मों से निवृत्त न हो तो उन्हें भी लौकिक ही कहा जाता है।"
आचार्य जयसेन तो तात्पर्यवृत्ति में लिखते हैं कि स्वयं आत्मा की भावना करनेवाला होने पर भी यदि असंयमी जनों का संग नहीं छोड़ता है। तो अग्नि की संगति में रहनेवाले जल के समान अति परिचय से रागादिभावरूप विकृत भावों को प्राप्त होता है।
वे लौकिकजन की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि भेदाभेद रत्नत्रय नष्ट करनेवाले प्रसिद्धि, पूजा, लाभ के निमित्तभूत ज्योतिष, मन्त्रवाद, वैद्यसंबंधी आदि इस लोकसंबंधी जीवन के उपायभूत कार्य करनेवाला साधु भी लौकिकजन ही हैं।
इन गाथाओं के भाव को पंडित देवीदासजी २ छप्पय और कविवर वृन्दावनदासजी १ कवित्त, १ द्रुमिल और ५ दोहे ह्न इसप्रकार कुल ७ छन्दों में प्रस्तुत करते हैं।
कविवर वृन्दावनदासजी कृत कतिपय छन्द इसप्रकार हैं ह्र ( कवित्त )
दिप जिनसिद्धांत सूत्रकरि, जानत है निहचै सब वस्त । अरु कषाय उपशमकरि जो मुनि, करत तपस्या अधिक प्रशस्त ।। जो न तजै लौकिक जनसंगति, तो न होय वह मुनि परशस्त । संगरंगत भंग होय व्रत, यातैं तजिय कुसंगत रस्त ।। ५६ ।।