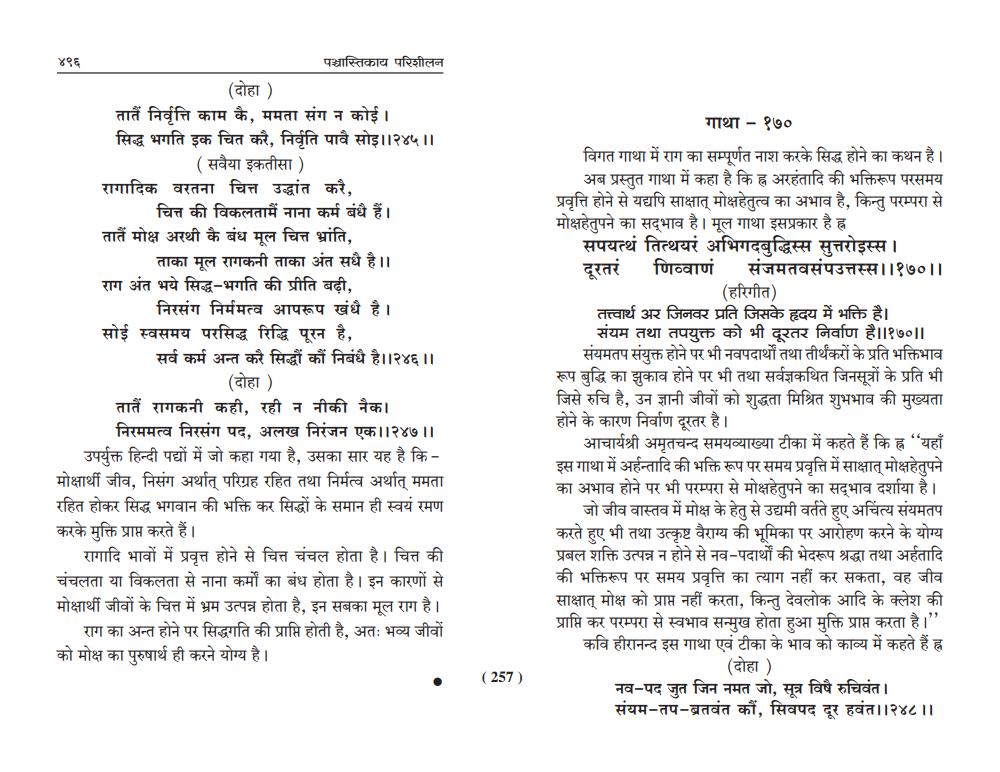________________
४९६
पञ्चास्तिकाय परिशीलन (दोहा) तातै निर्वृत्ति काम कै, ममता संग न कोई। सिद्ध भगति इक चित करै, निर्वृति पावै सोइ।।२४५ ।।
(सवैया इकतीसा ) रागादिक वरतना चित्त उद्धांत करै,
चित्त की विकलतामैं नाना कर्म बंध हैं। तारौं मोक्ष अरथी के बंध मूल चित्त भ्रांति,
ताका मूल रागकनी ताका अंत सधै है।। राग अंत भये सिद्ध-भगति की प्रीति बढ़ी,
निरसंग निर्ममत्व आपरूप खंधै है। सोई स्वसमय परसिद्ध रिद्धि पूरन है, सर्व कर्म अन्त करै सिद्धौं कौं निबंधै है।।२४६ ।।
(दोहा) तातें रागकनी कही, रही न नीकी नैक।
निरममत्व निरसंग पद, अलख निरंजन एक।।२४७ ।। उपर्युक्त हिन्दी पद्यों में जो कहा गया है, उसका सार यह है कि - मोक्षार्थी जीव, निसंग अर्थात् परिग्रह रहित तथा निर्मत्व अर्थात् ममता रहित होकर सिद्ध भगवान की भक्ति कर सिद्धों के समान ही स्वयं रमण करके मुक्ति प्राप्त करते हैं।
रागादि भावों में प्रवृत्त होने से चित्त चंचल होता है। चित्त की चंचलता या विकलता से नाना कर्मों का बंध होता है। इन कारणों से मोक्षार्थी जीवों के चित्त में भ्रम उत्पन्न होता है, इन सबका मूल राग है।
राग का अन्त होने पर सिद्धगति की प्राप्ति होती है, अतः भव्य जीवों को मोक्ष का पुरुषार्थ ही करने योग्य है।
.
गाथा - १७० विगत गाथा में राग का सम्पूर्णत नाश करके सिद्ध होने का कथन है।
अब प्रस्तुत गाथा में कहा है कि ह्र अरहंतादि की भक्तिरूप परसमय प्रवृत्ति होने से यद्यपि साक्षात् मोक्षहेतुत्व का अभाव है, किन्तु परम्परा से मोक्षहेतुपने का सद्भाव है। मूल गाथा इसप्रकार है तू
सपयत्थं तित्थयरं अभिगदबुद्धिस्स सुत्तरोइस्स । दूरतरं णिव्वाणं संजमतवसंपउत्तस्स।।१७०।।
(हरिगीत) तत्त्वार्थ अर जिनवर प्रति जिसके हृदय में भक्ति है। संयम तथा तपयुक्त को भी दूरतर निर्वाण है।।१७०|| संयमतप संयुक्त होने पर भी नवपदार्थों तथा तीर्थंकरों के प्रति भक्तिभाव रूप बुद्धि का झुकाव होने पर भी तथा सर्वज्ञकथित जिनसूत्रों के प्रति भी जिसे रुचि है, उन ज्ञानी जीवों को शुद्धता मिश्रित शुभभाव की मुख्यता होने के कारण निर्वाण दूरतर है।
आचार्यश्री अमृतचन्द समयव्याख्या टीका में कहते हैं कि ह्र “यहाँ इस गाथा में अर्हन्तादि की भक्ति रूप पर समय प्रवृत्ति में साक्षात् मोक्षहेतुपने का अभाव होने पर भी परम्परा से मोक्षहेतुपने का सद्भाव दर्शाया है।
जो जीव वास्तव में मोक्ष के हेतु से उद्यमी वर्तते हुए अचिंत्य संयमतप करते हुए भी तथा उत्कृष्ट वैराग्य की भूमिका पर आरोहण करने के योग्य प्रबल शक्ति उत्पन्न न होने से नव-पदार्थों की भेदरूप श्रद्धा तथा अर्हतादि की भक्तिरूप पर समय प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर सकता, वह जीव साक्षात् मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, किन्तु देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति कर परम्परा से स्वभाव सन्मुख होता हुआ मुक्ति प्राप्त करता है।" कवि हीरानन्द इस गाथा एवं टीका के भाव को काव्य में कहते हैं ह्न
(दोहा) नव-पद जुत जिन नमत जो, सूत्र विषै रुचिवंत । संयम-तप-ब्रतवंत कौं, सिवपद दूर हवंत।।२४८।।
(257)