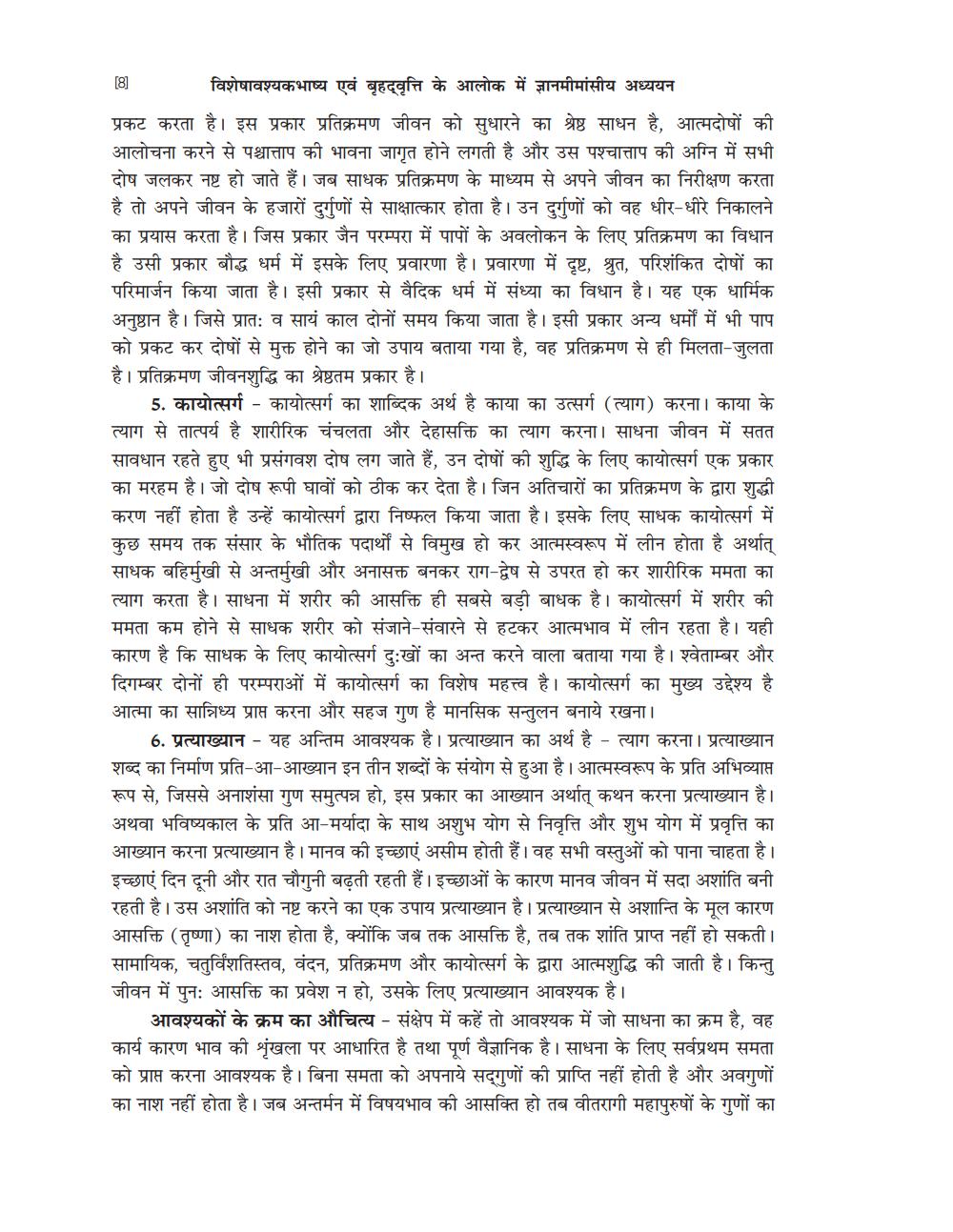________________
विशेषावश्यकभाष्य एवं बृहद्वृत्ति के आलोक में ज्ञानमीमांसीय अध्ययन प्रकट करता है। इस प्रकार प्रतिक्रमण जीवन को सुधारने का श्रेष्ठ साधन है, आत्मदोषों की आलोचना करने से पश्चात्ताप की भावना जागृत होने लगती है और उस पश्चात्ताप की अग्नि में सभी दोष जलकर नष्ट हो जाते हैं। जब साधक प्रतिक्रमण के माध्यम से अपने जीवन का निरीक्षण करता है तो अपने जीवन के हजारों दुर्गुणों से साक्षात्कार होता है। उन दुर्गुणों को वह धीर-धीरे निकालने का प्रयास करता है। जिस प्रकार जैन परम्परा में पापों के अवलोकन के लिए प्रतिक्रमण का विधान है उसी प्रकार बौद्ध धर्म में इसके लिए प्रवारणा है। प्रवारणा में दृष्ट, श्रुत, परिशंकित दोषों का परिमार्जन किया जाता है। इसी प्रकार से वैदिक धर्म में संध्या का विधान है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है। जिसे प्रातः व सायं काल दोनों समय किया जाता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी पाप को प्रकट कर दोषों से मुक्त होने का जो उपाय बताया गया है, वह प्रतिक्रमण से ही मिलता-जुलता है। प्रतिक्रमण जीवनशुद्धि का श्रेष्ठतम प्रकार है।
5. कायोत्सर्ग - कायोत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ है काया का उत्सर्ग (त्याग) करना। काया के त्याग से तात्पर्य है शारीरिक चंचलता और देहासक्ति का त्याग करना। साधना जीवन में सतत सावधान रहते हुए भी प्रसंगवश दोष लग जाते हैं, उन दोषों की शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग एक प्रकार का मरहम है। जो दोष रूपी घावों को ठीक कर देता है। जिन अतिचारों का प्रतिक्रमण के द्वारा शुद्धी करण नहीं होता है उन्हें कायोत्सर्ग द्वारा निष्फल किया जाता है। इसके लिए साधक कायोत्सर्ग में कुछ समय तक संसार के भौतिक पदार्थों से विमुख हो कर आत्मस्वरूप में लीन होता है अर्थात् साधक बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी और अनासक्त बनकर राग-द्वेष से उपरत हो कर शारीरिक ममता का त्याग करता है। साधना में शरीर की आसक्ति ही सबसे बड़ी बाधक है। कायोत्सर्ग में शरीर की ममता कम होने से साधक शरीर को संजाने-संवारने से हटकर आत्मभाव में लीन रहता है। यही कारण है कि साधक के लिए कायोत्सर्ग दु:खों का अन्त करने वाला बताया गया है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में कायोत्सर्ग का विशेष महत्त्व है। कायोत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का सान्निध्य प्राप्त करना और सहज गुण है मानसिक सन्तुलन बनाये रखना।
6. प्रत्याख्यान - यह अन्तिम आवश्यक है। प्रत्याख्यान का अर्थ है - त्याग करना। प्रत्याख्यान शब्द का निर्माण प्रति-आ-आख्यान इन तीन शब्दों के संयोग से हुआ है। आत्मस्वरूप के प्रति अभिव्याप्त रूप से, जिससे अनाशंसा गुण समुत्पन्न हो, इस प्रकार का आख्यान अर्थात् कथन करना प्रत्याख्यान है। अथवा भविष्यकाल के प्रति आ-मर्यादा के साथ अशुभ योग से निवृत्ति और शुभ योग में प्रवृत्ति का आख्यान करना प्रत्याख्यान है। मानव की इच्छाएं असीम होती हैं। वह सभी वस्तुओं को पाना चाहता है। इच्छाएं दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती रहती हैं। इच्छाओं के कारण मानव जीवन में सदा अशांति बनी रहती है। उस अशांति को नष्ट करने का एक उपाय प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान से अशान्ति के मूल कारण आसक्ति (तृष्णा) का नाश होता है, क्योंकि जब तक आसक्ति है, तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदन, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग के द्वारा आत्मशुद्धि की जाती है। किन्तु जीवन में पुनः आसक्ति का प्रवेश न हो, उसके लिए प्रत्याख्यान आवश्यक है।
आवश्यकों के क्रम का औचित्य - संक्षेप में कहें तो आवश्यक में जो साधना का क्रम है, वह कार्य कारण भाव की श्रृंखला पर आधारित है तथा पूर्ण वैज्ञानिक है। साधना के लिए सर्वप्रथम समता को प्राप्त करना आवश्यक है। बिना समता को अपनाये सद्गुणों की प्राप्ति नहीं होती है और अवगुणों का नाश नहीं होता है। जब अन्तर्मन में विषयभाव की आसक्ति हो तब वीतरागी महापुरुषों के गुणों का