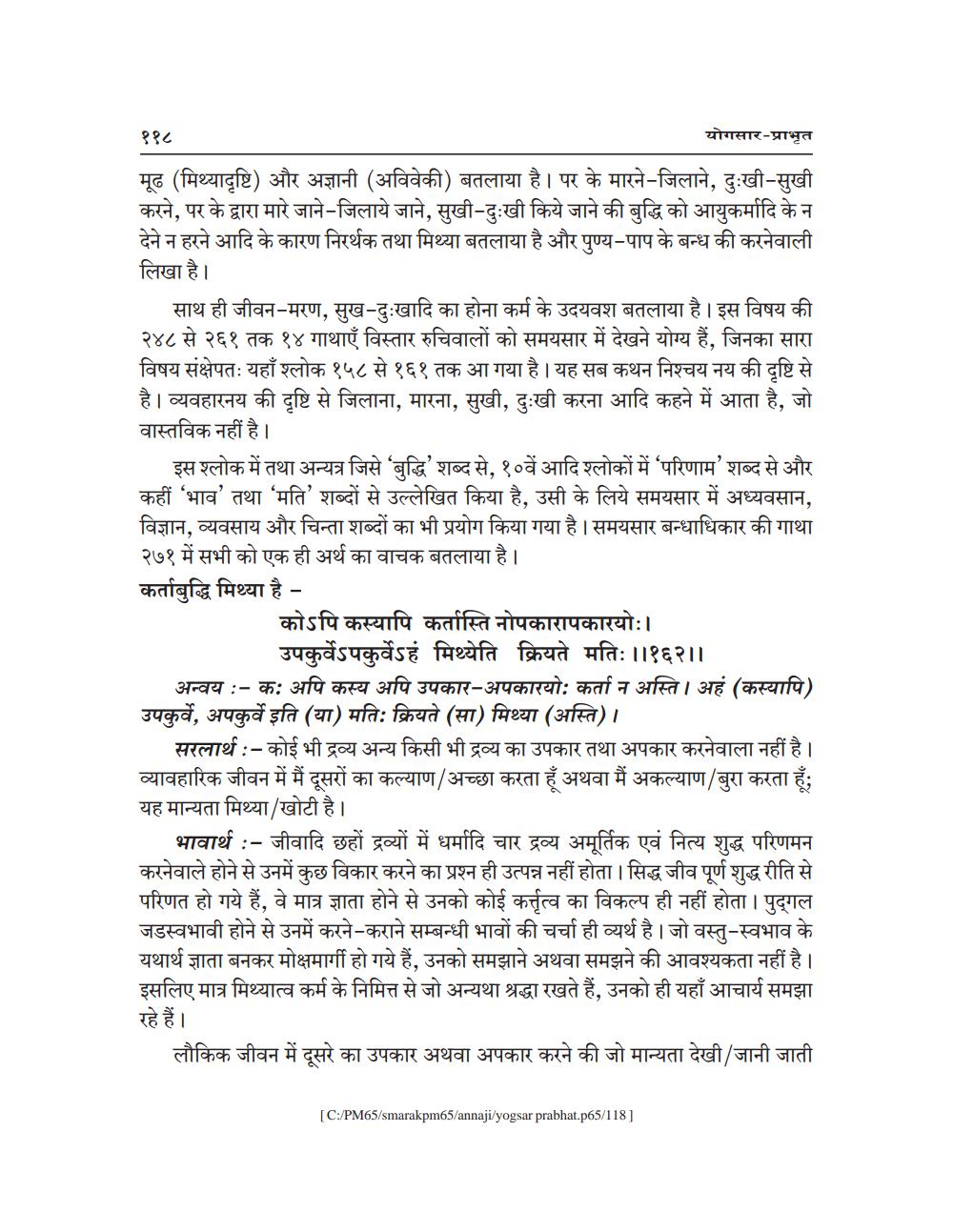________________
योगसार प्राभृत
१९८
मूढ (मिथ्यादृष्टि) और अज्ञानी (अविवेकी) बतलाया है । पर के मारने- जिलाने, दुःखी - सुखी करने, पर के द्वारा मारे जाने - जिलाये जाने, सुखी - दुःखी किये जाने की बुद्धि को आयुकर्मादि के न देने न हरने आदि के कारण निरर्थक तथा मिथ्या बतलाया है और पुण्य-पाप के बन्ध की करनेवाली लिखा है ।
साथ ही जीवन-मरण, सुख-दुःखादि का होना कर्म के उदयवश बतलाया है। इस विषय की २४८ से २६१ तक १४ गाथाएँ विस्तार रुचिवालों को समयसार में देखने योग्य हैं, जिनका सारा विषय संक्षेपतः यहाँ श्लोक १५८ से १६१ तक आ गया है। यह सब कथन निश्चय नय की दृष्टि से । व्यवहारनय की दृष्टि से जिलाना, मारना, सुखी, दुःखी करना आदि कहने में आता है, जो वास्तविक नहीं है ।
इस श्लोक में तथा अन्यत्र जिसे 'बुद्धि' शब्द से, १०वें आदि श्लोकों में 'परिणाम' शब्द से और कहीं 'भाव' तथा 'मति' शब्दों से उल्लेखित किया है, उसी के लिये समयसार में अध्यवसान, विज्ञान, व्यवसाय और चिन्ता शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । समयसार बन्धाधिकार की गाथा २७१ में सभी को एक ही अर्थ का वाचक बतलाया है ।
कर्ताबुद्धि मिथ्या है
-
कोऽपि कस्यापि कर्तास्ति नोपकारापकारयोः ।
उपकुर्वेऽपकुर्वेऽहं मिथ्येति क्रियते मतिः ।। १६२ ।।
अन्वय :- कः अपि कस्य अपि उपकार - अपकारयोः कर्ता न अस्ति । अहं ( कस्यापि ) उपकुर्वे, अपकुर्वे इति (या) मति: क्रियते (सा) मिथ्या (अस्ति) ।
-
सरलार्थ : - कोई भी द्रव्य अन्य किसी भी द्रव्य का उपकार तथा अपकार करनेवाला नहीं है । व्यावहारिक जीवन में मैं दूसरों का कल्याण / अच्छा करता हूँ अथवा मैं अकल्याण/बुरा करता हूँ; यह मान्यता मिथ्या / खोटी है।
-
भावार्थ जीवादि छहों द्रव्यों में धर्मादि चार द्रव्य अमूर्तिक एवं नित्य शुद्ध परिणमन करनेवाले होने से उनमें कुछ विकार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सिद्ध जीव पूर्ण शुद्ध रीति से परिणत हो गये हैं, वे मात्र ज्ञाता होने से उनको कोई कर्तृत्व का विकल्प ही नहीं होता । पुद्गल जडस्वभावी होने से उनमें करने-कराने सम्बन्धी भावों की चर्चा ही व्यर्थ है । जो वस्तु-स्वभाव के यथार्थ ज्ञाता बनकर मोक्षमार्गी हो गये हैं, उनको समझाने अथवा समझने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए मात्र मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से जो अन्यथा श्रद्धा रखते हैं, उनको ही यहाँ आचार्य समझा रहे हैं ।
लौकिक जीवन में दूसरे का उपकार अथवा अपकार करने की जो मान्यता देखी / जानी जाती
[C:/PM65/smarakpm65 / annaji/yogsar prabhat.p65/118]