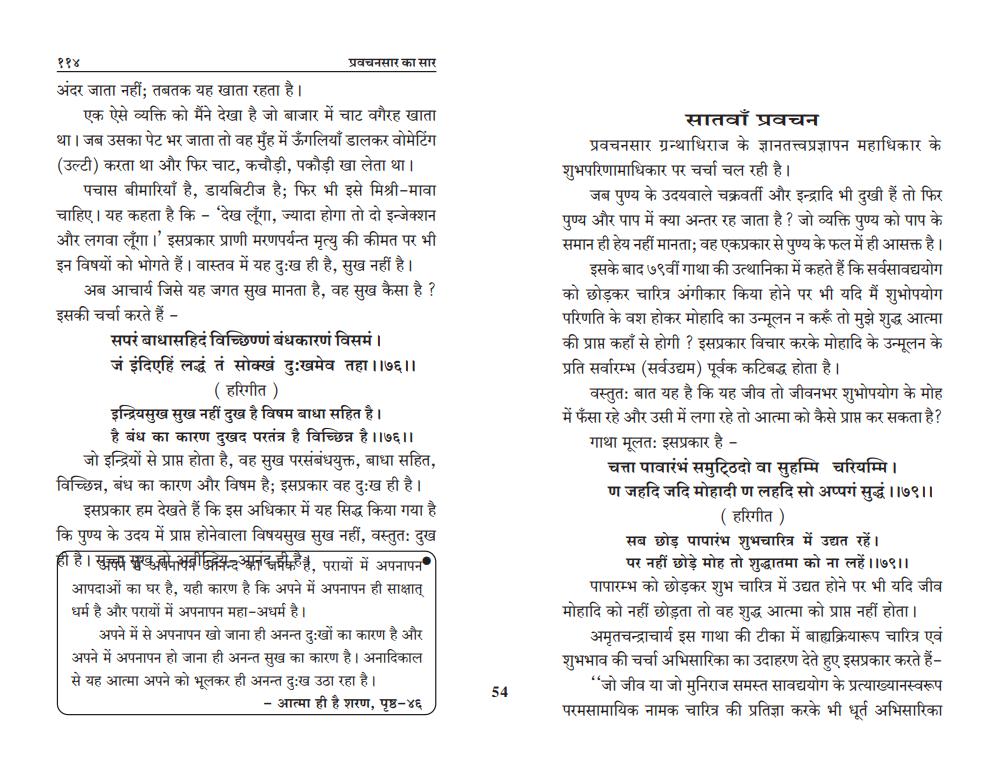________________
११४
अंदर जाता नहीं; तबतक यह खाता रहता है।
एक ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है जो बाजार में चाट वगैरह खाता था। जब उसका पेट भर जाता तो वह मुँह में ऊँगलियाँ डालकर वोमेटिंग (उल्टी) करता था और फिर चाट, कचौड़ी, पकौड़ी खा लेता था।
प्रवचनसार का सार
पचास बीमारियाँ है, डायबिटीज है; फिर भी इसे मिश्री - मावा चाहिए। यह कहता है कि- 'देख लूँगा, ज्यादा होगा तो दो इन्जेक्शन और लगवा लूंगा।' इसप्रकार प्राणी मरणपर्यन्त मृत्यु की कीमत पर भी इन विषयों को भोगते हैं। वास्तव में यह दुःख ही है, सुख नहीं है।
अब आचार्य जिसे यह जगत सुख मानता है, वह सुख कैसा है ? इसकी चर्चा करते हैं -
सपरं बाधासहिदं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं । जं इंदिएहिं लद्धं तं सोक्खं दुःखमेव तहा । ७६ ।। ( हरिगीत )
इन्द्रियसुख सुख नहीं दुख है विषम बाधा सहित है ।
है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है ।। ७६ ।। जो इन्द्रियों से प्राप्त होता है, वह सुख परसंबंधयुक्त, बाधा सहित, विच्छिन्न, बंध का कारण और विषम है; इसप्रकार वह दुःख ही है।
इसप्रकार हम देखते हैं कि इस अधिकार में यह सिद्ध किया गया है कि पुण्य के उदय में प्राप्त होनेवाला विषयसुख सुख नहीं, वस्तुतः दुख ही है। सुत्दा खोजीदि आनंद है है, परायों में अपनापन आपदाओं का घर है, यही कारण है कि अपने में अपनापन ही साक्षात् धर्म है और परायों में अपनापन महा-अधर्म है।
अपने में से अपनापन खो जाना ही अनन्त दुःखों का कारण है और अपने में अपनापन हो जाना ही अनन्त सुख का कारण है। अनादिकाल से यह आत्मा अपने को भूलकर ही अनन्त दुःख उठा रहा है।
- आत्मा ही है शरण, पृष्ठ ४६
54
सातवाँ प्रवचन
प्रवचनसार ग्रन्थाधिराज के ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापन महाधिकार के शुभपरिणामाधिकार पर चर्चा चल रही है।
जब पुण्य के उदयवाले चक्रवर्ती और इन्द्रादि भी दुखी हैं तो फिर पुण्य और पाप में क्या अन्तर रह जाता है ? जो व्यक्ति पुण्य को पाप के समान ही हेय नहीं मानता; वह एकप्रकार से पुण्य के फल में ही आसक्त है।
इसके बाद ७९वीं गाथा की उत्थानिका में कहते हैं कि सर्वसावद्ययोग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी यदि मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोहादि का उन्मूलन न करूँ तो मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्त कहाँ से होगी ? इसप्रकार विचार करके मोहादि के उन्मूलन के प्रति सर्वारम्भ (सर्वउद्यम) पूर्वक कटिबद्ध होता है।
वस्तुत: बात यह है कि यह जीव तो जीवनभर शुभोपयोग के मोह में फँसा रहे और उसी में लगा रहे तो आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? गाथा मूलतः इसप्रकार है -
चत्ता पावारंभं समुट्ठिदो वा सुहम्मि चरियम्मि । जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पगं सुद्धं । । ७९ ।। ( हरिगीत )
सब छोड़ पापारंभ शुभचारित्र में उद्यत रहें ।
पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धातमा को ना लहें ।। ७९ ।। पापारम्भ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता ।
अमृतचन्द्राचार्य इस गाथा की टीका में बाह्यक्रियारूप चारित्र एवं शुभभाव की चर्चा अभिसारिका का उदाहरण देते हुए इसप्रकार करते हैं"जो जीव या जो मुनिराज समस्त सावद्ययोग के प्रत्याख्यानस्वरूप परमसामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका