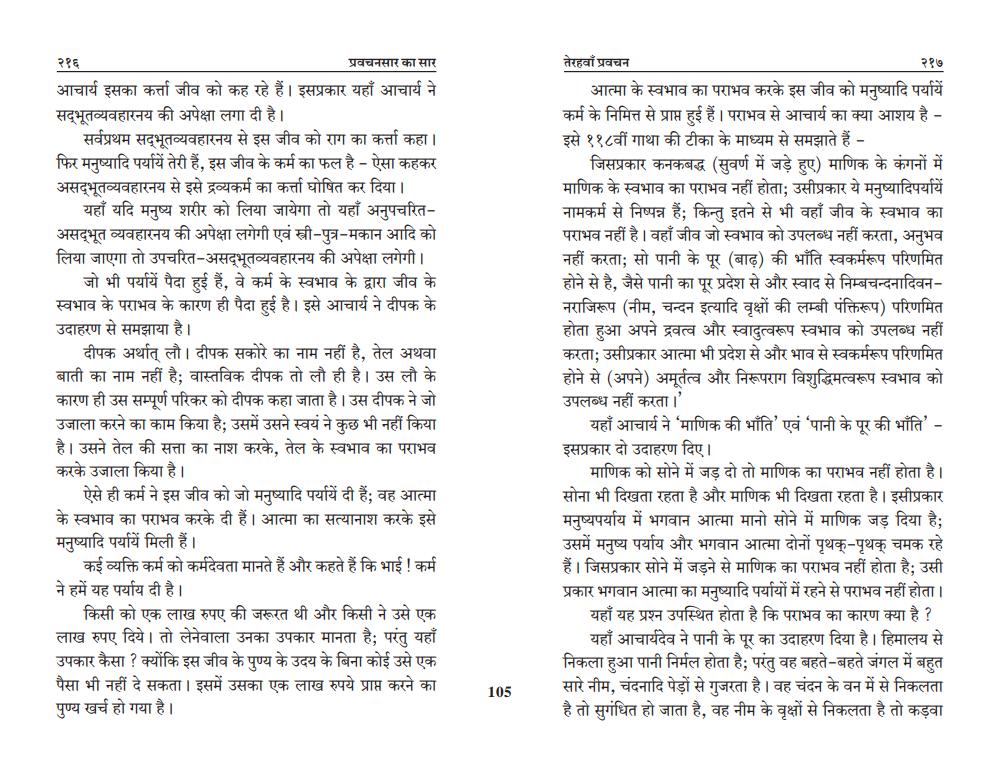________________
२१६
प्रवचनसार का सार
आचार्य इसका कर्त्ता जीव को कह रहे हैं। इसप्रकार यहाँ आचार्य ने सद्भूतव्यवहारनय की अपेक्षा लगा दी है।
सर्वप्रथम सद्भूतव्यवहारनय से इस जीव को राग का कर्त्ता कहा। फिर मनुष्यादि पर्यायें तेरी हैं, इस जीव के कर्म का फल है - ऐसा कहकर असद्भूतव्यवहारनय से इसे द्रव्यकर्म का कर्त्ता घोषित कर दिया।
यहाँ यदि मनुष्य शरीर को लिया जायेगा तो यहाँ अनुपचरितअसद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा लगेगी एवं स्त्री-पुत्र - मकान आदि को लिया जाएगा तो उपचरित - असद्भूतव्यवहारनय की अपेक्षा लगेगी।
जो भी पर्यायें पैदा हुई हैं, वे कर्म के स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव के पराभव के कारण ही पैदा हुई है। इसे आचार्य ने दीपक के उदाहरण से समझाया है।
दीपक अर्थात् लौ । दीपक सकोरे का नाम नहीं है, तेल अथवा बाती का नाम नहीं है; वास्तविक दीपक तो लौ ही है। उस लौ के कारण ही उस सम्पूर्ण परिकर को दीपक कहा जाता है। उस दीपक ने जो उजाला करने का काम किया है; उसमें उसने स्वयं ने कुछ भी नहीं किया है। उसने तेल की सत्ता का नाश करके, तेल के स्वभाव का पराभव करके उजाला किया है।
ऐसे ही कर्म ने इस जीव को जो मनुष्यादि पर्यायें दी हैं; वह आत्मा के स्वभाव का पराभव करके दी हैं। आत्मा का सत्यानाश करके इसे मनुष्यादि पर्यायें मिली हैं।
कई व्यक्ति कर्म को कर्मदेवता मानते हैं और कहते हैं कि भाई ! कर्म ने हमें यह पर्याय दी है।
किसी को एक लाख रुपए की जरूरत थी और किसी ने उसे एक लाख रुपए दिये । तो लेनेवाला उनका उपकार मानता है; परंतु यहाँ उपकार कैसा ? क्योंकि इस जीव के पुण्य के उदय के बिना कोई उसे एक पैसा भी नहीं दे सकता। इसमें उसका एक लाख रुपये प्राप्त करने का पुण्य खर्च हो गया है।
105
तेरहवाँ प्रवचन
२१७
आत्मा के स्वभाव का पराभव करके इस जीव को मनुष्यादि पर्यायें कर्म के निमित्त से प्राप्त हुई हैं। पराभव से आचार्य का क्या आशय है। इसे ११८वीं गाथा की टीका के माध्यम से समझाते हैं -
जिसप्रकार कनकबद्ध (सुवर्ण में जड़े हुए) माणिक के कंगनों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता; उसीप्रकार ये मनुष्यादिपर्यायें नामकर्म से निष्पन्न हैं; किन्तु इतने से भी वहाँ जीव के स्वभाव का पराभव नहीं है। वहाँ जीव जो स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, अनुभव नहीं करता; सो पानी के पूर (बाढ़) की भाँति स्वकर्मरूप परिणमित होने से है, जैसे पानी का पूर प्रदेश से और स्वाद से निम्बचन्दनादिवननराजिरूप (नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षों की लम्बी पंक्तिरूप) परिणमित होता हुआ अपने द्रवत्व और स्वादुत्वरूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता; उसीप्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्मरूप परिणमित होने से (अपने) अमूर्तत्व और निरूपराग विशुद्धिमत्वरूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता ।'
यहाँ आचार्य ने 'माणिक की भाँति' एवं 'पानी के पूर की भाँति' - इसप्रकार दो उदाहरण दिए ।
माणिक को सोने में जड़ दो तो माणिक का पराभव नहीं होता है। सोना भी दिखता रहता है और माणिक भी दिखता रहता है। इसीप्रकार मनुष्यपर्याय में भगवान आत्मा मानो सोने में माणिक जड़ दिया है; उसमें मनुष्य पर्याय और भगवान आत्मा दोनों पृथक्-पृथक् चमक रहे हैं। जिसप्रकार सोने में जड़ने से माणिक का पराभव नहीं होता है; उसी प्रकार भगवान आत्मा का मनुष्यादि पर्यायों में रहने से पराभव नहीं होता।
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पराभव का कारण क्या है ? यहाँ आचार्यदेव ने पानी के पूर का उदाहरण दिया है। हिमालय से निकला हुआ पानी निर्मल होता है; परंतु वह बहते - बहते जंगल में बहुत सारे नीम, चंदनादि पेड़ों से गुजरता है। वह चंदन के वन में से निकलता है तो सुगंधित हो जाता है, वह नीम के वृक्षों से निकलता है तो कड़वा