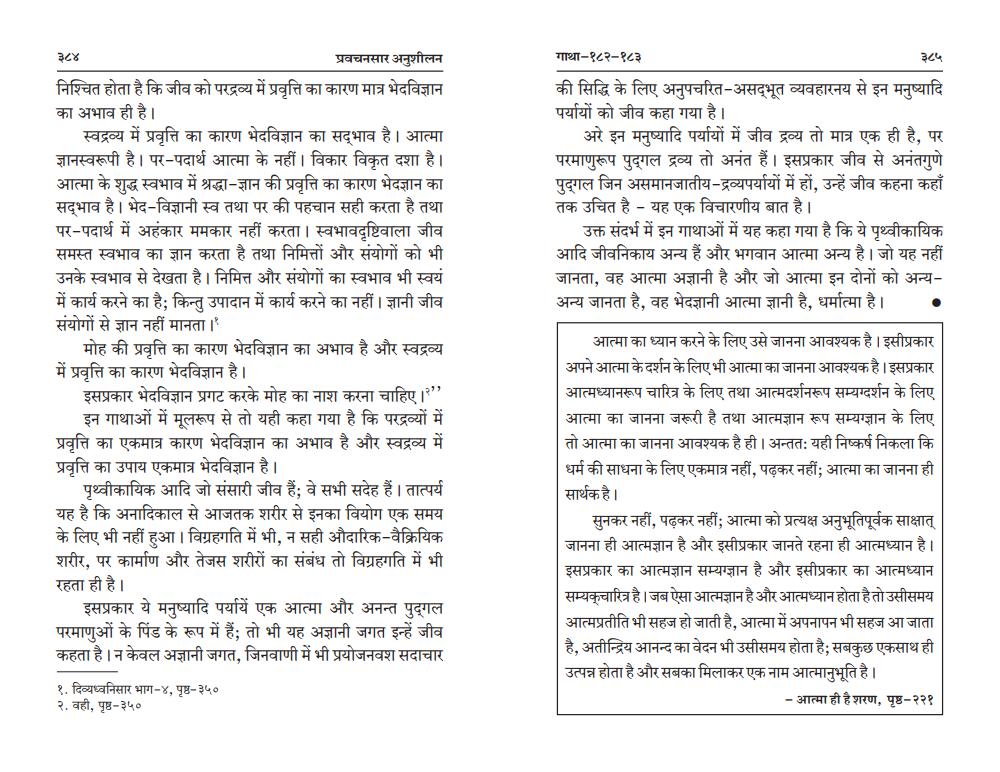________________
गाथा-१८२-१८३
३८५ की सिद्धि के लिए अनुपचरित-असद्भूत व्यवहारनय से इन मनुष्यादि पर्यायों को जीव कहा गया है।
अरे इन मनुष्यादि पर्यायों में जीव द्रव्य तो मात्र एक ही है, पर परमाणुरूप पुद्गल द्रव्य तो अनंत हैं। इसप्रकार जीव से अनंतगुणे पुद्गल जिन असमानजातीय-द्रव्यपर्यायों में हों, उन्हें जीव कहना कहाँ तक उचित है - यह एक विचारणीय बात है।
उक्त संदर्भ में इन गाथाओं में यह कहा गया है कि ये पृथ्वीकायिक आदि जीवनिकाय अन्य हैं और भगवान आत्मा अन्य है। जो यह नहीं जानता, वह आत्मा अज्ञानी है और जो आत्मा इन दोनों को अन्यअन्य जानता है, वह भेदज्ञानी आत्मा ज्ञानी है, धर्मात्मा है।
३८४
प्रवचनसार अनुशीलन निश्चित होता है कि जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण मात्र भेदविज्ञान का अभाव ही है।
स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेदविज्ञान का सद्भाव है। आत्मा ज्ञानस्वरूपी है। पर-पदार्थ आत्मा के नहीं। विकार विकृत दशा है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव में श्रद्धा-ज्ञान की प्रवृत्ति का कारण भेदज्ञान का सद्भाव है। भेद-विज्ञानी स्व तथा पर की पहचान सही करता है तथा पर-पदार्थ में अहंकार ममकार नहीं करता। स्वभावदृष्टिवाला जीव समस्त स्वभाव का ज्ञान करता है तथा निमित्तों और संयोगों को भी उनके स्वभाव से देखता है। निमित्त और संयोगों का स्वभाव भी स्वयं में कार्य करने का है; किन्तु उपादान में कार्य करने का नहीं। ज्ञानी जीव संयोगों से ज्ञान नहीं मानता।
मोह की प्रवृत्ति का कारण भेदविज्ञान का अभाव है और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेदविज्ञान है।
इसप्रकार भेदविज्ञान प्रगट करके मोह का नाश करना चाहिए।"
इन गाथाओं में मूलरूप से तो यही कहा गया है कि परद्रव्यों में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण भेदविज्ञान का अभाव है और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का उपाय एकमात्र भेदविज्ञान है।
पृथ्वीकायिक आदि जो संसारी जीव हैं; वे सभी सदेह हैं। तात्पर्य यह है कि अनादिकाल से आजतक शरीर से इनका वियोग एक समय के लिए भी नहीं हुआ। विग्रहगति में भी, न सही औदारिक-वैक्रियिक शरीर, पर कार्माण और तेजस शरीरों का संबंध तो विग्रहगति में भी रहता ही है।
इसप्रकार ये मनुष्यादि पर्यायें एक आत्मा और अनन्त पुद्गल परमाणुओं के पिंड के रूप में हैं; तो भी यह अज्ञानी जगत इन्हें जीव कहता है। न केवल अज्ञानी जगत, जिनवाणी में भी प्रयोजनवश सदाचार
आत्मा का ध्यान करने के लिए उसे जानना आवश्यक है। इसीप्रकार अपने आत्मा के दर्शन के लिए भी आत्मा का जानना आवश्यक है। इसप्रकार आत्मध्यानरूप चारित्र के लिए तथा आत्मदर्शनरूप सम्यग्दर्शन के लिए आत्मा का जानना जरूरी है तथा आत्मज्ञान रूप सम्यग्ज्ञान के लिए तो आत्मा का जानना आवश्यक है ही। अन्तत: यही निष्कर्ष निकला कि धर्म की साधना के लिए एकमात्र नहीं, पढ़कर नहीं; आत्मा का जानना ही सार्थक है। ___ सुनकर नहीं, पढ़कर नहीं; आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूतिपूर्वक साक्षात् जानना ही आत्मज्ञान है और इसीप्रकार जानते रहना ही आत्मध्यान है। इसप्रकार का आत्मज्ञान सम्यग्ज्ञान है और इसीप्रकार का आत्मध्यान सम्यक्चारित्र है। जब ऐसा आत्मज्ञान है और आत्मध्यान होता है तो उसीसमय आत्मप्रतीति भी सहज हो जाती है, आत्मा में अपनापन भी सहज आ जाता है, अतीन्द्रिय आनन्द का वेदन भी उसीसमय होता है; सबकुछ एकसाथ ही उत्पन्न होता है और सबका मिलाकर एक नाम आत्मानुभूति है।
- आत्मा ही है शरण, पृष्ठ-२२१
१. दिव्यध्वनिसार भाग-४, पृष्ठ-३५० २. वही, पृष्ठ-३५०