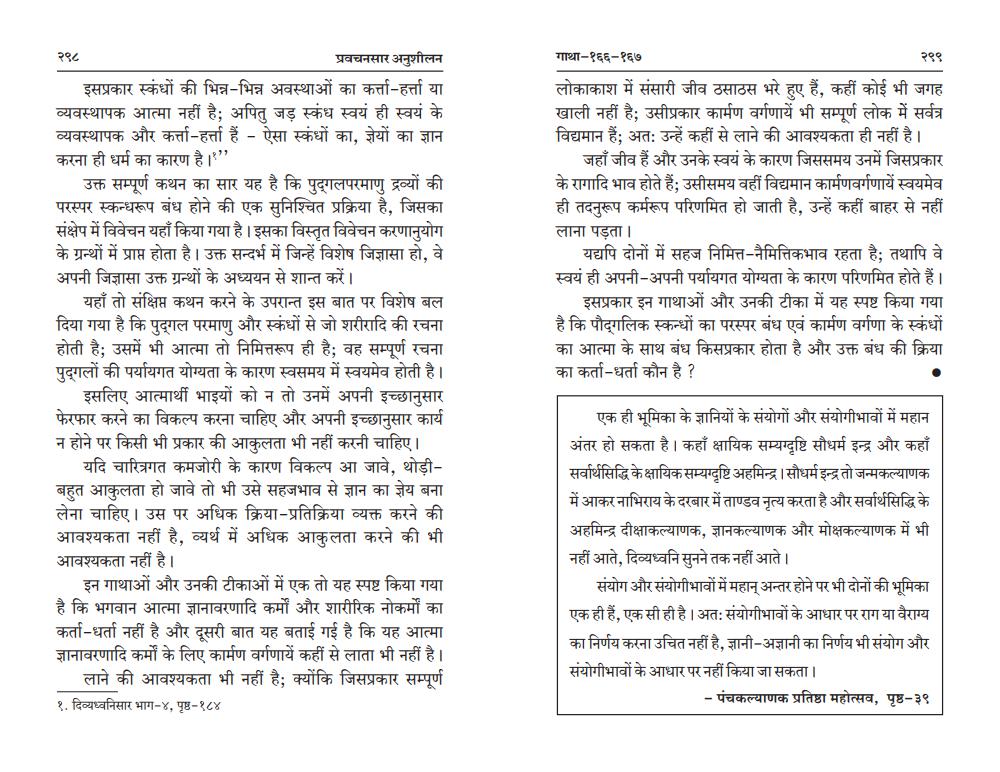________________
प्रवचनसार अनुशीलन इसप्रकार स्कंधों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का कर्त्ता हर्त्ता या व्यवस्थापक आत्मा नहीं है; अपितु जड़ स्कंध स्वयं ही स्वयं के व्यवस्थापक और कर्त्ता हर्त्ता हैं - ऐसा स्कंधों का, ज्ञेयों का ज्ञान करना ही धर्म का कारण है।"
उक्त सम्पूर्ण कथन का सार यह है कि पुद्गलपरमाणु द्रव्यों की परस्पर स्कन्धरूप बंध होने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, जिसका संक्षेप में विवेचन यहाँ किया गया है। इसका विस्तृत विवेचन करणानुयोग के ग्रन्थों में प्राप्त होता है। उक्त सन्दर्भ में जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो, वे अपनी जिज्ञासा उक्त ग्रन्थों के अध्ययन से शान्त करें ।
२९८
यहाँ तो संक्षिप्त कथन करने के उपरान्त इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पुद्गल परमाणु और स्कंधों से जो शरीरादि की रचना होती है; उसमें भी आत्मा तो निमित्तरूप ही है; वह सम्पूर्ण रचना पुद्गलों की पर्यायगत योग्यता के कारण स्वसमय में स्वयमेव होती है।
इसलिए आत्मार्थी भाइयों को न तो उनमें अपनी इच्छानुसार फेरफार करने का विकल्प करना चाहिए और अपनी इच्छानुसार कार्य न होने पर किसी भी प्रकार की आकुलता भी नहीं करनी चाहिए।
यदि चारित्रगत कमजोरी के कारण विकल्प आ जावे, थोड़ीबहुत आकुलता हो जावे तो भी उसे सहजभाव से ज्ञान का ज्ञेय बना लेना चाहिए। उस पर अधिक क्रिया-प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ में अधिक आकुलता करने की भी आवश्यकता नहीं है।
इन गाथाओं और उनकी टीकाओं में एक तो यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों और शारीरिक नोकर्मों का कर्ता-धर्ता नहीं है और दूसरी बात यह बताई गई है कि यह आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों के लिए कार्मण वर्गणायें कहीं से लाता भी नहीं है। लाने की आवश्यकता भी नहीं है; क्योंकि जिसप्रकार सम्पूर्ण १. दिव्यध्वनिसार भाग-४, पृष्ठ- १८४
गाथा - १६६-१६७
२९९
लोकाकाश में संसारी जीव ठसाठस भरे हुए हैं, कहीं कोई भी जगह खाली नहीं है; उसीप्रकार कार्मण वर्गणायें भी सम्पूर्ण लोक में सर्वत्र विद्यमान हैं; अत: उन्हें कहीं से लाने की आवश्यकता ही नहीं है।
जहाँ जीव हैं और उनके स्वयं के कारण जिससमय उनमें जिसप्रकार के रागादि भाव होते हैं; उसीसमय वहीं विद्यमान कार्मणवर्गणायें स्वयमेव ही तदनुरूप कर्मरूप परिणमित हो जाती है, उन्हें कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता ।
यद्यपि दोनों में सहज निमित्त नैमित्तिकभाव रहता है; तथापि वे स्वयं ही अपनी-अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण परिणमित होते हैं।
इसप्रकार इन गाथाओं और उनकी टीका में यह स्पष्ट किया गया है कि पौद्गलिक स्कन्धों का परस्पर बंध एवं कार्मण वर्गणा के स्कंधों का आत्मा के साथ बंध किसप्रकार होता है और उक्त बंध की क्रिया का कर्ता-धर्ता कौन है ?
एक ही भूमिका के ज्ञानियों के संयोगों और संयोगीभावों में महान अंतर हो सकता है । कहाँ क्षायिक सम्यग्दृष्टि सौधर्म इन्द्र और कहाँ सर्वार्थसिद्धि के क्षायिक सम्यग्दृष्टि अहमिन्द्र । सौधर्म इन्द्र तो जन्मकल्याणक में आकर नाभिराय के दरबार में ताण्डव नृत्य करता है और सर्वार्थसिद्धि के अहमिन्द्र दीक्षाकल्याणक, ज्ञानकल्याणक और मोक्षकल्याणक में भी नहीं आते, दिव्यध्वनि सुनने तक नहीं आते।
संयोग और संयोगी भावों में महान् अन्तर होने पर भी दोनों की भूमिका एक ही हैं, एक सी ही है। अतः संयोगीभावों के आधार पर राग या वैराग्य का निर्णय करना उचित नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय भी संयोग और संयोगीभावों के आधार पर नहीं किया जा सकता।
- पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, पृष्ठ-३९