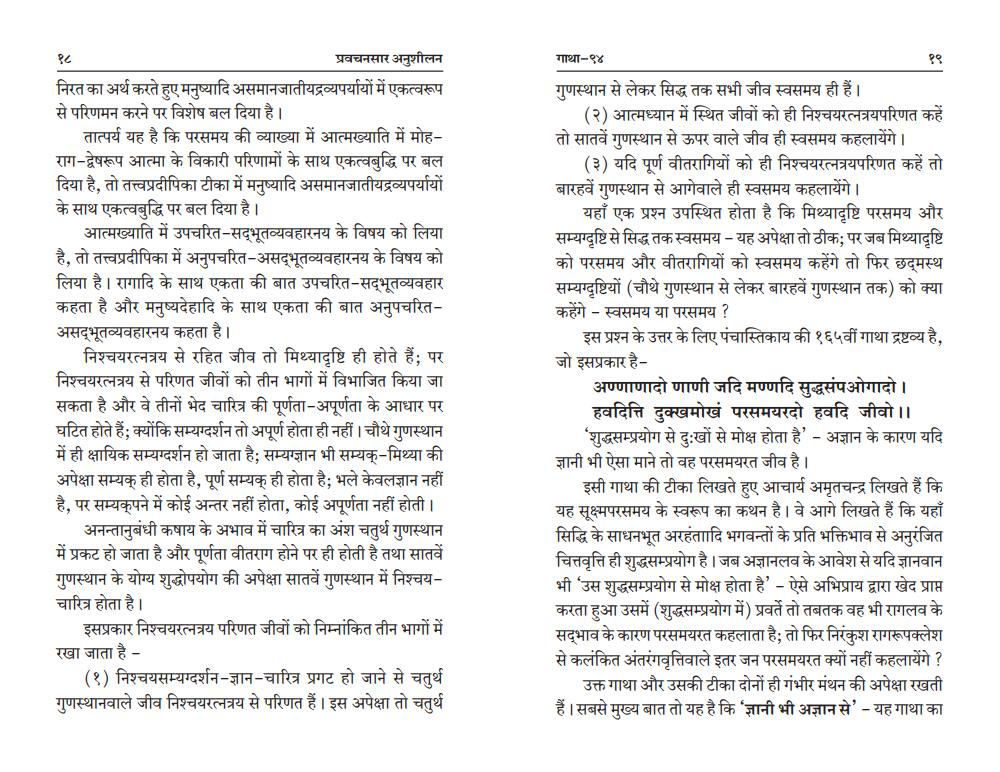________________
गाथा-९४
प्रवचनसार अनुशीलन निरत का अर्थ करते हुए मनुष्यादि असमानजातीयद्रव्यपर्यायों में एकत्वरूप से परिणमन करने पर विशेष बल दिया है।
तात्पर्य यह है कि परसमय की व्याख्या में आत्मख्याति में मोहराग-द्वेषरूप आत्मा के विकारी परिणामों के साथ एकत्वबुद्धि पर बल दिया है, तो तत्त्वप्रदीपिका टीका में मनुष्यादि असमानजातीयद्रव्यपर्यायों के साथ एकत्वबुद्धि पर बल दिया है।
आत्मख्याति में उपचरित-सद्भूतव्यवहारनय के विषय को लिया है, तो तत्त्वप्रदीपिका में अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय के विषय को लिया है। रागादि के साथ एकता की बात उपचरित-सद्भूतव्यवहार कहता है और मनुष्यदेहादि के साथ एकता की बात अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय कहता है।
निश्चयरत्नत्रय से रहित जीव तो मिथ्यादृष्टि ही होते हैं; पर निश्चयरत्नत्रय से परिणत जीवों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है और वे तीनों भेद चारित्र की पूर्णता-अपूर्णता के आधार पर घटित होते हैं; क्योंकि सम्यग्दर्शन तो अपूर्ण होता ही नहीं । चौथे गुणस्थान में ही क्षायिक सम्यग्दर्शन हो जाता है; सम्यग्ज्ञान भी सम्यक्-मिथ्या की अपेक्षा सम्यक् ही होता है, पूर्ण सम्यक् ही होता है; भले केवलज्ञान नहीं है, पर सम्यक्पने में कोई अन्तर नहीं होता, कोई अपूर्णता नहीं होती।
अनन्तानुबंधी कषाय के अभाव में चारित्र का अंश चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट हो जाता है और पूर्णता वीतराग होने पर ही होती है तथा सातवें गुणस्थान के योग्य शुद्धोपयोग की अपेक्षा सातवें गुणस्थान में निश्चयचारित्र होता है।
इसप्रकार निश्चयरत्नत्रय परिणत जीवों को निम्नांकित तीन भागों में रखा जाता है -
(१) निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र प्रगट हो जाने से चतुर्थ गुणस्थानवाले जीव निश्चयरत्नत्रय से परिणत हैं। इस अपेक्षा तो चतुर्थ
गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक सभी जीव स्वसमय ही हैं।
(२) आत्मध्यान में स्थित जीवों को ही निश्चयरत्नत्रयपरिणत कहें तो सातवें गुणस्थान से ऊपर वाले जीव ही स्वसमय कहलायेंगे।
(३) यदि पूर्ण वीतरागियों को ही निश्चयरत्नत्रयपरिणत कहें तो बारहवें गुणस्थान से आगेवाले ही स्वसमय कहलायेंगे। __यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मिथ्यादृष्टि परसमय और सम्यग्दृष्टि से सिद्ध तक स्वसमय - यह अपेक्षा तो ठीक; पर जब मिथ्यादृष्टि को परसमय और वीतरागियों को स्वसमय कहेंगे तो फिर छद्मस्थ सम्यग्दृष्टियों (चौथे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक) को क्या कहेंगे - स्वसमय या परसमय ?
इस प्रश्न के उत्तर के लिए पंचास्तिकाय की १६५वीं गाथा द्रष्टव्य है, जो इसप्रकार है
अण्णाणादो णाणी जदि मण्णदि सुद्धसंपओगादो। हवदित्ति दुक्खमोखं परसमयरदो हवदि जीवो ।। 'शुद्धसम्प्रयोग से दु:खों से मोक्ष होता है' - अज्ञान के कारण यदि ज्ञानी भी ऐसा माने तो वह परसमयरत जीव है।
इसी गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं कि यह सूक्ष्मपरसमय के स्वरूप का कथन है। वे आगे लिखते हैं कि यहाँ सिद्धि के साधनभूत अरहतादि भगवन्तों के प्रति भक्तिभाव से अनुरंजित चित्तवृत्ति ही शुद्धसम्प्रयोग है । जब अज्ञानलव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी 'उस शुद्धसम्प्रयोग से मोक्ष होता है' - ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें (शुद्धसम्प्रयोग में) प्रवर्ते तो तबतक वह भी रागलव के सद्भाव के कारण परसमयरत कहलाता है; तो फिर निरंकुश रागरूपक्लेश से कलंकित अंतरंगवृत्तिवाले इतर जन परसमयरत क्यों नहीं कहलायेंगे?
उक्त गाथा और उसकी टीका दोनों ही गंभीर मंथन की अपेक्षा रखती हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि 'ज्ञानी भी अज्ञान से' - यह गाथा का