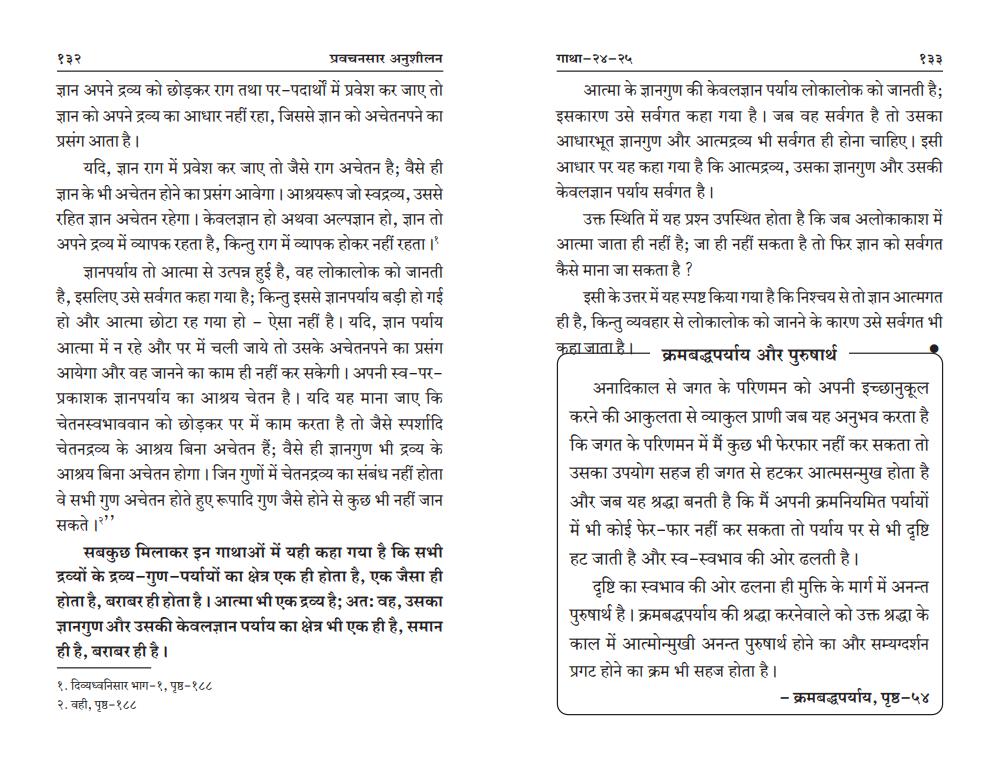________________
१३२
प्रवचनसार अनुशीलन ज्ञान अपने द्रव्य को छोड़कर राग तथा पर-पदार्थों में प्रवेश कर जाए तो ज्ञान को अपने द्रव्य का आधार नहीं रहा, जिससे ज्ञान को अचेतनपने का प्रसंग आता है।
यदि, ज्ञान राग में प्रवेश कर जाए तो जैसे राग अचेतन है; वैसे ही ज्ञान के भी अचेतन होने का प्रसंग आवेगा। आश्रयरूप जो स्वद्रव्य, उससे रहित ज्ञान अचेतन रहेगा। केवलज्ञान हो अथवा अल्पज्ञान हो, ज्ञान तो अपने द्रव्य में व्यापक रहता है, किन्तु राग में व्यापक होकर नहीं रहता। ज्ञानपर्याय तो आत्मा से उत्पन्न हुई है, वह लोकालोक को जानती है, इसलिए उसे सर्वगत कहा गया है; किन्तु इससे ज्ञानपर्याय बड़ी हो गई हो और आत्मा छोटा रह गया हो ऐसा नहीं है। यदि, ज्ञान पर्याय आत्मा में न रहे और पर में चली जाये तो उसके अचेतनपने का प्रसंग आयेगा और वह जानने का काम ही नहीं कर सकेगी। अपनी स्व-परप्रकाशक ज्ञानपर्याय का आश्रय चेतन है । यदि यह माना जाए कि चेतनस्वभाववान को छोड़कर पर में काम करता है तो जैसे स्पर्शादि चेतनद्रव्य के आश्रय बिना अचेतन हैं; वैसे ही ज्ञानगुण भी द्रव्य के आश्रय बिना अचेतन होगा । जिन गुणों में चेतनद्रव्य का संबंध नहीं होता वे सभी गुण अचेतन होते हुए रूपादि गुण जैसे होने से कुछ भी नहीं जान सकते। २"
सबकुछ मिलाकर इन गाथाओं में यही कहा गया है कि सभी द्रव्यों के द्रव्य-गुण- पर्यायों का क्षेत्र एक ही होता है, एक जैसा ही होता है, बराबर ही होता है। आत्मा भी एक द्रव्य है; अत: वह, उसका ज्ञानगुण और उसकी केवलज्ञान पर्याय का क्षेत्र भी एक ही है, समान ही है, बराबर ही है ।
१. दिव्यध्वनिसार भाग-१, पृष्ठ १८८
२. वही, पृष्ठ- १८८
गाथा - २४-२५
१३३
आत्मा के ज्ञानगुण की केवलज्ञान पर्याय लोकालोक को जानती है; इसकारण उसे सर्वगत कहा गया है। जब वह सर्वगत है तो उसका आधारभूत ज्ञानगुण और आत्मद्रव्य भी सर्वगत ही होना चाहिए। इसी आधार पर यह कहा गया है कि आत्मद्रव्य, उसका ज्ञानगुण और उसकी केवलज्ञान पर्याय सर्वगत है ।
उक्त स्थिति में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अलोकाकाश में आत्मा जाता ही नहीं है; जा ही नहीं सकता है तो फिर ज्ञान को सर्वगत कैसे माना जा सकता है ?
इसी के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि निश्चय से तो ज्ञान आत्मगत ही है, किन्तु व्यवहार से लोकालोक को जानने के कारण उसे सर्वगत भी कहा जाता है । क्रमबद्धपर्याय और पुरुषार्थ
अनादिकाल से जगत के परिणमन को अपनी इच्छानुकूल करने की आकुलता से व्याकुल प्राणी जब यह अनुभव करता है कि जगत के परिणमन में मैं कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता तो उसका उपयोग सहज ही जगत से हटकर आत्मसन्मुख होता है और जब यह श्रद्धा बनती है कि मैं अपनी क्रमनियमित पर्यायों में भी कोई फेर-फार नहीं कर सकता तो पर्याय पर से भी दृष्टि हट जाती है और स्व-स्वभाव की ओर ढलती है।
दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनन्त पुरुषार्थ है। क्रमबद्धपर्याय की श्रद्धा करनेवाले को उक्त श्रद्धा के काल में आत्मोन्मुखी अनन्त पुरुषार्थ होने का और सम्यग्दर्शन प्रगट होने का क्रम भी सहज होता है।
- क्रमबद्धपर्याय, पृष्ठ-५४