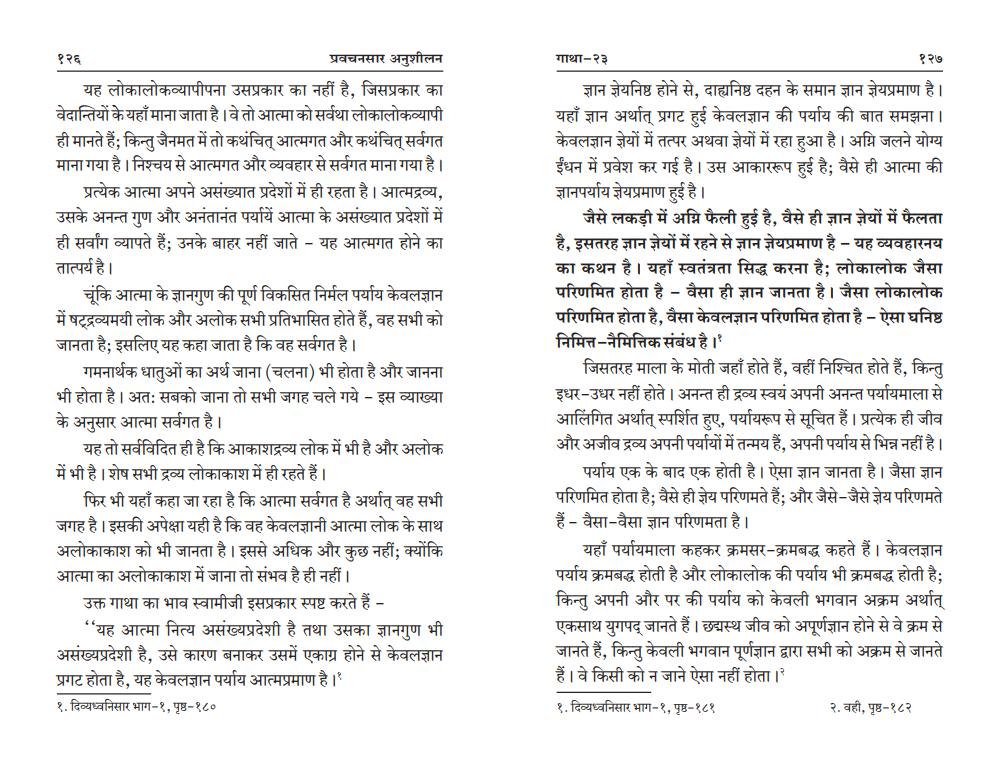________________
१२६
प्रवचनसार अनुशीलन यह लोकालोकव्यापीपना उसप्रकार का नहीं है, जिसप्रकार का वेदान्तियों के यहाँ माना जाता है। वे तो आत्मा को सर्वथा लोकालोकव्यापी ही मानते हैं; किन्तु जैनमत में तो कथंचित् आत्मगत और कथंचित् सर्वगत माना गया है। निश्चय से आत्मगत और व्यवहार से सर्वगत माना गया है।
प्रत्येक आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। आत्मद्रव्य, उसके अनन्त गुण और अनंतानंत पर्यायें आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में ही सर्वांग व्यापते हैं; उनके बाहर नहीं जाते - यह आत्मगत होने का तात्पर्य है।
चूंकि आत्मा के ज्ञानगुण की पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय केवलज्ञान में षद्रव्यमयी लोक और अलोक सभी प्रतिभासित होते हैं, वह सभी को जानता है; इसलिए यह कहा जाता है कि वह सर्वगत है।
गमनार्थक धातुओं का अर्थ जाना (चलना) भी होता है और जानना भी होता है। अत: सबको जाना तो सभी जगह चले गये - इस व्याख्या के अनुसार आत्मा सर्वगत है।
यह तो सर्वविदित ही है कि आकाशद्रव्य लोक में भी है और अलोक में भी है। शेष सभी द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं।
फिर भी यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मा सर्वगत है अर्थात् वह सभी जगह है। इसकी अपेक्षा यही है कि वह केवलज्ञानी आत्मा लोक के साथ अलोकाकाश को भी जानता है। इससे अधिक और कुछ नहीं; क्योंकि आत्मा का अलोकाकाश में जाना तो संभव है ही नहीं।
उक्त गाथा का भाव स्वामीजी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -
"यह आत्मा नित्य असंख्यप्रदेशी है तथा उसका ज्ञानगुण भी असंख्यप्रदेशी है, उसे कारण बनाकर उसमें एकाग्र होने से केवलज्ञान प्रगट होता है, यह केवलज्ञान पर्याय आत्मप्रमाण है। १. दिव्यध्वनिसार भाग-१, पृष्ठ-१८०
गाथा-२३
१२७ ज्ञान ज्ञेयनिष्ठ होने से, दाह्यनिष्ठ दहन के समान ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है। यहाँ ज्ञान अर्थात् प्रगट हुई केवलज्ञान की पर्याय की बात समझना । केवलज्ञान ज्ञेयों में तत्पर अथवा ज्ञेयों में रहा हुआ है। अग्नि जलने योग्य ईंधन में प्रवेश कर गई है। उस आकाररूप हुई है; वैसे ही आत्मा की ज्ञानपर्याय ज्ञेयप्रमाण हुई है।
जैसे लकड़ी में अग्नि फैली हुई है, वैसे ही ज्ञान ज्ञेयों में फैलता है, इसतरह ज्ञान ज्ञेयों में रहने से ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है - यह व्यवहारनय का कथन है। यहाँ स्वतंत्रता सिद्ध करना है; लोकालोक जैसा परिणमित होता है - वैसा ही ज्ञान जानता है। जैसा लोकालोक परिणमित होता है, वैसा केवलज्ञान परिणमित होता है - ऐसा घनिष्ठ निमित्त-नैमित्तिक संबंध है।
जिसतरह माला के मोती जहाँ होते हैं, वहीं निश्चित होते हैं, किन्तु इधर-उधर नहीं होते। अनन्त ही द्रव्य स्वयं अपनी अनन्त पर्यायमाला से आलिंगित अर्थात् स्पर्शित हुए, पर्यायरूप से सूचित हैं। प्रत्येक ही जीव और अजीव द्रव्य अपनी पर्यायों में तन्मय हैं, अपनी पर्याय से भिन्न नहीं है। ___पर्याय एक के बाद एक होती है। ऐसा ज्ञान जानता है। जैसा ज्ञान परिणमित होता है; वैसे ही ज्ञेय परिणमते हैं; और जैसे-जैसे ज्ञेय परिणमते हैं - वैसा-वैसा ज्ञान परिणमता है।
यहाँ पर्यायमाला कहकर क्रमसर-क्रमबद्ध कहते हैं। केवलज्ञान पर्याय क्रमबद्ध होती है और लोकालोक की पर्याय भी क्रमबद्ध होती है; किन्तु अपनी और पर की पर्याय को केवली भगवान अक्रम अर्थात् एकसाथ युगपद् जानते हैं । छद्मस्थ जीव को अपूर्णज्ञान होने से वे क्रम से जानते हैं, किन्तु केवली भगवान पूर्णज्ञान द्वारा सभी को अक्रम से जानते हैं। वे किसी को न जाने ऐसा नहीं होता। १. दिव्यध्वनिसार भाग-१, पृष्ठ-१८१
२. वही, पृष्ठ-१८२