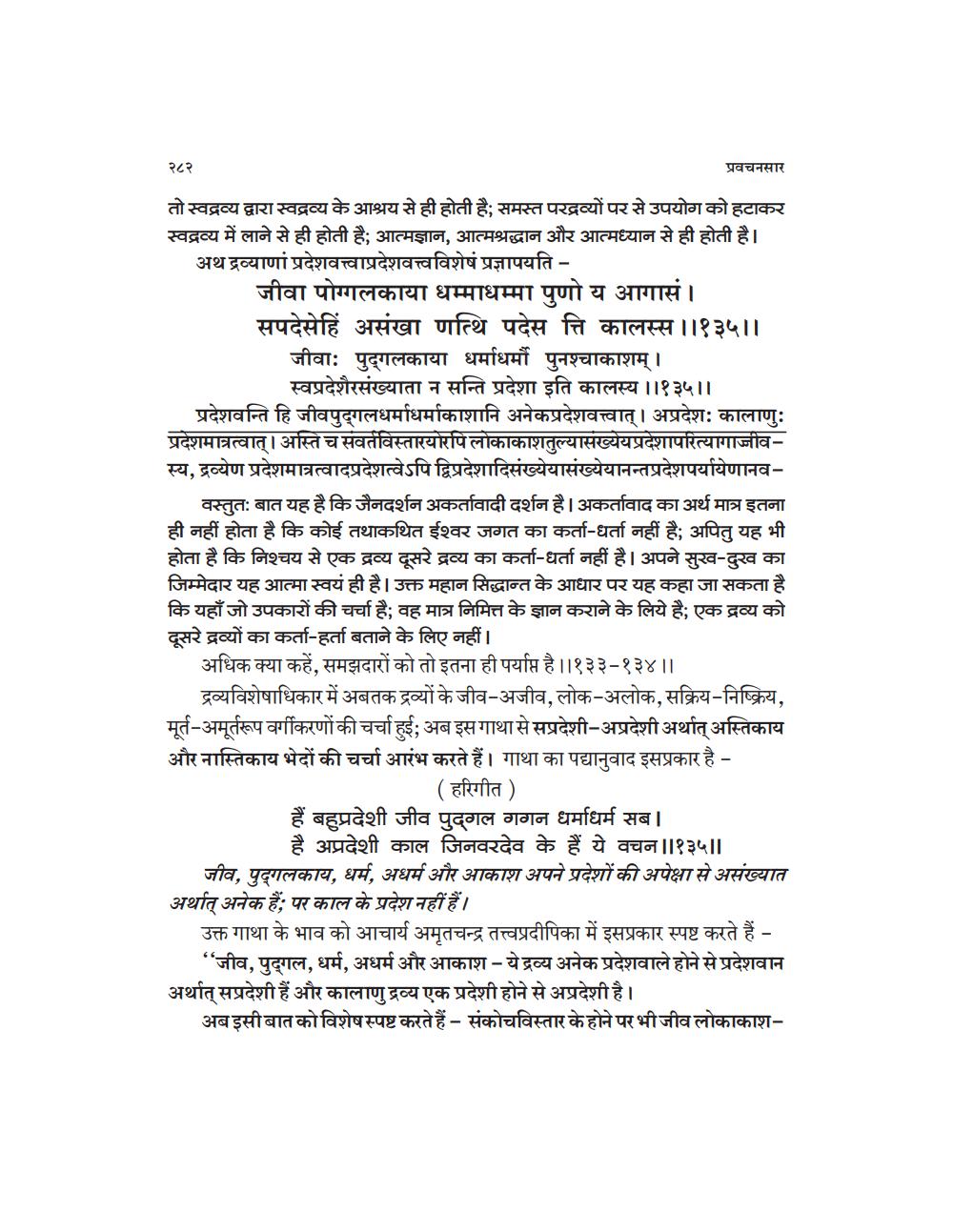________________
२८२
प्रवचनसार
तो स्वद्रव्य द्वारा स्वद्रव्य के आश्रय से ही होती है; समस्त परद्रव्यों पर से उपयोग को हटाकर स्वद्रव्य में लाने से ही होती है; आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धान और आत्मध्यान से ही होती है। अथ द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वविशेषं प्रज्ञापयति -
जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा पुणो य आगासं ।
सपदेसेहिं असंखा णत्थि पदेस त्ति कालस्स ।। १३५ ।। जीवा: पुद्गलकाया धर्माधर्मौ पुनश्चाकाशम् । स्वप्रदेशैरसंख्याता न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ।। १३५ ।।
प्रदेशवन्ति हि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशानि अनेकप्रदेशवत्त्वात् । अप्रदेश: कालाणुः प्रदेशमात्रत्वात् । अस्ति च संवर्तविस्तारयोरपि लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशापरित्यागाज्जीवस्य, द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वेऽपि द्विप्रदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायेणानव
वस्तुत: बात यह है कि जैनदर्शन अकर्तावादी दर्शन है। अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना नहीं होता है कि कोई तथाकथित ईश्वर जगत का कर्ता-धर्ता नहीं है, अपितु यह भी होता है कि निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता-धर्ता नहीं है । अपने सुख-दुख का जिम्मेदार यह आत्मा स्वयं ही है। उक्त महान सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ जो उपकारों की चर्चा है; वह मात्र निमित्त के ज्ञान कराने के लिये है; एक द्रव्य को दूसरे द्रव्यों का कर्ता हर्ता बताने के लिए नहीं ।
अधिक क्या कहें, समझदारों को तो इतना ही पर्याप्त है ।। १३३-१३४ ।।
द्रव्यविशेषाधिकार में अबतक द्रव्यों के जीव-अजीव, लोक- अलोक, सक्रिय-निष्क्रिय, मूर्त-अमूर्तरूप वर्गीकरणों की चर्चा हुई; अब इस गाथा से सप्रदेशी - अप्रदेशी अर्थात् अस्तिकाय और नास्तिकाय भेदों की चर्चा आरंभ करते हैं। गाथा का पद्यानुवाद इसप्रकार है -
( हरिगीत )
हैं बहुप्रदेशी जीव पुद्गल गगन धर्माधर्म सब ।
है अप्रदेशी काल जिनवरदेव के हैं ये वचन || १३५||
जीव, पुद्गलकाय, धर्म, अधर्म और आकाश अपने प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात अर्थात् अनेक हैं; पर काल के प्रदेश नहीं हैं ।
उक्त गाथा के भाव को आचार्य अमृतचन्द्र तत्त्वप्रदीपिका में इसप्रकार स्पष्ट करते
"जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश - ये द्रव्य अनेक प्रदेशवाले होने से प्रदेशवान अर्थात् सप्रदेशी हैं और कालाणु द्रव्य एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है ।
अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं- संकोचविस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश
-