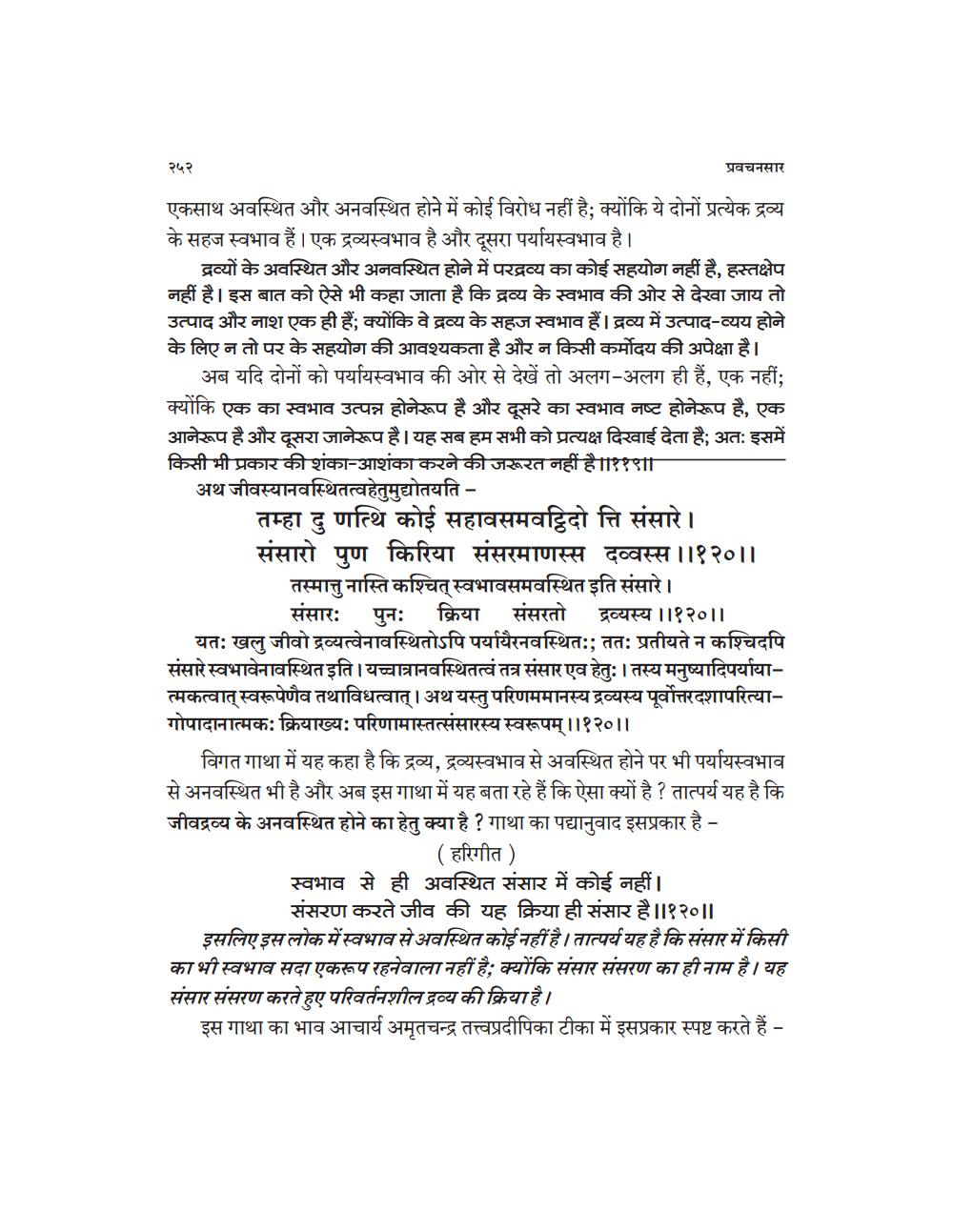________________
२५२
प्रवचनसार
एकसाथ अवस्थित और अनवस्थित होने में कोई विरोध नहीं है; क्योंकि ये दोनों प्रत्येक द्रव्य के सहज स्वभाव हैं। एक द्रव्यस्वभाव है और दूसरा पर्यायस्वभाव है।
द्रव्यों के अवस्थित और अनवस्थित होने में परद्रव्य का कोई सहयोग नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। इस बात को ऐसे भी कहा जाता है कि द्रव्य के स्वभाव की ओर से देखा जाय तो उत्पाद और नाश एक ही हैं; क्योंकि वे द्रव्य के सहज स्वभाव हैं। द्रव्य में उत्पाद-व्यय होने के लिए न तो पर के सहयोग की आवश्यकता है और न किसी कर्मोदय की अपेक्षा है।
अब यदि दोनों को पर्यायस्वभाव की ओर से देखें तो अलग-अलग ही हैं, एक नहीं; क्योंकि एक का स्वभाव उत्पन्न होनेरूप है और दूसरे का स्वभाव नष्ट होनेरूप है, एक आनेरूप है और दूसरा जानेरूप है। यह सब हम सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देता है; अत: इसमें किसी भी प्रकार कीशंका-आशंका करने की जरूरत नहीं है। १९|| अथ जीवस्यानवस्थितत्वहेतुमुद्योतयति -
तम्हा दु णत्थि कोई सहावसमवट्ठिदो त्ति संसारे। संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दव्वस्स ।।१२०॥
तस्मात्तु नास्ति कश्चित् स्वभावसमवस्थित इति संसारे।
संसारः पुनः क्रिया संसरतो द्रव्यस्य ।।१२०।। यतः खलु जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पर्यायैरनवस्थितः; ततः प्रतीयते न कश्चिदपि संसारे स्वभावेनावस्थित इति । यच्चानानवस्थितत्वंतत्र संसार एव हेतुः । तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्वात् स्वरूपेणैव तथाविधत्वात् । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरित्यागोपादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामास्तत्संसारस्य स्वरूपम् ।।१२०।।
विगत गाथा में यह कहा है कि द्रव्य, द्रव्यस्वभाव से अवस्थित होने पर भी पर्यायस्वभाव से अनवस्थित भी है और अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है ? तात्पर्य यह है कि जीवद्रव्य के अनवस्थित होने का हेतु क्या है ? गाथा का पद्यानुवाद इसप्रकार है -
(हरिगीत) स्वभाव से ही अवस्थित संसार में कोई नहीं।
संसरण करते जीव की यह क्रिया ही संसार है।।१२०|| इसलिए इस लोक में स्वभाव से अवस्थित कोई नहीं है। तात्पर्य यह है कि संसार में किसी का भी स्वभाव सदा एकरूप रहनेवाला नहीं है; क्योंकि संसार संसरण का ही नाम है। यह संसार संसरण करते हुए परिवर्तनशील द्रव्य की क्रिया है।
इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचन्द्र तत्त्वप्रदीपिका टीका में इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -