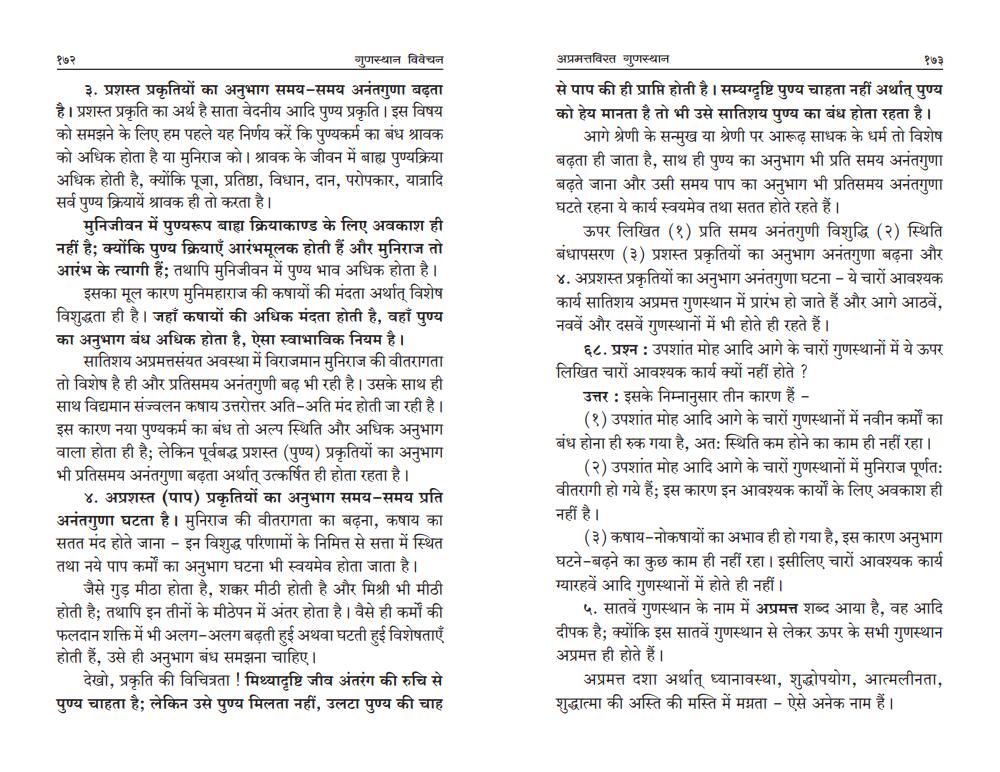________________
गुणस्थान विवेचन ३. प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय-समय अनंतगुणा बढ़ा है । प्रशस्त प्रकृति का अर्थ है साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृति । इस विषय को समझने के लिए हम पहले यह निर्णय करें कि पुण्यकर्म का बंध श्रावक को अधिक होता है या मुनिराज को । श्रावक के जीवन में बाह्य पुण्यक्रिया अधिक होती है, क्योंकि पूजा, प्रतिष्ठा, विधान, दान, परोपकार, यात्रादि सर्व पुण्य क्रियायें श्रावक ही तो करता है।
१७२
मुनिजीवन में पुण्यरूप बाह्य क्रियाकाण्ड के लिए अवकाश नहीं है; क्योंकि पुण्य क्रियाएँ आरंभमूलक होती हैं और मुनिराज तो आरंभ के त्यागी हैं; तथापि मुनिजीवन में पुण्य भाव अधिक होता है।
इसका मूल कारण मुनिमहाराज की कषायों की मंदता अर्थात् विशेष विशुद्धता ही है । जहाँ कषायों की अधिक मंदता होती है, वहाँ पुण्य का अनुभाग बंध अधिक होता है, ऐसा स्वाभाविक नियम है।
सातिशय अप्रमत्तसंयत अवस्था में विराजमान मुनिराज की वीतरागता तो विशेष है ही और प्रतिसमय अनंतगुणी बढ़ भी रही है। उसके साथ ही साथ विद्यमान संज्वलन कषाय उत्तरोत्तर अति-अति मंद होती जा रही है। इस कारण नया पुण्यकर्म का बंध तो अल्प स्थिति और अधिक अनुभाग वाला होता ही है; लेकिन पूर्वबद्ध प्रशस्त (पुण्य) प्रकृतियों का अनुभाग भी प्रतिसमय अनंतगुणा बढ़ता अर्थात् उत्कर्षित ही होता रहता है।
४. अप्रशस्त (पाप) प्रकृतियों का अनुभाग समय-समय प्रति अनंतगुणा घटता है । मुनिराज की वीतरागता का बढ़ना, कषाय का सतत मंद होते जाना इन विशुद्ध परिणामों के निमित्त से सत्ता में स्थित तथा नये पाप कर्मों का अनुभाग घटना भी स्वयमेव होता जाता है।
जैसे गुड़ मीठा होता है, शक्कर मीठी होती है और मिश्री भी मीठी होती है; तथापि इन तीनों के मीठेपन में अंतर होता है। वैसे ही कर्मों की फलदान शक्ति में भी अलग-अलग बढ़ती हुई अथवा घटती हुई विशेषताएँ होती हैं, उसे ही अनुभाग बंध समझना चाहिए।
देखो, प्रकृति की विचित्रता ! मिथ्यादृष्टि जीव अंतरंग की रुचि पुण्य चाहता है; लेकिन उसे पुण्य मिलता नहीं, उलटा पुण्य की चाह
अप्रमत्तविरत गुणस्थान
१७३
से पाप की ही प्राप्ति होती है। सम्यग्दृष्टि पुण्य चाहता नहीं अर्थात् पुण्य को हेय मानता है तो भी उसे सातिशय पुण्य का बंध होता रहता है। श्रेणी के सन्मुख या श्रेणी पर आरूढ़ साधक के धर्म तो विशेष बढ़ता ही जाता है, साथ ही पुण्य का अनुभाग भी प्रति समय अनंतगुणा बढ़ते जाना और उसी समय पाप का अनुभाग भी प्रतिसमय अनंतगुणा घटते रहना ये कार्य स्वयमेव तथा सतत होते रहते हैं।
ऊपर लिखित (१) प्रति समय अनंतगुणी विशुद्धि (२) स्थिति बंधापसरण ( ३ ) प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंतगुणा बढ़ना और ४. अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंतगुणा घटना - ये चारों आवश्यक कार्य सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में प्रारंभ हो जाते हैं और आगे आठवें, नववें और दसवें गुणस्थानों में भी होते ही रहते हैं।
६८. प्रश्न : उपशांत मोह आदि आगे के चारों गुणस्थानों में ये ऊपर लिखित चारों आवश्यक कार्य क्यों नहीं होते ?
उत्तर : इसके निम्नानुसार तीन कारण हैं -
(१) उपशांत मोह आदि आगे के चारों गुणस्थानों में नवीन कर्मों का बंध होना ही रुक गया है, अतः स्थिति कम होने का काम ही नहीं रहा ।
(२) उपशांत मोह आदि आगे के चारों गुणस्थानों में मुनिराज पूर्णतः वीतरागी हो गये हैं; इस कारण इन आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही नहीं है।
(३) कषाय-नोकषायों का अभाव ही हो गया है, इस कारण अनुभाग घटने-बढ़ने का कुछ काम ही नहीं रहा । इसीलिए चारों आवश्यक कार्य ग्यारहवें आदि गुणस्थानों में होते ही नहीं ।
५. सातवें गुणस्थान के नाम में अप्रमत्त शब्द आया है, वह आदि दीपक है; क्योंकि इस सातवें गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थान अप्रमत्त ही होते हैं।
अप्रमत्त दशा अर्थात् ध्यानावस्था, शुद्धोपयोग, आत्मलीनता, शुद्धात्मा की अस्ति की मस्ति में मग्नता ऐसे अनेक नाम हैं।