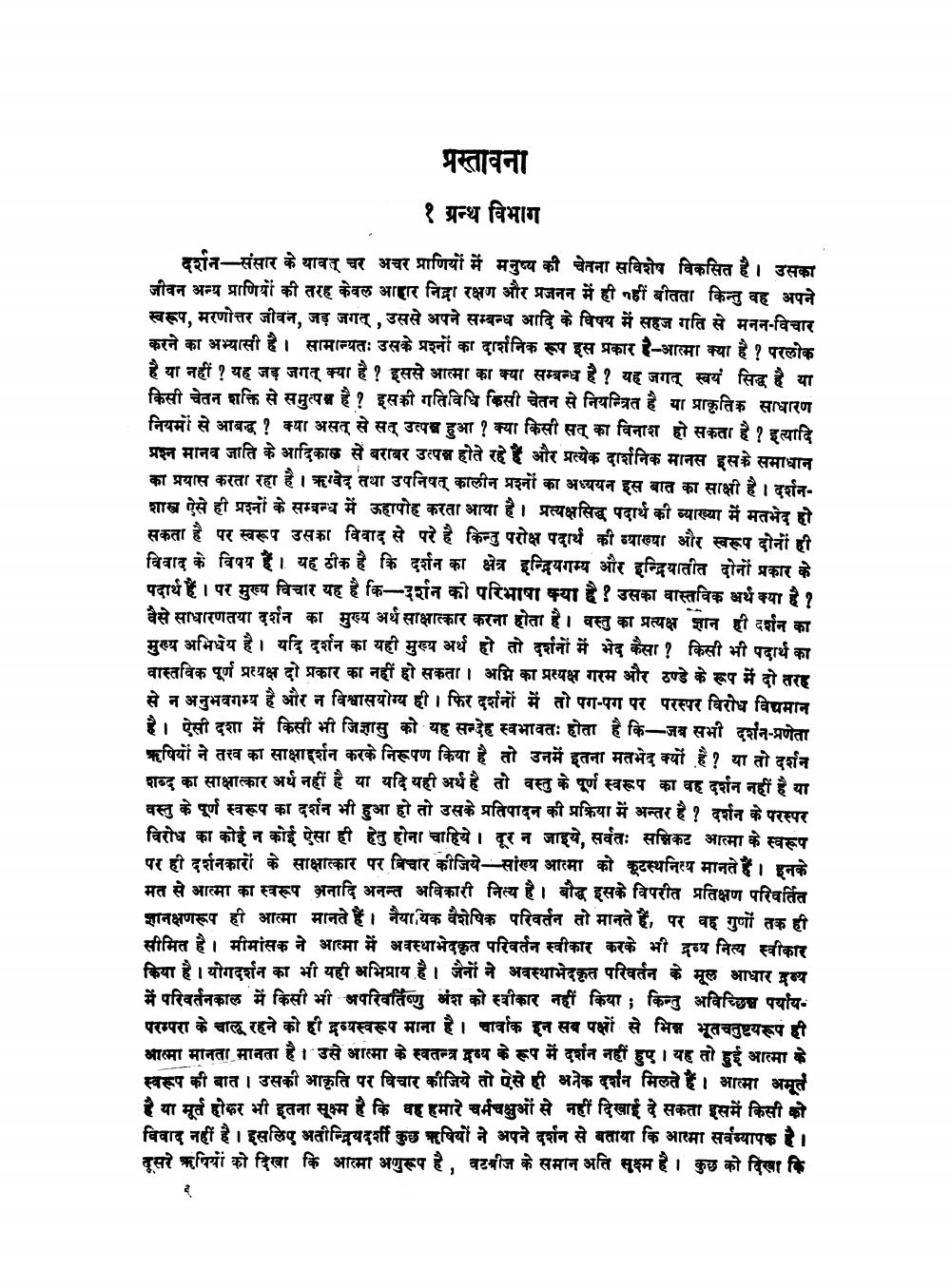________________
प्रस्तावना १ ग्रन्थ विभाग
दर्शन-संसार के यावत् चर अचर प्राणियों में मनुष्य की चेतना सविशेष विकसित है। उसका जीवन अन्य प्राणियों की तरह केवल आहार निद्रा रक्षण और प्रजनन में ही नहीं बीतता किन्तु वह अपने स्वरूप, मरणोत्तर जीवन, जड़ जगत् , उससे अपने सम्बन्ध आदि के विषय में सहज गति से मनन-विचार करने का अभ्यासी है। सामान्यतः उसके प्रश्नों का दार्शनिक रूप इस प्रकार है-आत्मा क्या है ? परलोक है या नहीं ? यह जद जगत् क्या है ? इससे आत्मा का क्या सम्बन्ध है? यह जगत् स्वयं सिद्ध है या किसी चेतन शक्ति से समुत्पन्न है ? इसकी गतिविधि किसी चेतन से नियन्त्रित है या प्राकृतिक साधारण नियमों से आबद्ध ? क्या असत् से सत् उत्पन्न हुआ ? क्या किसी सत् का विनाश हो सकता है? इत्यादि प्रश्न मानव जाति के आदिकाल से बराबर उत्पन्न होते रहे हैं और प्रत्येक दार्शनिक मानस इसके समाधान का प्रयास करता रहा है। ऋग्वेद तथा उपनिषत् कालीन प्रश्नों का अध्ययन इस बात का साक्षी है। दर्शनशास्त्र ऐसे ही प्रश्नों के सम्बन्ध में ऊहापोह करता आया है। प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थ की व्याख्या में मतभेद हो सकता है पर स्वरूप उसका विवाद से परे है किन्तु परोक्ष पदार्थ की व्याख्या और स्वरूप दोनों ही विवाद के विषय हैं। यह ठीक है कि दर्शन का क्षेत्र इन्द्रियगम्य और इन्द्रियातीत दोनों प्रकार के पदार्थ । पर मुख्य विचार यह है कि-दर्शन को परिभाषा क्या है? उसका वास्तविक अर्थ क्या है। वैसे साधारणतया दर्शन का मुख्य अर्थ साक्षात्कार करना होता है। वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान ही दर्शन का मुख्य अभिधेय है। यदि दर्शन का यही मुख्य अर्थ हो तो दर्शनों में भेद कैसा ? किसी भी पदार्थ का वास्तविक पूर्ण प्रत्यक्ष दो प्रकार का नहीं हो सकता। अग्नि का प्रत्यक्ष गरम और ठण्डे के रूप में दो तरह से न अनुभवगम्य है और न विश्वासयोग्य ही। फिर दर्शनों में तो पग-पग पर परस्पर विरोध विद्यमान है। ऐसी दशा में किसी भी जिज्ञासु को यह सन्देह स्वभावतः होता है कि जब सभी दर्शन-प्रणेता ऋषियों ने तत्व का साक्षादर्शन करके निरूपण किया है तो उनमें इतना मतभेद क्यों है? या तो दर्शन शब्द का साक्षात्कार अर्थ नहीं है या यदि यही अर्थ है तो वस्तु के पूर्ण स्वरूप का वह दर्शन नहीं है या वस्तु के पूर्ण स्वरूप का दर्शन भी हुआ हो तो उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया में अन्तर है? दर्शन के परस्पर विरोध का कोई न कोई ऐसा ही हेतु होना चाहिये। दूर न जाइये, सर्वतः सन्निकट आत्मा के स्वरूप पर ही दर्शनकारों के साक्षात्कार पर विचार कीजिये-सांख्य आत्मा को कूटस्थनित्य मानते हैं। इनके मत से आत्मा का स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य है। बौद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवर्तित ज्ञानक्षणरूप ही आत्मा मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक परिवर्तन तो मानते हैं, पर वह गुणों तक ही सीमित है। मीमांसक ने आत्मा में अवस्थाभेदकृत परिवर्तन स्वीकार करके भी द्रव्य नित्य स्वीकार किया है। योगदर्शन का भी यही अभिप्राय है। जैनों ने अवस्थाभेदकृत परिवर्तन के मूल आधार द्रव्य में परिवर्तनकाल में किसी भी अपरिवर्तिष्णु अंश को स्वीकार नहीं किया; किन्तु अविच्छिन्न पर्यायपरम्परा के चालू रहने को ही द्रव्यस्वरूप माना है। चार्वाक इन सब पक्षों से भिन्न भूतचतुष्टयरूप ही आत्मा मानता मानता है। उसे आस्मा के स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में दर्शन नहीं हुए। यह तो हुई आत्मा के स्वरूप की बात । उसकी आकृति पर विचार कीजिये तो ऐसे ही अनेक दर्शन मिलते हैं। आत्मा अमृत है या मूर्त होकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चर्मचक्षुओं से नहीं दिखाई दे सकता इसमें किसी को विवाद नहीं है। इसलिए अतीन्द्रियदर्शी कुछ ऋषियों ने अपने दर्शन से बताया कि आत्मा सर्वव्यापक है। दूसरे ऋषियों को दिखा कि आत्मा अणुरूप है , वटबीज के समान अति सूक्ष्म है। कुछ को दिखा कि