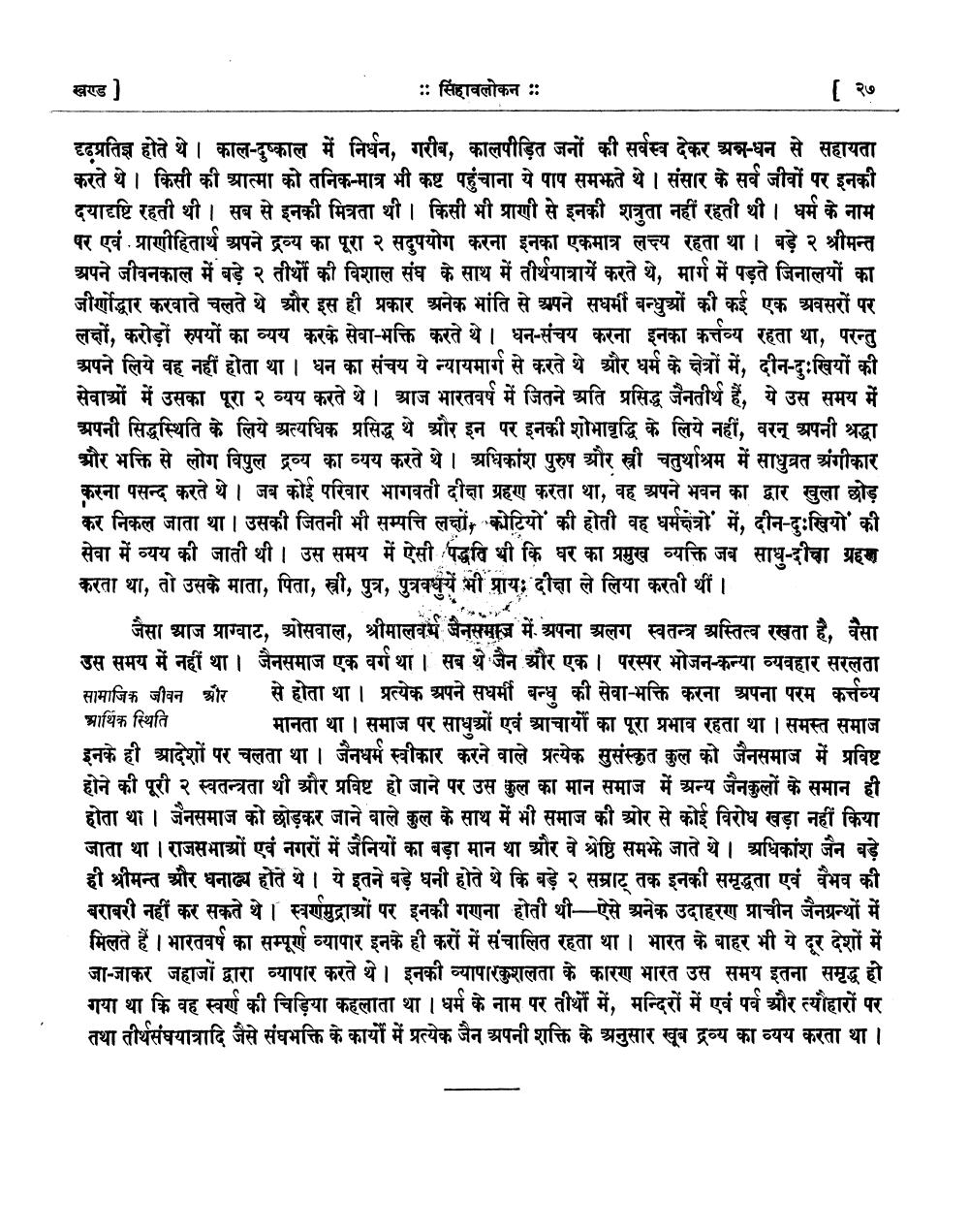________________
खण्ड
:: सिंहावलोकन::
[ २७
दृढ़प्रतिज्ञ होते थे । काल-दुष्काल में निर्धन, गरीब, कालपीड़ित जनों की सर्वस्व देकर अन्न-धन से सहायता करते थे। किसी की आत्मा को तनिक-मात्र भी कष्ट पहुंचाना ये पाप समझते थे । संसार के सर्व जीवों पर इनकी दयादृष्टि रहती थी। सब से इनकी मित्रता थी। किसी भी प्राणी से इनकी शत्रुता नहीं रहती थी। धर्म के नाम पर एवं प्राणीहितार्थ अपने द्रव्य का पूरा २ सदुपयोग करना इनका एकमात्र लक्ष्य रहता था। बड़े २ श्रीमन्त अपने जीवनकाल में बड़े २ तीर्थों की विशाल संघ के साथ में तीर्थयात्रायें करते थे, मार्ग में पड़ते जिनालयों का जीर्णोद्धार करवाते चलते थे और इस ही प्रकार अनेक भांति से अपने सधर्मी बन्धुओं की कई एक अवसरों पर लक्षों, करोड़ों रुपयों का व्यय करके सेवा-भक्ति करते थे। धन-संचय करना इनका कर्तव्य रहता था, परन्तु अपने लिये वह नहीं होता था। धन का संचय ये न्यायमार्ग से करते थे और धर्म के क्षेत्रों में, दीन-दुःखियों की सेवाओं में उसका पूरा २ व्यय करते थे। आज भारतवर्ष में जितने अति प्रसिद्ध जैनतीर्थ हैं, ये उस समय में अपनी सिद्धस्थिति के लिये अत्यधिक प्रसिद्ध थे और इन पर इनकी शोभावृद्धि के लिये नहीं, वरन् अपनी श्रद्धा और भक्ति से लोग विपुल द्रव्य का व्यय करते थे। अधिकांश पुरुष और स्त्री चतुर्थाश्रम में साधुव्रत अंगीकार करना पसन्द करते थे। जब कोई परिवार भागवती दीक्षा ग्रहण करता था, वह अपने भवन का द्वार खुला छोड़ कर निकल जाता था। उसकी जितनी भी सम्पत्ति लक्षोंकोटियों की होती वह धर्मक्षेत्रों में, दीन-दुःखियों की सेवा में व्यय की जाती थी। उस समय में ऐसी पद्धति थी कि घर का प्रमुख व्यक्ति जब साधु-दीचा ग्रहण करता था, तो उसके माता, पिता, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधुयें भी प्रायः दीक्षा ले लिया करती थीं।
जैसा श्राज प्राग्वाट, प्रोसवाल, श्रीमालवर्म जैनसमाज में अपना अलग स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, वैसा उस समय में नहीं था। जैनसमाज एक वर्ग था। सब थे जैन और एक । परस्पर भोजन-कन्या व्यवहार सरलता सामाजिक जीवन और से होता था। प्रत्येक अपने सधर्मी बन्धु की सेवा-भक्ति करना अपना परम कर्तव्य
आर्थिक स्थिति मानता था । समाज पर साधुओं एवं आचार्यों का पूरा प्रभाव रहता था । समस्त समाज इनके ही आदेशों पर चलता था। जैनधर्म स्वीकार करने वाले प्रत्येक सुसंस्कृत कुल को जैनसमाज में प्रविष्ट होने की पूरी २ स्वतन्त्रता थी और प्रविष्ट हो जाने पर उस कुल का मान समाज में अन्य जैनकुलों के समान ही होता था। जैनसमाज को छोड़कर जाने वाले कुल के साथ में भी समाज की ओर से कोई विरोध खड़ा नहीं किया जाता था । राजसभाओं एवं नगरों में जैनियों का बड़ा मान था और वे श्रेष्ठि समझे जाते थे। अधिकांश जैन बड़े ही श्रीमन्त और धनाढ्य होते थे। ये इतने बड़े धनी होते थे कि बड़े २ सम्राट तक इनकी समृद्धता एवं वैभव की बराबरी नहीं कर सकते थे। स्वर्णमुद्राओं पर इनकी गणना होती थी—ऐसे अनेक उदाहरण प्राचीन जैनग्रन्थों में मिलते हैं । भारतवर्ष का सम्पूर्ण व्यापार इनके ही करों में संचालित रहता था। भारत के बाहर भी ये दूर देशों में जा-जाकर जहाजों द्वारा व्यापार करते थे। इनकी व्यापारकुशलता के कारण भारत उस समय इतना समृद्ध हो गया था कि वह स्वर्ण की चिड़िया कहलाता था । धर्म के नाम पर तीर्थों में, मन्दिरों में एवं पर्व और त्यौहारों पर तथा तीर्थसंघयात्रादि जैसे संघभक्ति के कार्यों में प्रत्येक जैन अपनी शक्ति के अनुसार खूब द्रव्य का व्यय करता था।