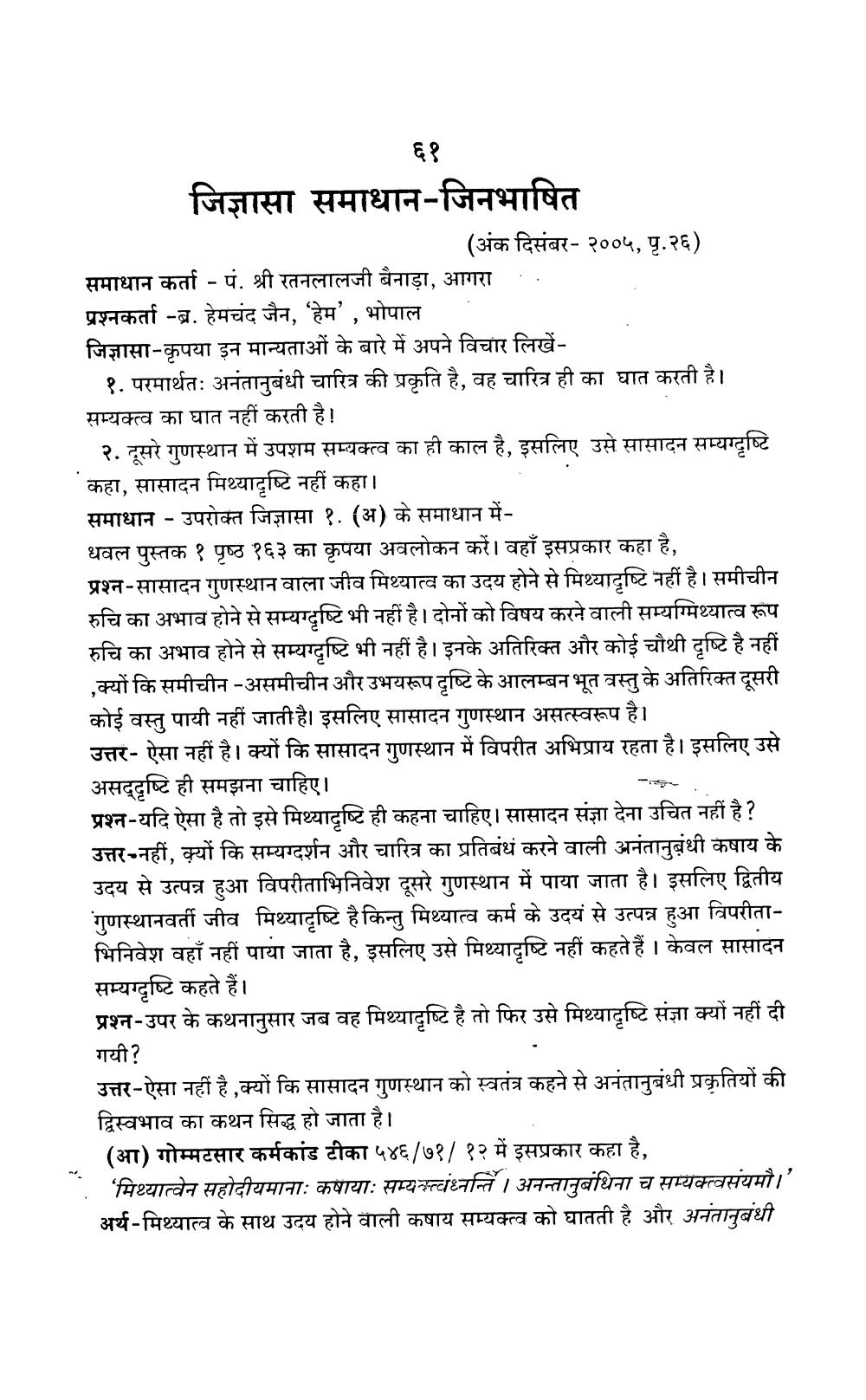________________
जिज्ञासा समाधान-जिनभाषित
(अंक दिसंबर- २००५, पृ.२६) समाधान कर्ता - पं. श्री रतनलालजी बैनाड़ा, आगरा प्रश्नकर्ता -ब्र. हेमचंद जैन, 'हेम' , भोपाल जिज्ञासा-कृपया इन मान्यताओं के बारे में अपने विचार लिखें
१. परमार्थतः अनंतानुबंधी चारित्र की प्रकृति है, वह चारित्र ही का घात करती है। सम्यक्त्व का घात नहीं करती है। २. दूसरे गुणस्थान में उपशम सम्यक्त्व का ही काल है, इसलिए उसे सासादन सम्यग्दृष्टि कहा, सासादन मिथ्यादृष्टि नहीं कहा। समाधान - उपरोक्त जिज्ञासा १. (अ) के समाधान मेंधवल पुस्तक १ पृष्ठ १६३ का कृपया अवलोकन करें। वहाँ इसप्रकार कहा है, प्रश्न-सासादन गुणस्थान वाला जीव मिथ्यात्व का उदय होने से मिथ्यादृष्टि नहीं है। समीचीन रुचि का अभाव होने से सम्यग्दृष्टि भी नहीं है। दोनों को विषय करने वाली सम्यग्मिथ्यात्व रूप रुचि का अभाव होने से सम्यग्दृष्टि भी नहीं है। इनके अतिरिक्त और कोई चौथी दृष्टि है नहीं ,क्यों कि समीचीन -असमीचीन और उभयरूप दृष्टि के आलम्बन भूत वस्तु के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु पायी नहीं जाती है। इसलिए सासादन गुणस्थान असत्स्वरूप है। उत्तर- ऐसा नहीं है। क्यों कि सासादन गुणस्थान में विपरीत अभिप्राय रहता है। इसलिए उसे असदृष्टि ही समझना चाहिए। प्रश्न-यदि ऐसा है तो इसे मिथ्यादृष्टि ही कहना चाहिए। सासादन संज्ञा देना उचित नहीं है? उत्तर-नहीं, क्यों कि सम्यग्दर्शन और चारित्र का प्रतिबंध करने वाली अनंतानुबंधी कषाय के उदय से उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश दूसरे गुणस्थान में पाया जाता है। इसलिए द्वितीय गुणस्थानवी जीव मिथ्यादृष्टि है किन्तु मिथ्यात्व कर्म के उदयं से उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश वहाँ नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे मिथ्यादृष्टि नहीं कहते हैं । केवल सासादन सम्यग्दृष्टि कहते हैं। प्रश्न-उपर के कथनानुसार जब वह मिथ्यादृष्टि है तो फिर उसे मिथ्यादृष्टि संज्ञा क्यों नहीं दी गयी? उत्तर-ऐसा नहीं है ,क्यों कि सासादन गुणस्थान को स्वतंत्र कहने से अनंतानुबंधी प्रकृतियों की द्विस्वभाव का कथन सिद्ध हो जाता है।
(आ) गोम्मटसार कर्मकांड टीका ५४६/७१/ १२ में इसप्रकार कहा है, .. 'मिथ्यात्वेन सहोदीयमानाः कषायाः सम्यस्त्वंध्नन्ति । अनन्तानुबंधिना च सम्यक्त्वसंयमौ।'
अर्थ-मिथ्यात्व के साथ उदय होने वाली कषाय सम्यक्त्व को घातती है और अनंतानुबंधी