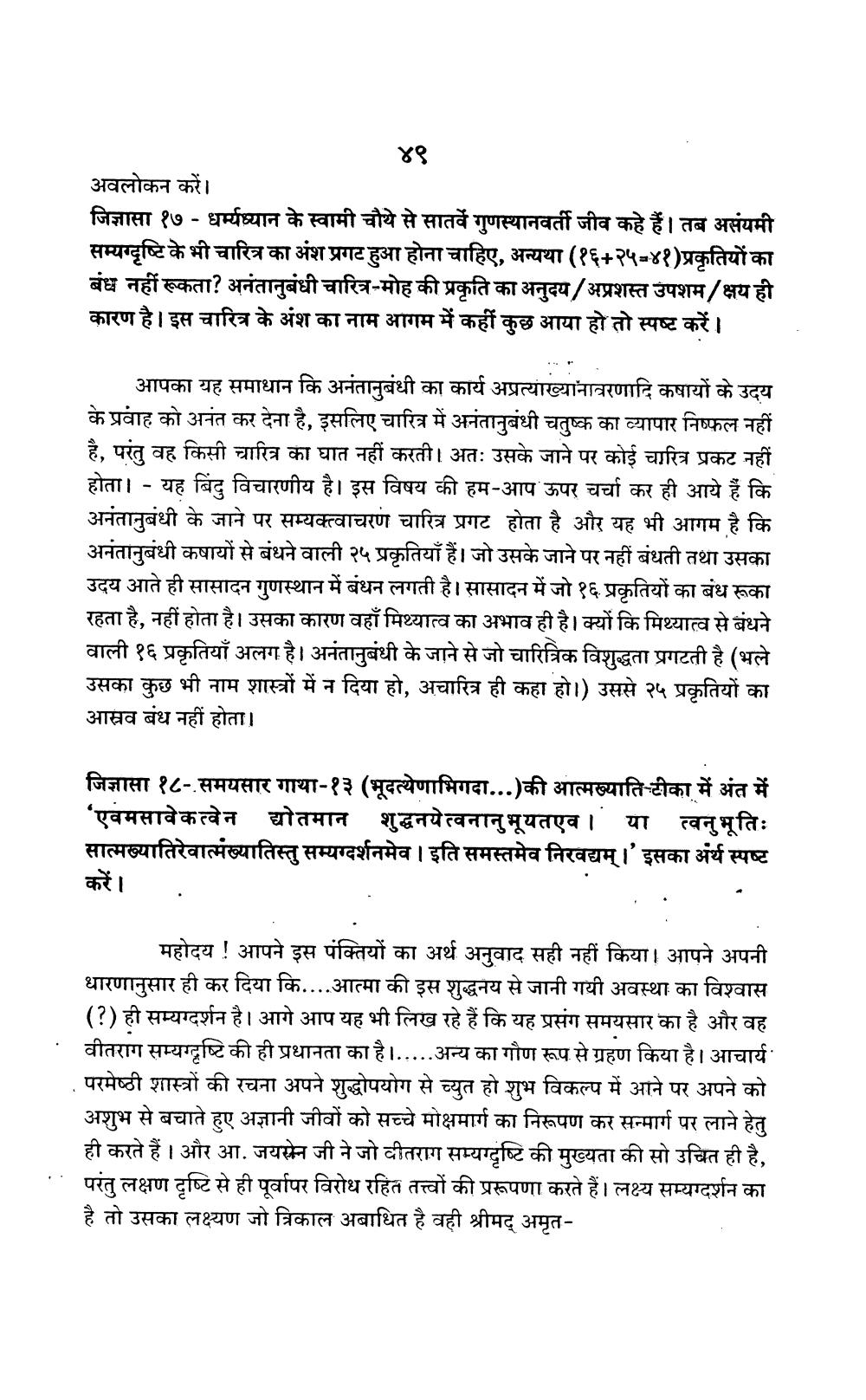________________
अवलोकन करें। जिज्ञासा १७ - धर्म्यध्यान के स्वामी चौथे से सातवें गुणस्थानवी जीव कहे हैं। तब असंयमी सम्यग्दृष्टि के भी चारित्र का अंश प्रगट हुआ होना चाहिए, अन्यथा (१६+२५-४१)प्रकृतियों का बंध नहीं रूकता? अनंतानुबंधी चारित्र-मोह की प्रकृति का अनुदय/अप्रशस्त उपशम/क्षय ही कारण है। इस चारित्र के अंश का नाम आगम में कहीं कुछ आया हो तो स्पष्ट करें।
आपका यह समाधान कि अनंतानुबंधी का कार्य अप्रत्याख्यानावरणादि कषायों के उदय के प्रवाह को अनंत कर देना है, इसलिए चारित्र में अनंतानुबंधी चतुष्क का व्यापार निष्फल नहीं है, परंतु वह किसी चारित्र का घात नहीं करती। अतः उसके जाने पर कोई चारित्र प्रकट नहीं होता। - यह बिंदु विचारणीय है। इस विषय की हम-आप ऊपर चर्चा कर ही आये हैं कि अनंतानुबंधी के जाने पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रगट होता है और यह भी आगम है कि अनंतानुबंधी कषायों से बंधने वाली २५ प्रकृतियाँ हैं। जो उसके जाने पर नहीं बंधती तथा उसका उदय आते ही सासादन गुणस्थान में बंधन लगती है। सासादन में जो १६ प्रकृतियों का बंध रूका रहता है, नहीं होता है। उसका कारण वहाँ मिथ्यात्व का अभाव ही है। क्यों कि मिथ्यात्व से बंधने वाली १६ प्रकृतियाँ अलग है। अनंतानुबंधी के जाने से जो चारित्रिक विशुद्धता प्रगटती है (भले उसका कुछ भी नाम शास्त्रों में न दिया हो, अचारित्र ही कहा हो।) उससे २५ प्रकृतियों का आस्रव बंध नहीं होता।
जिज्ञासा १८- समयसार गाथा-१३ (भूदत्येणाभिगदा...)की आत्मख्याति-टीका में अंत में 'एवमसावेकत्वेन द्योतमान शुद्धनयेत्वनानुभूयतएव । या त्वनुभूतिः सात्मख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेव । इति समस्तमेव निरवद्यम्।' इसका अर्थ स्पष्ट
करें।
महोदय ! आपने इस पंक्तियों का अर्थ अनुवाद सही नहीं किया। आपने अपनी धारणानुसार ही कर दिया कि....आत्मा की इस शुद्धनय से जानी गयी अवस्था का विश्वास (?) ही सम्यग्दर्शन है। आगे आप यह भी लिख रहे हैं कि यह प्रसंग समयसार का है और वह वीतराग सम्यग्दृष्टि की ही प्रधानता का है।.....अन्य का गौण रूप से ग्रहण किया है। आचार्य परमेष्ठी शास्त्रों की रचना अपने शुद्धोपयोग से च्युत हो शुभ विकल्प में आने पर अपने को अशुभ से बचाते हुए अज्ञानी जीवों को सच्चे मोक्षमार्ग का निरूपण कर सन्मार्ग पर लाने हेतु ही करते हैं। और आ. जयसेन जी ने जो वीतराग सम्यग्दृष्टि की मुख्यता की सो उचित ही है, परंतु लक्षण दृष्टि से ही पूर्वापर विरोध रहित तत्त्वों की प्ररूपणा करते हैं। लक्ष्य सम्यग्दर्शन का है तो उसका लक्ष्यण जो त्रिकाल अबाधित है वही श्रीमद् अमृत