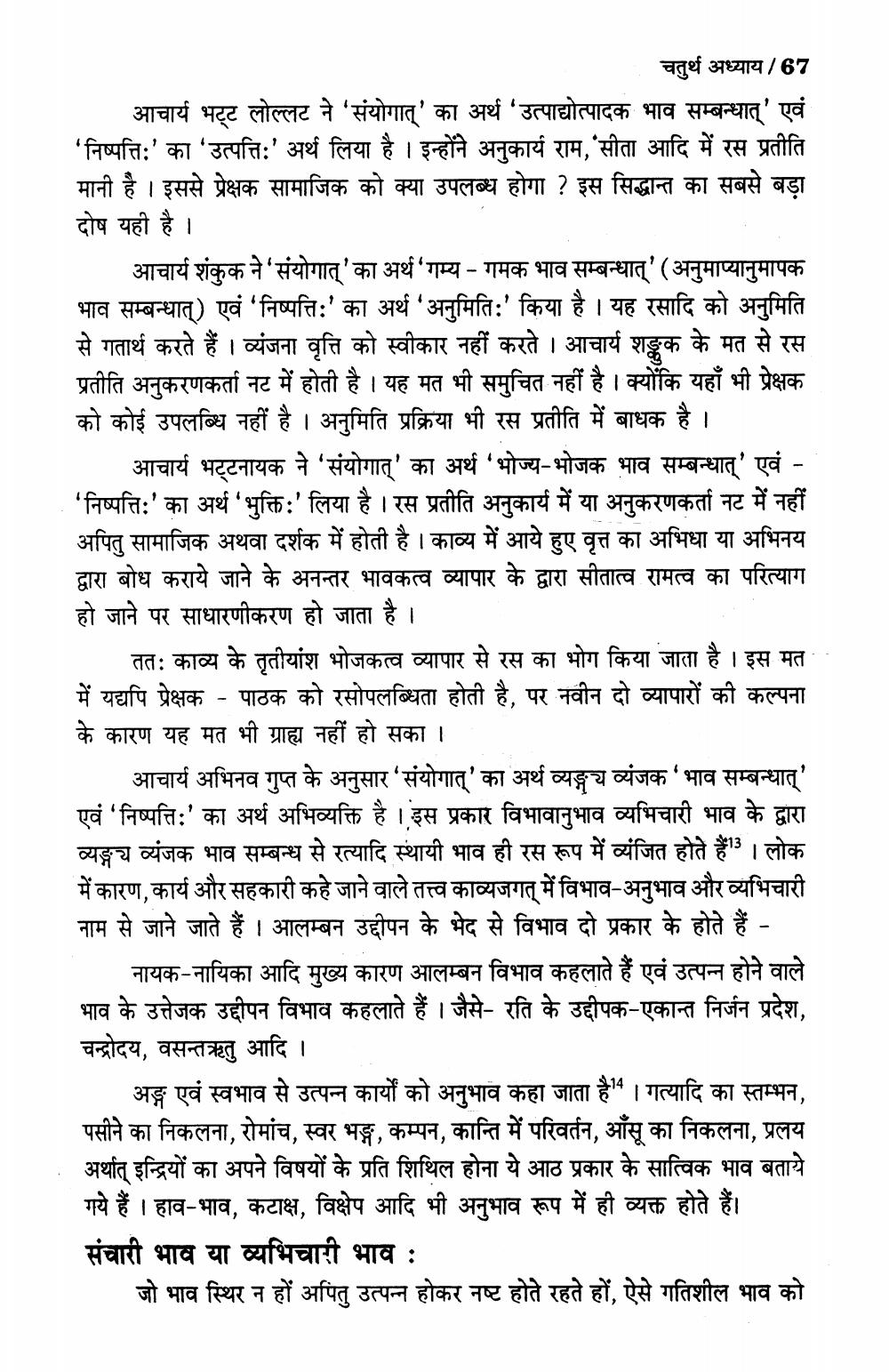________________
चतुर्थ अध्याय / 67 आचार्य भट्ट लोल्लट ने 'संयोगात्' का अर्थ 'उत्पाद्योत्पादक भाव सम्बन्धात्' एवं 'निष्पत्तिः' का ‘उत्पत्तिः' अर्थ लिया है । इन्होंने अनुकार्य राम, सीता आदि में रस प्रतीति मानी है । इससे प्रेक्षक सामाजिक को क्या उपलब्ध होगा ? इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा दोष यही है ।
आचार्य शंकुक ने ‘संयोगात्' का अर्थ 'गम्य - गमक भाव सम्बन्धात्' (अनुमाप्यानुमापक भाव सम्बन्धात्) एवं ‘निष्पत्ति:' का अर्थ 'अनुमिति:' किया है । यह रसादि को अनुमिति से गतार्थ करते हैं । व्यंजना वृत्ति को स्वीकार नहीं करते । आचार्य शङ्कु के मत से रस प्रतीति अनुकरणकर्ता नट में होती है। यह मत भी समुचित नहीं है । क्योंकि यहाँ भी प्रेक्षक को कोई उपलब्धि नहीं है । अनुमिति प्रक्रिया भी रस प्रतीति में बाधक है ।
आचार्य भट्टनायक ने 'संयोगात्' का अर्थ 'भोज्य- भोजक भाव सम्बन्धात्' एवं ‘निष्पत्तिः' का अर्थ 'भुक्तिः' लिया है। रस प्रतीति अनुकार्य में या अनुकरणकर्ता नट में नहीं अपितु सामाजिक अथवा दर्शक में होती है। काव्य में आये हुए वृत्त का अभिधा या अभिनय द्वारा बोध कराये जाने के अनन्तर भावकत्व व्यापार के द्वारा सीतात्व रामत्व का परित्याग हो जाने पर साधारणीकरण हो जाता है ।
ततः काव्य के तृतीयांश भोजकत्व व्यापार से रस का भोग किया जाता है । इस म में यद्यपि प्रेक्षक पाठक को रसोपलब्धिता होती है, पर नवीन दो व्यापारों की कल्पना के कारण यह मत भी ग्राह्य नहीं हो सका ।
-
आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार 'संयोगात्' का अर्थ व्यङ्ग्य व्यंजक 'भाव सम्बन्धात्' एवं ‘निष्पत्ति:' का अर्थ अभिव्यक्ति है । इस प्रकार विभावानुभाव व्यभिचारी भाव के द्वारा व्यङ्गय व्यंजक भाव सम्बन्ध से रत्यादि स्थायी भाव ही रस रूप में व्यंजित होते हैं । लोक में कारण, कार्य और सहकारी कहे जाने वाले तत्त्व काव्यजगत् में विभाव- अनुभाव और व्यभिचारी नाम से जाने जाते हैं । आलम्बन उद्दीपन के भेद से विभाव दो प्रकार के होते हैं -
I
नायक-नायिका आदि मुख्य कारण आलम्बन विभाव कहलाते हैं एवं उत्पन्न होने वाले भाव के उत्तेजक उद्दीपन विभाव कहलाते हैं । जैसे- रति के उद्दीपक- एकान्त निर्जन प्रदेश, चन्द्रोदय, वसन्तऋतु आदि ।
अङ्ग एवं स्वभाव से उत्पन्न कार्यों को अनुभाव कहा जाता है 14 । गत्यादि का स्तम्भन, पसीने का निकलना, रोमांच, स्वर भङ्ग, कम्पन, कान्ति में परिवर्तन, आँसू का निकलना, प्रलय अर्थात् इन्द्रियों का अपने विषयों के प्रति शिथिल होना ये आठ प्रकार के सात्विक भाव बताये गये हैं । हाव-भाव, कटाक्ष, विक्षेप आदि भी अनुभाव रूप में ही व्यक्त होते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव :
जो भाव स्थिर न हों अपितु उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते हों, ऐसे गतिशील भाव को