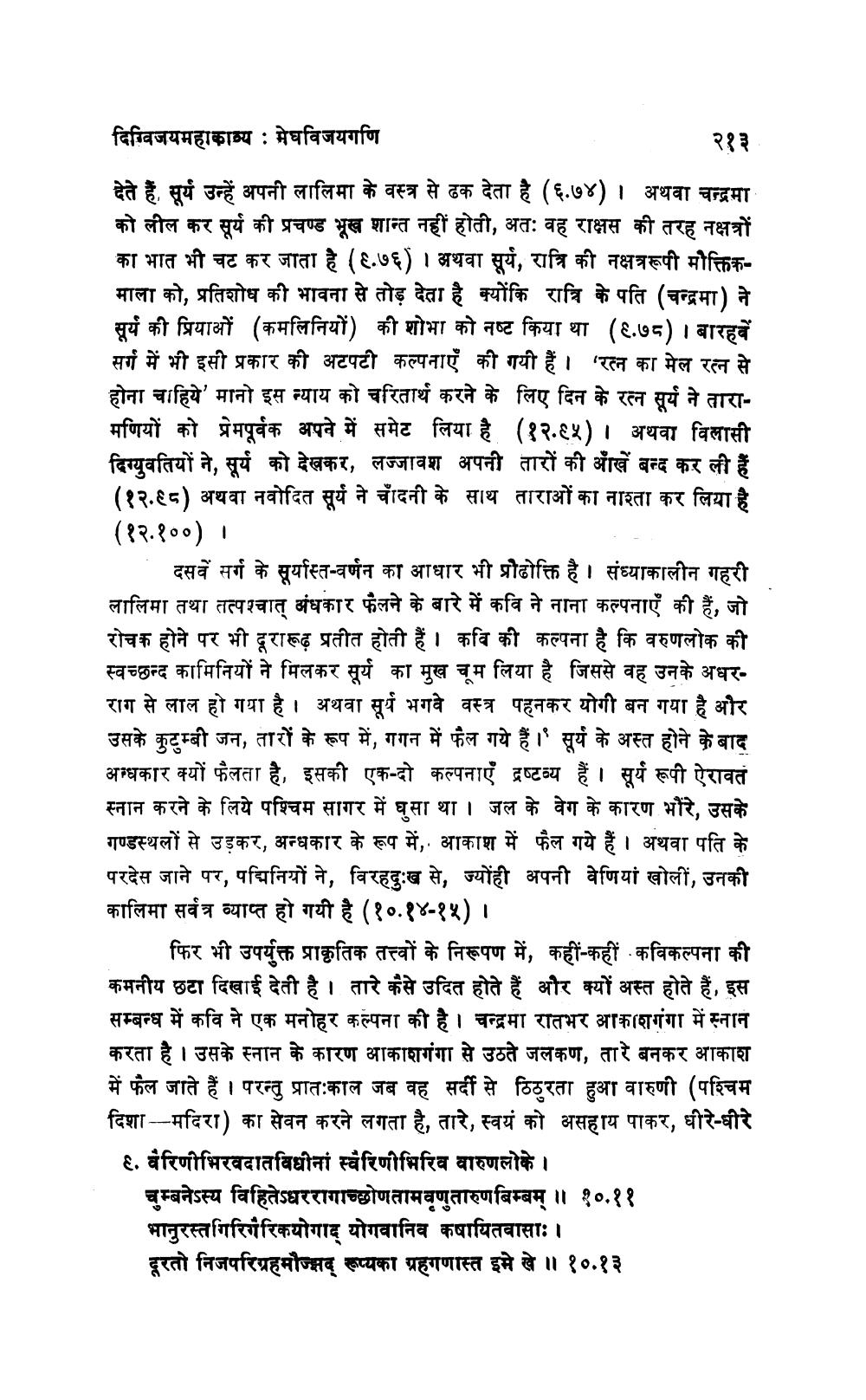________________
दिग्विजयमहाकाव्य : मेघविजयगणि
२१३ देते हैं, सूर्य उन्हें अपनी लालिमा के वस्त्र से ढक देता है (६.७४) । अथवा चन्द्रमा को लील कर सूर्य की प्रचण्ड भूख शान्त नहीं होती, अतः वह राक्षस की तरह नक्षत्रों का भात भी चट कर जाता है (६.७६) । अथवा सूर्य, रात्रि की नक्षत्ररूपी मौक्तिकमाला को, प्रतिशोध की भावना से तोड़ देता है क्योंकि रात्रि के पति (चन्द्रमा) ने सूर्य की प्रियाओं (कमलिनियों) की शोभा को नष्ट किया था (६.७८) । बारहवें सर्ग में भी इसी प्रकार की अटपटी कल्पनाएँ की गयी हैं। 'रत्न का मेल रत्न से होना चाहिये' मानो इस न्याय को चरितार्थ करने के लिए दिन के रत्न सूर्य ने तारामणियों को प्रेमपूर्वक अपने में समेट लिया है (१२.६५)। अथवा विलासी दिग्युवतियों ने, सूर्य को देखकर, लज्जावश अपनी तारों की आंखें बन्द कर ली हैं (१२.६८) अथवा नवोदित सूर्य ने चाँदनी के साथ ताराओं का नाश्ता कर लिया है (१२.१००) ।
दसवें सर्ग के सूर्यास्त-वर्णन का आधार भी प्रौढोक्ति है। संध्याकालीन गहरी लालिमा तथा तत्पश्चात् अंधकार फैलने के बारे में कवि ने नाना कल्पनाएँ की हैं, जो रोचक होने पर भी दूरारूढ़ प्रतीत होती हैं। कवि की कल्पना है कि वरुणलोक की स्वच्छन्द कामिनियों ने मिलकर सूर्य का मुख चूम लिया है जिससे वह उनके अधरराग से लाल हो गया है। अथवा सूर्य भगवे वस्त्र पहनकर योगी बन गया है और उसके कुटुम्बी जन, तारों के रूप में, गगन में फैल गये हैं। सूर्य के अस्त होने के बाद अन्धकार क्यों फैलता है, इसकी एक-दो कल्पनाएँ द्रष्टव्य हैं। सूर्य रूपी ऐरावतं स्नान करने के लिये पश्चिम सागर में घुसा था । जल के वेग के कारण भौंरे, उसके गण्डस्थलों से उड़कर, अन्धकार के रूप में, आकाश में फैल गये हैं । अथवा पति के परदेस जाने पर, पमिनियों ने, विरहदुःख से, ज्योंही अपनी वेणियां खोलीं, उनकी कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो गयी है (१०.१४-१५) ।।
फिर भी उपर्युक्त प्राकृतिक तत्त्वों के निरूपण में, कहीं-कहीं कविकल्पना की कमनीय छटा दिखाई देती है। तारे कैसे उदित होते हैं और क्यों अस्त होते हैं, इस सम्बन्ध में कवि ने एक मनोहर कल्पना की है। चन्द्रमा रातभर आकाशगंगा में स्नान करता है । उसके स्नान के कारण आकाशगंगा से उठते जलकण, तारे बनकर आकाश में फैल जाते हैं । परन्तु प्रातःकाल जब वह सर्दी से ठिठुरता हुआ वारुणी (पश्चिम दिशा-मदिरा) का सेवन करने लगता है, तारे, स्वयं को असहाय पाकर, धीरे-धीरे ६. वैरिणीभिरवदातविधीनां स्वैरिणीभिरिव वारुणलोके ।
चुम्बनेऽस्य विहितेऽधररागाच्छोणतामवृणुतारुणबिम्बम् ॥ १०.११ भानुरस्तगिरिगरिकयोगाद् योगवानिव कषायितवासाः । दूरतो निजपरिग्रहमौज्झन् रूप्यका ग्रहगणास्त इमे खे ॥ १०.१३