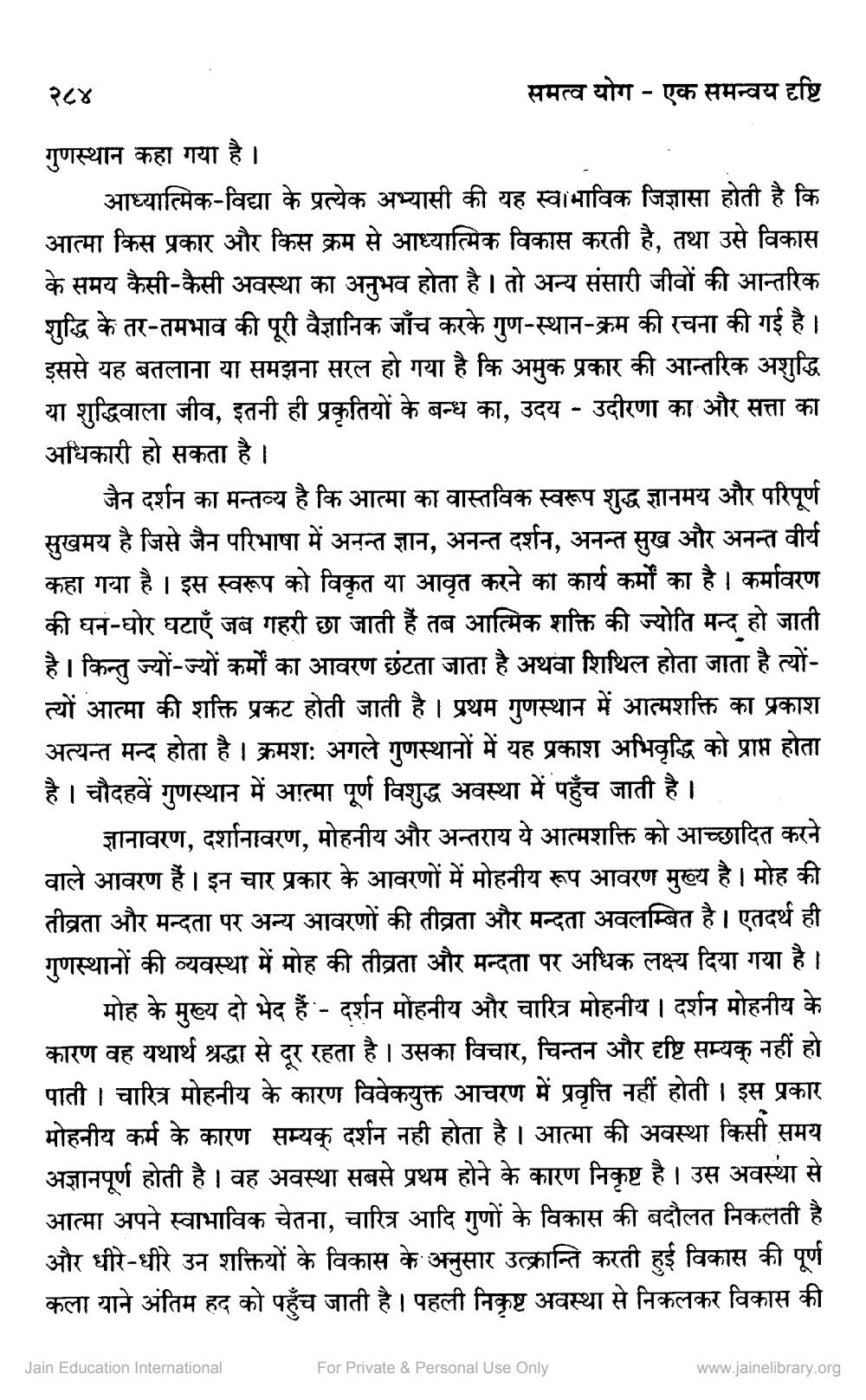________________
२८४
समत्व योग - एक समन्वय दृष्टि गुणस्थान कहा गया है।
आध्यात्मिक-विद्या के प्रत्येक अभ्यासी की यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि आत्मा किस प्रकार और किस क्रम से आध्यात्मिक विकास करती है, तथा उसे विकास के समय कैसी-कैसी अवस्था का अनुभव होता है। तो अन्य संसारी जीवों की आन्तरिक शुद्धि के तर-तमभाव की पूरी वैज्ञानिक जाँच करके गुण-स्थान-क्रम की रचना की गई है। इससे यह बतलाना या समझना सरल हो गया है कि अमुक प्रकार की आन्तरिक अशुद्धि या शुद्धिवाला जीव, इतनी ही प्रकृतियों के बन्ध का, उदय - उदीरणा का और सत्ता का अधिकारी हो सकता है। __जैन दर्शन का मन्तव्य है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध ज्ञानमय और परिपूर्ण सुखमय है जिसे जैन परिभाषा में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य कहा गया है । इस स्वरूप को विकृत या आवृत करने का कार्य कर्मों का है। कर्मावरण की घन-घोर घटाएँ जब गहरी छा जाती हैं तब आत्मिक शक्ति की ज्योति मन्द हो जाती है। किन्तु ज्यों-ज्यों कर्मों का आवरण छंटता जाता है अथवा शिथिल होता जाता है त्योंत्यों आत्मा की शक्ति प्रकट होती जाती है। प्रथम गुणस्थान में आत्मशक्ति का प्रकाश अत्यन्त मन्द होता है । क्रमश: अगले गुणस्थानों में यह प्रकाश अभिवृद्धि को प्राप्त होता है । चौदहवें गुणस्थान में आत्मा पूर्ण विशुद्ध अवस्था में पहुँच जाती है।
ज्ञानावरण, दर्शानावरण, मोहनीय और अन्तराय ये आत्मशक्ति को आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इन चार प्रकार के आवरणों में मोहनीय रूप आवरण मुख्य है । मोह की तीव्रता और मन्दता पर अन्य आवरणों की तीव्रता और मन्दता अवलम्बित है। एतदर्थ ही गुणस्थानों की व्यवस्था में मोह की तीव्रता और मन्दता पर अधिक लक्ष्य दिया गया है।
मोह के मुख्य दो भेद हैं - दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीय के कारण वह यथार्थ श्रद्धा से दूर रहता है। उसका विचार, चिन्तन और दृष्टि सम्यक् नहीं हो पाती । चारित्र मोहनीय के कारण विवेकयुक्त आचरण में प्रवृत्ति नहीं होती । इस प्रकार मोहनीय कर्म के कारण सम्यक् दर्शन नही होता है। आत्मा की अवस्था किसी समय अज्ञानपूर्ण होती है। वह अवस्था सबसे प्रथम होने के कारण निकृष्ट है । उस अवस्था से आत्मा अपने स्वाभाविक चेतना, चारित्र आदि गुणों के विकास की बदौलत निकलती है और धीरे-धीरे उन शक्तियों के विकास के अनुसार उत्क्रान्ति करती हुई विकास की पूर्ण कला याने अंतिम हद को पहुँच जाती है। पहली निकृष्ट अवस्था से निकलकर विकास की
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org