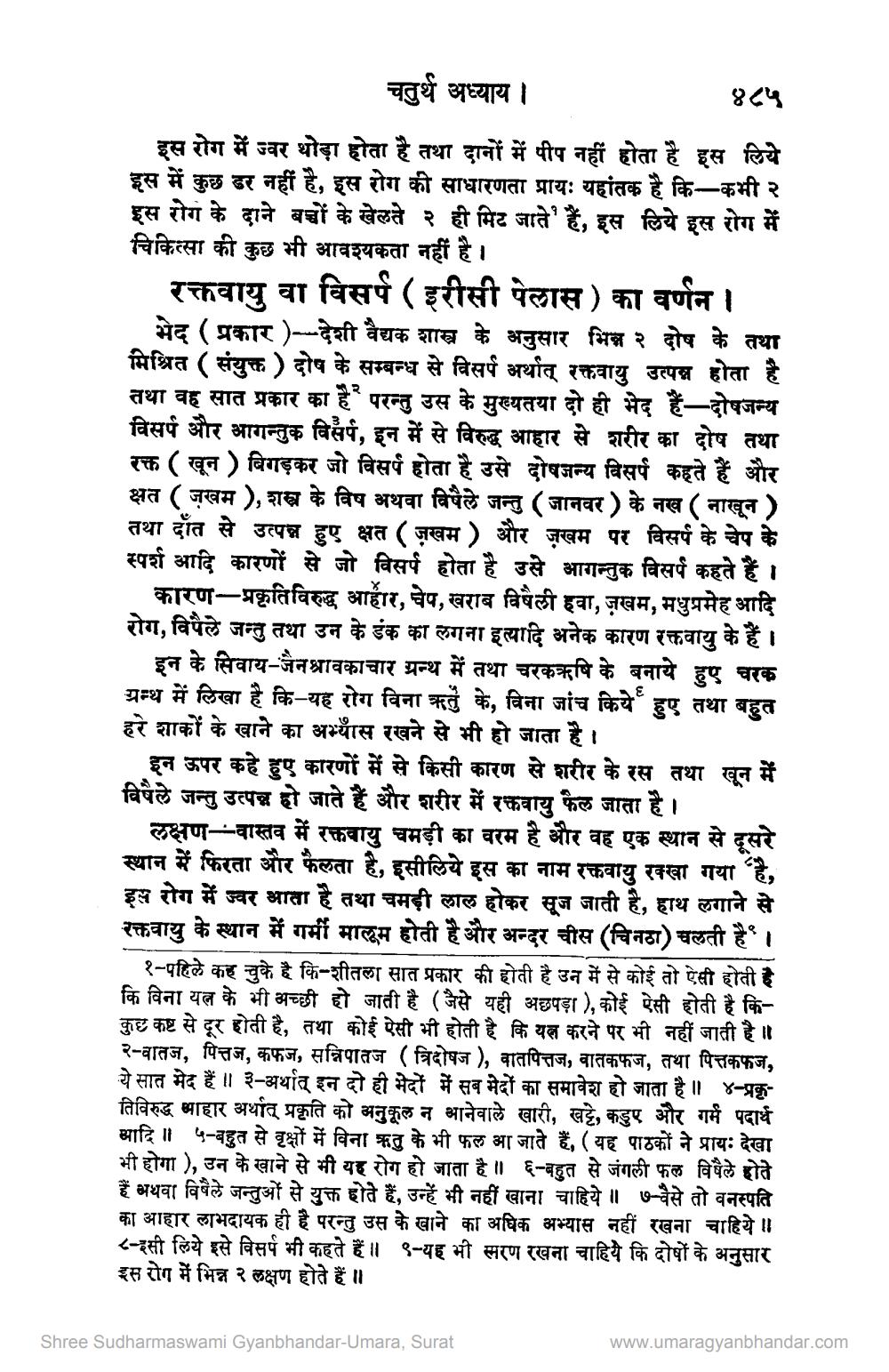________________
चतुर्थ अध्याय ।
४८५ इस रोग में ज्वर थोड़ा होता है तथा दानों में पीप नहीं होता है इस लिये इस में कुछ डर नहीं है, इस रोग की साधारणता प्रायः यहांतक है कि-कभी २ इस रोग के दाने बच्चों के खेलते २ ही मिट जाते हैं, इस लिये इस रोग में चिकित्सा की कुछ भी आवश्यकता नहीं है।
रक्तवायु वा विसर्प (इरीसी पेलास) का वर्णन ।
भेद (प्रकार )-देशी वैद्यक शास्त्र के अनुसार भिन्न २ दोष के तथा मिश्रित (संयुक्त) दोष के सम्बन्ध से विसर्प अर्थात् रक्तवायु उत्पन्न होता है तथा वह सात प्रकार का है परन्तु उस के मुख्यतया दो ही भेद हैं-दोषजन्य विसर्प और आगन्तुक विसर्प, इन में से विरुद्ध आहार से शरीर का दोष तथा रक्त (खून) बिगड़कर जो विसर्प होता है उसे दोषजन्य विसर्प कहते हैं और क्षत (जखम), शस्त्र के विष अथवा विषैले जन्तु (जानवर) के नख (नाखून) तथा दाँत से उत्पन्न हुए क्षत (जखम) और जखम पर विसर्प के चेप के स्पर्श आदि कारणों से जो विसर्प होता है उसे आगन्तुक विसर्प कहते हैं । __ कारण-प्रकृतिविरुद्ध आहार, चेप, खराब विषैली हवा, ज़खम, मधुप्रमेह आदि रोग, विपैले जन्तु तथा उन के डंक का लगना इत्यादि अनेक कारण रक्तवायु के हैं।
इन के सिवाय-जैनश्रावकाचार ग्रन्थ में तथा चरकऋषि के बनाये हुए चरक ग्रन्थ में लिखा है कि यह रोग विना ऋतु के, विना जांच किये हुए तथा बहुत हरे शाकों के खाने का अभ्यास रखने से भी हो जाता है।। ___ इन ऊपर कहे हुए कारणों में से किसी कारण से शरीर के रस तथा खून में विषैले जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर में रक्तवायु फैल जाता है।
लक्षण वास्तव में रक्तवायु चमड़ी का वरम है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता और फैलता है, इसीलिये इस का नाम रक्तवायु रक्खा गया है, इस रोग में ज्वर आता है तथा चमड़ी लाल होकर सूज जाती है, हाथ लगाने से रक्तवायु के स्थान में गर्मी मालूम होती है और अन्दर चीस (चिनठा) चलती है।
१-पहिले कह चुके है कि-शीतला सात प्रकार की होती है उन में से कोई तो ऐसी होती है कि विना यत्न के भी अच्छी हो जाती है (जैसे यही अछपड़ा), कोई ऐसी होती है किकुछ कष्ट से दूर होती है, तथा कोई ऐसी भी होती है कि यल करने पर भी नहीं जाती है । २-वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज (त्रिदोषज), वातपित्तज, वातकफज, तथा पित्तकफज, ये सात मेद हैं ॥ ३-अर्थात् इन दो ही भेदों में सब मेदों का समावेश हो जाता है ॥ ४-प्रकृतिविरुद्ध आहार अर्थात् प्रकृति को अनुकूल न आनेवाले खारी, खट्टे, कडुए और गर्म पदार्थ आदि ॥ ५-बहुत से वृक्षों में विना ऋतु के भी फल आ जाते हैं, (यह पाठकों ने प्रायः देखा भी होगा), उन के खाने से भी यह रोग हो जाता है ॥ ६-बहुत से जंगली फल विषैले होते हैं अथवा विषैले जन्तुओं से युक्त होते हैं, उन्हें भी नहीं खाना चाहिये ॥ ७-वैसे तो वनस्पति का आहार लाभदायक ही है परन्तु उस के खाने का अधिक अभ्यास नहीं रखना चाहिये। --इसी लिये इसे विसर्प भी कहते हैं ॥ ९-यह भी मरण रखना चाहिये कि दोषों के अनुसार इस रोग में भिन्न २ लक्षण होते हैं।
Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat
www.umaragyanbhandar.com