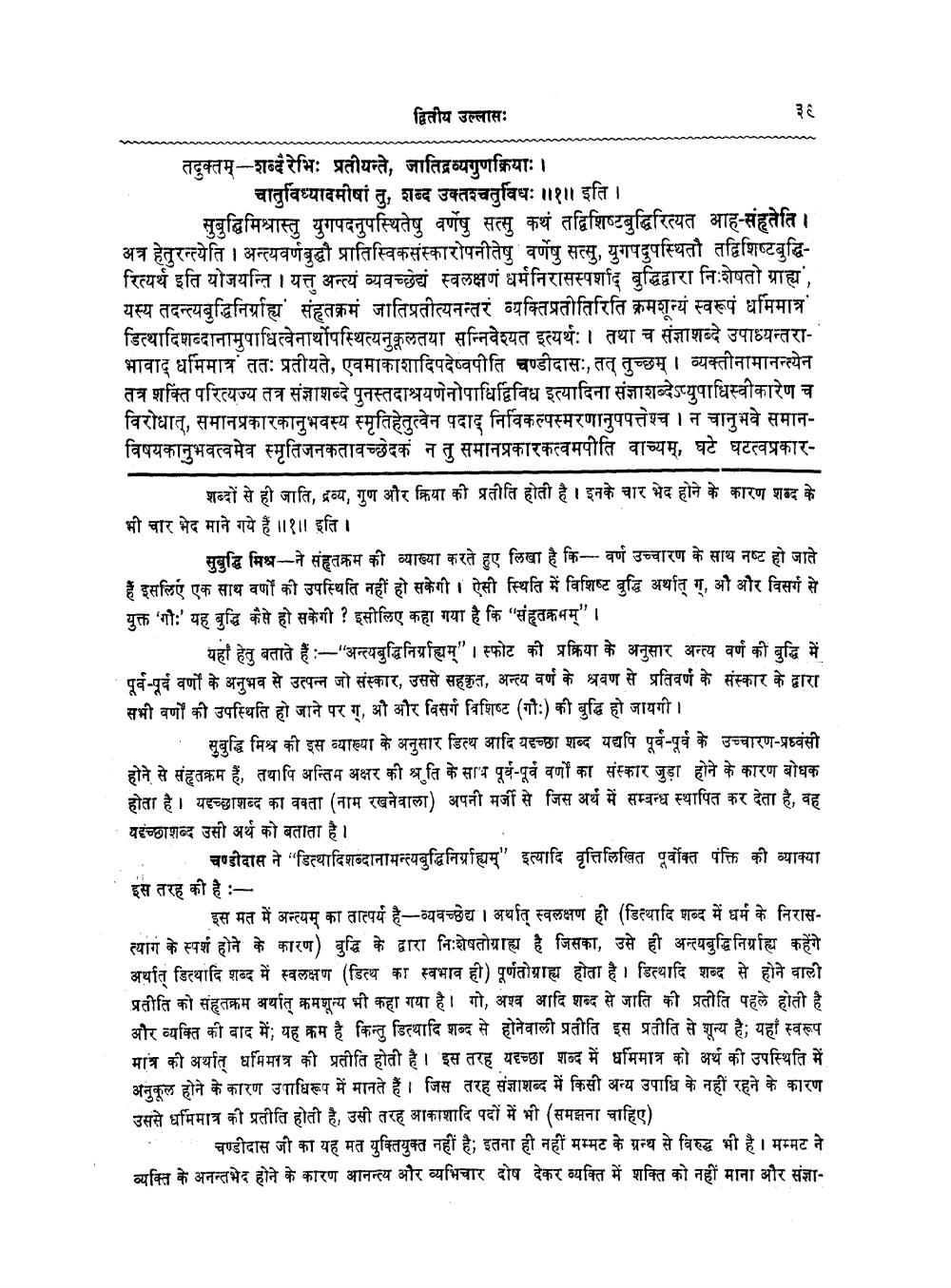________________
द्वितीय उल्लासः
तदुक्तम्-शब्दै रेभिः प्रतीयन्ते, जातिद्रव्यगुणक्रियाः।
चातुर्विध्यादमीषां तु, शब्द उक्तश्चतुर्विधः ॥१॥ इति ।
सुबुद्धिमिश्रास्तु युगपदनुपस्थितेषु वर्णेषु सत्सु कथं तद्विशिष्टबुद्धिरित्यत आह-संहृतेति । अत्र हेतरन्त्येति । अन्त्यवर्णबद्धौ प्रातिस्विकसंस्कारोपनीतेष वर्णेष सत्स, युगपदपस्थितौ तद्विशिष्टबुद्धिरित्यर्थ इति योजयन्ति । यत्तु अन्त्यं व्यवच्छेद्यं स्वलक्षणं धर्मनिरासस्पर्शाद् बुद्धिद्वारा निःशेषतो ग्राह्य, यस्य तदन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्य संहृतक्रमं जातिप्रतीत्यनन्तरं व्यक्तिप्रतीतिरिति क्रमशून्यं स्वरूपं धर्मिमात्र डित्थादिशब्दानामुपाधित्वेनार्थोपस्थित्यनुकूलतया सन्निवेश्यत इत्यर्थः । तथा च संज्ञाशब्दे उपाध्यन्तराभावाद् धर्मिमात्र ततः प्रतीयते, एवमाकाशादिपदेष्वपीति चण्डीदासः, तत् तुच्छम् । व्यक्तीनामानन्त्येन तत्र शक्ति परित्यज्य तत्र संज्ञाशब्दे पुनस्तदाश्रयणेनोपाधिविविध इत्यादिना संज्ञाशब्देऽप्युपाधिस्वीकारेण च विरोधात्, समानप्रकारकानुभवस्य स्मृतिहेतुत्वेन पदाद् निर्विकल्पस्मरणानुपपत्तेश्च । न चानुभवे समानविषयकानुभवत्वमेव स्मृतिजनकतावच्छेदकं न तु समानप्रकारकत्वमपीति वाच्यम्, घटे घटत्वप्रकार
शब्दों से ही जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया की प्रतीति होती है। इनके चार भेद होने के कारण शब्द के भी चार भेद माने गये हैं ।।१।। इति ।
सुबुद्धि मिश्र-ने संहतक्रम की व्याख्या करते हुए लिखा है कि-वर्ण उच्चारण के साथ नष्ट हो जाते हैं इसलिए एक साथ वर्णों की उपस्थिति नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में विशिष्ट बुद्धि अर्थात् ग, औ और विसर्ग से युक्त 'गौः' यह बुद्धि कैसे हो सकेगी? इसीलिए कहा गया है कि “संहृतक्रमम्"।
यहाँ हेतु बताते हैं :--"अन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यम्" । स्फोट की प्रक्रिया के अनुसार अन्त्य वर्ण की बुद्धि में पूर्व-पूर्व वर्णों के अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार, उससे सहकृत, अन्त्य वर्ण के श्रवण से प्रतिवर्ण के संस्कार के द्वारा सभी वर्गों की उपस्थिति हो जाने पर ग्, औ और विसर्ग विशिष्ट (गौः) की बुद्धि हो जायगी।
सुबुद्धि मिश्र की इस व्याख्या के अनुसार डित्थ आदि यदृच्छा शब्द यद्यपि पूर्व-पूर्व के उच्चारण-प्रध्वंसी होने से संहृतक्रम हैं, तथापि अन्तिम अक्षर की श्रुति के साथ पूर्व-पूर्व वर्गों का संस्कार जुड़ा होने के कारण बोधक होता है। यहच्छाशब्द का वक्ता (नाम रखनेवाला) अपनी मर्जी से जिस अर्थ में सम्बन्ध स्थापित कर देता है, वह यहच्छाशब्द उसी अर्थ को बताता है। . चण्डीदास ने “डित्थादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यम्" इत्यादि वृत्तिलिखित पूर्वोक्त पंक्ति की व्याक्या इस तरह की है :
इस मत में अन्त्यम् का तात्पर्य है-व्यवच्छेद्य । अर्थात् स्वलक्षण ही (डित्यादि शब्द में धर्म के निरासत्याग के स्पर्श होने के कारण) बुद्धि के द्वारा निःशेषतोग्राह्य है जिसका, उसे ही अन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्य कहेंगे अर्थात् डित्यादि शब्द में स्वलक्षण (डित्थ का स्वभाव ही) पूर्णतोग्राह्य होता है। डित्थादि शब्द से होने वाली प्रतीति को संहृतक्रम अर्थात् क्रमशून्य भी कहा गया है। गो, अश्व आदि शब्द से जाति की प्रतीति पहले होती है और व्यक्ति की बाद में; यह क्रम है किन्तु डित्यादि शब्द से होनेवाली प्रतीति इस प्रतीति से शून्य है; यहाँ स्वरूप मात्र की अर्थात् धर्मिमात्र की प्रतीति होती है। इस तरह यदृच्छा शब्द में धर्मिमात्र को अर्थ की उपस्थिति में अनुकूल होने के कारण उपाधिरूप में मानते हैं। जिस तरह संज्ञाशब्द में किसी अन्य उपाधि के नहीं रहने के कारण उससे मिमात्र की प्रतीति होती है, उसी तरह आकाशादि पदों में भी (समझना चाहिए)
चण्डीदास जी का यह मत युक्तियुक्त नहीं है। इतना ही नहीं मम्मट के ग्रन्थ से विरुद्ध भी है। मम्मट ने व्यक्ति के अनन्तभेद होने के कारण आनन्त्य और व्यभिचार दोष देकर व्यक्ति में शक्ति को नहीं माना और संज्ञा